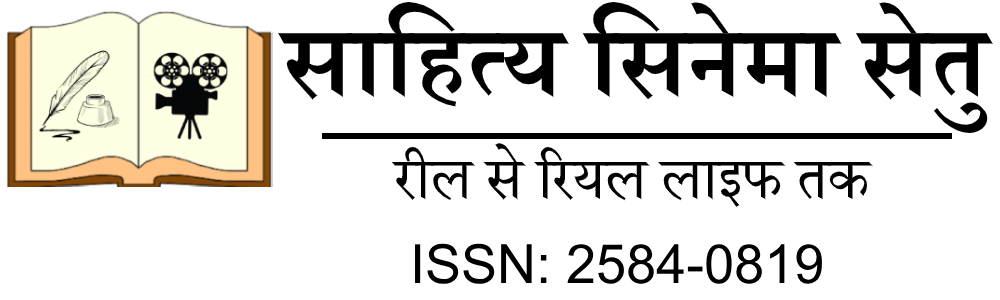“मैं” से उठकर मैंने जब देखा जो ज़रा ध्यान से
आत्मा थी दिग्भ्रमित, मन था भरा अज्ञान से।
चक्षुओं की परिधि भी सीमित रही स्वकुटुंब तक
संकुचित समस्त भावनाएँ, थी पहुँच प्रतिबिम्ब तक
ओज़ वाणी में था इतना, स्वयं सुन सकता था बस
अंतर्मन प्रदूषित-कलुषित, आंतरिक संरचना ध्वस्त।
तेज अपना देखना नहीं चाहता था खुद ही जानकर
कहीं सो रही थी प्रेरणायें संधि की चादर तानकर
संवेदनाएं जीवित तो थी पर रूप धर असंवेदना का
स्पर्श मृतप्राय: था लगभग बोध नहीं कुछ चेतना का।
ह्रदय की आतुरता बढती तोड़ पुष्प माला गूंथने को
अधरों पर रखकर पंखुडियां सुगंध उनकी सूंघने को
कुछ टूटे धागों से बंधी हुई स्वाद-ग्रंथि की जटिलता
दासता कहें शब्द बेहतर गरिमामयी नहीं शिथिलता।
त्याग “मैं” जब एक दिवस स्वप्रेरित हो मंथन किया
कुछ आत्म विश्लेषण किया, कुछ आत्म चिंतन किया
मैंने देखा धरनी है विस्तृत अन्दर समाहित व्योम है
रोम-रोम आदित्य रूप और शिख से नख तक ॐ है
अग्नि, माटी, वायु, नभ की भीतर मेरे जल-धार है
“दीपक” मैं नहीं संसार से, मुझसे समस्त संसार है।