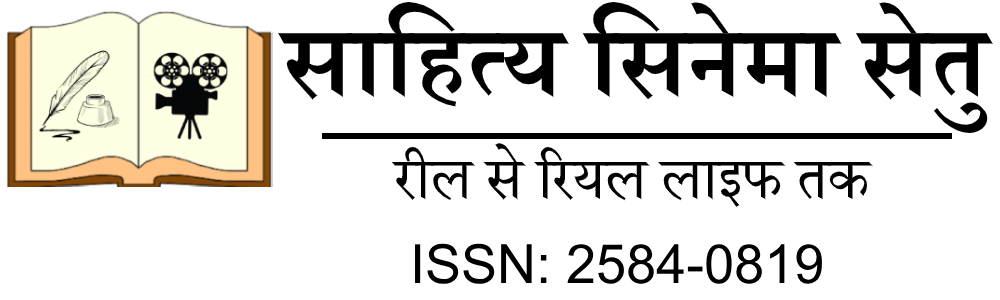मध्यकाल इतिहास के पन्नों पर ‘संक्रांत युग’ के रूप में दर्ज़ है। इतिहास साक्षी है कि क्रांति सदैव नए मूल्य स्थापित करती है। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में स्थापित मूल्यों पर बात करने से पहले एक दृष्टि इस तत्व पर कि ‘मूल्य क्या है’? और ‘इसकी उद्भावना कैसे होती है’?
मूल्य समाज के विविध ढाँचों के अनुरूप तय होते हैं, साथ ही समय और समाज से संबद्ध भी। मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार, “मूल्य द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से बदलते रहते हैं। ” इसलिए प्रत्येक युग में प्रत्येक समाज की संरचना एवं मूल्य अलग-अलग होते हैं। यह कहना उचित होगा कि मूल्य की उद्भावना वैयक्तिक स्तर पर न होकर, सामाजिक संदर्भ में होती है।
बदलते समय में नए मूल्यों की स्थापना यह प्रमाणित करती है कि हम ‘स्व’ से ‘पर’, ‘भाव’ से ‘वस्तु’ तथा अंतर्जगत से बहिर्जगत की ओर अग्रसर रहे हैं। प्लेटो ने ‘सत्य, शिव ,सुंदर’ के समवेत रूप को मूल्य माना और समाज तथा संस्कृति में तलाशा तो अरस्तू ने ‘सत्, श्रेयस और सौंदर्य ‘ को भिन्न -भिन्न मूल्य मानते हुए यूनानी अवधारणा को बल दिया। मार्शल मूल्य को ‘ईश्वर- निर्मित’ मानते हैं, जबकि नीत्से मूल्यों के निर्माण के लिए ‘मनुष्य’ को उत्तरदायी मानते हैं। सार्त्र भी मनुष्य को मूल्य- निर्माता मानते हैं।
मूल्य वह तत्व है, जो मानव-चेतना को ऊर्जास्वित करता है और मानवता के हित की चिंता के लिए मनुष्य को सक्रिय रखता है। हॉब्स, स्पिनोजा, बेंथम, मिल आदि के अनुसार, मूल्य ‘मनोवैज्ञानिक हेतुओं’ से निर्मित होते हैं। मूल्य के संबंध में मुक्तिबोध ने कहा है, “जब स्वयं अस्वयं हो जाता है — अपने से बृहत्तर, विलक्षण, अस्वयं ।” 1) बलवीर सिंह गौंछवाल के अनुसार, “साधारण अर्थों में कोई वस्तु जो मानवीय इच्छा तथा आवश्यकता की पूर्ति करती है, मूल्य कहलाती है।”2) इसीप्रकार वीरेंद्र मोहन का मानना है , “मानवीय जीवन की गतिविधि को निर्धारित करने तथा संचालित करने वाले मूलभूत तत्वों को मूल्य की संज्ञा दी जाती है।” 3)
मूल्यों की उद्भावना पर विचार करें तो यह एक द्वंद्वात्मक स्थिति का परिणाम है, जिनके लिए सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को उत्तरदायी माना जाता रहा है। कालखंड अपनी राजनीतिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि पर मूल्य स्थापित करते हैं। समय के साथ कुछ मूल्यों का ह्रास होता है तो कुछ की स्थापना। मूल्य स्थापक कई बार क्रांति में स्वयं को सशरीर आहूत कर और कई बार अपनी रचनाओं को माध्यम बनाकर नवीन मूल्यों का बीजारोपण करते हैं। साहित्य एक ओर नवीन मूल्यों की रचना कर, सड़ित गलित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध नवीन व्यवस्था की स्थापना की प्रेरणा देता है तो दूसरी ओर तात्कालिक समय में समाज को निष्क्रिय बनाने वाले बंजर हो रहे मूल्यों के प्रतिकार हेतु क्रांति का आह्वान करता है।
मूल्यों में बदलाव का कारण ‘समाज में परिवर्तन’ होना है। सामंती व्यवस्था में स्थापित मूल्यों का पूंजीवादी व्यवस्था में क्षरण हो गया। यह स्थापित सत्य है कि जब -जब सामाजिक व्यवस्था शोषण तंत्र को जन्म देती है, तब-तब जनसामान्य इसके प्रतिकार हेतु उठ खड़ा होता है। इसीप्रकार मूल्य- परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण ‘युग-परिवर्तन’ भी माना जा सकता है। ‘युग -परिवर्तन’ अर्थात दृष्टि- विस्तार और यह विस्तार अपनी प्राचीन पृष्ठभूमि से ऊर्जा पाता है। नेमिचंद् जैन का मानना है : “वास्तव में प्रत्येक नवीन युग अपने साथ साहित्य ही नहीं, जीवन की समस्त सर्जनात्मक गतिविधियों के नए मानदंड लाता है।”4)
अतएव यह मानना बेहतर होगा कि मूल्य में परिवर्तन तभी आते हैं जब पूर्व स्थापित मूल्य बर्बर हो जाते हैं। साहित्य के अंतर्गत सभी विधाएँ भिन्न- भिन्न युगों में अपनी स्थापनाएँ बदलती रहती हैं। यह इस बात का प्रमाण भी है कि समाज में नवीन मूल्यों की उद्भावना की अपनी अनिवार्यता है। रचनाकार सामाजिक संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था के विरुद्ध संघर्षरत होता है और इस दृष्टि से वह बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधि होता है। वह समाज का प्रतिनिधि पहले होता है, रचनाकार बाद में। बात यदि कविता की हो तो इस संदर्भ में वेणुगोपाल जी के लेख का उद्धरण यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है :
“अगर कविता एक सामाजिक कार्य है (जो कि वह है) तो फिर उसका राजनीतिक , सामाजिक, आर्थिक, परिस्थितियों से जुड़ना अनिवार्य ही है। कवि इसलिए प्रभावित होता है और प्रतिक्रिया करता है। कविता उसकी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा होती है।5)
मूल्य एवं रचना के अंतर्संबंधों पर बात करें तो यह कहना उचित होगा कि रचनाकार अपने युग और समाज का साक्षी एवं भोक्ता उसीप्रकार होता है, जैसे आम आदमी। अनुभव, मूल्य- निर्माण एवं रचना की निर्मिति — दोनों की प्रक्रियाओं से संबद्ध होता है। मूल्य एवं रचना के सृजन में रचनाकार के परिवेश की भी आधारभूत भूमिका होती है। उसी आधार पर रचना की आत्मा आकार ग्रहण करती है।
पूर्वमध्यकालीन समाज पर एक नज़र डालें तो मेरे हिसाब से इस काल को ‘सामंती शासन का काल’ कहा जा सकता है। क्योंकि उस समय सामंत न केवल भूमि पर, बल्कि किसानों के श्रम पर भी एकाधिकार रखते थे। किसान बंधुआ मज़दूर न होकर भी अर्धदास की सी स्थिति में थे।
के. एस. लाल ने लिखा भी है — ” प्रारंभिक मुसलमान राजाओं ने भारतवर्ष पर शासन करते समय देखा कि यहाँ की जनता राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि स्वीकार करती है।”6)
अब्दुर्रहमान इब्ने खलदून ने लिखा है :” मध्यकाल के सम्राट जनता से प्राप्त होने वाले कर एवं लगान और लूट की संपत्ति से अपनी विलासिता का साधन एकत्रित करते थे।” 7)
हालाँकि अकबर ने अपनी नीतियों से इस्लाम का भारतीयकरण कर दिया, मगर उन्होंने तथा कुछ अन्य बादशाहों ने दरबार में कुछ ऐसी रस्में प्रारंभ कीं जो अनैतिक कही जानी चाहिए। जैसे — अबुल फज़ल ने ‘कोर्निश’ और ‘तस्लीम’ का आयोजन सम्राट के अभिवादन के लिए किया। अकबर ने ‘सिजदा’ और जहाँगीर ने ‘ज़मीनबोस’ यानी बादशाह के सम्मान में झुककर धरती चूमने की प्रथा चालू की।8)
नूरल हसन ने भी स्वीकारा, “मुग़ल व्यवस्था अपने अपने चरित्र में मूलत: सामंतवादी तथा प्राक् पूँजीवादी है।” 9)
सामंतों की बढ़ती संख्या ने शासक और जनता की दूरी बढ़ाई। दोनों वर्गों के बीच मध्य वर्ग उदित हुआ। उसने भी मूढ़ श्रमिक वर्ग का शोषण ही किया। सामंतों का अंतहीन विकास ही आगे चलकर उनके अंतर्विरोध और अंतत: विनाश का कारण बना और व्यक्तिवाद का उदय हुआ। यह काल हरएक क्षेत्र में विघटन का काल रहा। ‘स्व’ प्रमुख हो चला। अर्थ के स्वामित्व ने धर्म को अर्थ का दास बना डाला। हिंदू पुरोहितों और मुसलमान उलमाओं का प्रभुत्व रहा, जिनके द्वारा मूढ़ जनमानस के बीच धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता और वर्णवादिता को हवा दी गई। उन्हें ईश्वर का भय दिखाकर विधि- निषेध के कर्मकांडों में उलझाया गया। धर्म के छोले में आडंबर का इतना सूक्ष्म और कठोर जाल बुना गया कि समाज ‘अमानवीयता का घर’ बनकर रह गया। पुरोहित और मुल्ला सामंत और शासक वर्ग के अनुरूप नियम बनाते और निरीह निरक्षर प्रजा उनकी थोथी रूढ़ियों में जकड़ी हाड़- माँस का पुतला बनकर रह जाती। आर्थिक दुरवस्था ने अनेक अमानवीय कृत्यों को जन्म दिया। किसान- मज़दूर अपने बच्चे बेचने लगे। स्वामी रामानंद, कबीर एवं अन्य संतों तथा भक्तों के काव्य में देशवासियों के प्रति तत्कालीन पीड़ा उभर कर आई है।
अबुल फज़ल ने अकाल का ज़िक्र किया है : ” अकबर के समय का अकाल इतना भीषण था कि लोगों ने एक – दूसरे का भक्षण करना शुरू कर दिया था तथा नगर के मार्ग तथा गलियाँ लाशों से पट गई थीं।10)
गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस दयनीय स्थिति का उल्लेख किया है। इरफ़ान हबीब ने निष्पक्ष भाव से लिखा, ” जनता को जोतने के लिए ज़मीन मिलती थी लेकिन पेट भरने के लिए अन्न उपलब्ध नहीं हो पाता था।”11)
मध्यकाल में हिंदू या तो युद्ध में मारे गए या दास बनाए गए। विजेताओं / आक्रमणकारियों से कन्या की रक्षा के लिए ‘बाल विवाह ‘ की प्रथा शुरू हुई। जौहर के नाम पर अमानवीय ‘सती प्रथा’ का सूत्रपात हुआ जिसमें मृत पति के साथ जीवित पत्नी आग की लपटों के हवाले की जाती थी और पुरोहित उसकी स्वर्ग-यात्रा का स्वाँग रचते न थकते थे । सती प्रथा को धर्म का चोला पहनाया गया और विधवा विवाह को निकृष्ट माना गया। श्रमिक शूद्र और अछूत की श्रेणी में पहुँचाए गए, जिन्हें न शिक्षा का अधिकार था ,न मंदिर में प्रवेश करने का।
ताराचंद ने ‘सोसाइटी एंड स्टेट इन मुग़ल पीरियड’ में विस्तार से लिखा है। प्रेमशंकर ने लिखा है : “कई बार भक्ति चेतना के माध्यम से निम्न वर्ग को धार्मिक आधार देने की चेष्टा की गई, पर बार -बार नेतृत्व उच्च वर्ग हथिया लेता था। ब्राह्मण उसे सैद्धांतिक रूप दे रहे थे। उसे क्षत्रियों का प्रश्रय तथा वैश्यों का आर्थिक समर्थन प्राप्त था।12)
मध्यकाल ने स्त्री से उसकी सोच छीन ली थी। समय के प्रवाह, पुरुष समाज के प्रभुत्व, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों के कारण महज उपादान बनी स्त्री भूलने लगी कि वह भी मानवी है — सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना — ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार! निम्न वर्ग की स्त्रियों को घर से बाहर कमाने जाना पड़ता था तो भी वे पुरुषों के समान स्वच्छंद नहीं थीं, दिखती भले हों। कई घरों में इसी समय से कन्या जन्म दुर्भाग्य माना जाने लगा। व्यापारी, सामंत और शासक वर्ग की स्त्रियाँ महँगी पोशाकों और गहनों से लदी-फदी कठपुतलियाँ थीं जो पुरुषों को खुश करने और रखने का निमित्तमात्र थीं। इसे ही उन्होंने अपनी नियति मान ली थी। धर्म, संस्कार और मर्यादा के नाम पर लादी गई बेड़ियाँ उन्हें सुरक्षा कवच लगने लगीं। अस्मिता के नाम पर स्त्री मस्तिष्क से उतरकर देहमात्र हो गई। और देह-शुचिता की रक्षा के नाम पर नियामकों ने उसे वर्जनाओं से लाद दिया। हद तो यह हुई कि शापित ज़िंदगी जीती स्त्रियों के कामिनी स्वरूप को ही पुरुष समाज की कामुकता का कारण मानकर उसकी उपेक्षा ही की गई। संतों ने धिक्कार के स्वर निकाले। संत कबीर ने स्त्री को साधना -मार्ग की बाधा माना है :
“एक कनक अरु कामिनी, विष फल की ए उपाइ।
देखै हीं धै विष चढ़ै , खायें सूँ मरि जाइ।।”
किसी ने भी नहीं सोचा कि इसमें स्त्री कहाँ दोषी है? या क्या वह उपादान से अधिक समझी जा रही है? किंतु वर्जनाओं में जकड़ी प्रतिभा जहाँ परिस्थितियों की अनुकूलता या प्रतिकूलता को ही अवसर मानकर स्वत: बिखरी, वहीं नए मूल्य रच गई। मीराबाई इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी प्रकार, सहजोबाई, दयाबाई, उमा आदि संत कवयित्रियों के साहित्य में अभिव्यक्त भाव एवं विचारों की ऊँचाई ने कबीर एवं उन जैसे अन्य संतों की सोच को गलत साबित कर दिया है।
हम देखते हैं कि एक ओर यह काल अराजकता और निरंकुशता के युग के रूप में उभरता है तो दूसरी ओर वर्ण, जाति, कुल, गोत्र में टूटती हुई स्थिति भी मूल्य मानी जाती है। हिंदू और इस्लाम के रूप में धार्मिक मूल्य प्रतिष्ठित होते हैं, अन्य धार्मिक आचार- व्यवहार सहयोगी मूल्यों का स्थान पाते हैं।
मूल्य वस्तुत: मनुष्य से संबद्ध हैं। मध्यकालीन मूल्यों की स्थापना का श्रेय श्रमिक वर्ग को जाता है, जिसने सहज सौंदर्य को माध्यम बनाकर इसकी रचना की। मध्यकाल सामंती भोग का युग रहा। इसलिए ‘काम'(कामवासना) को मूल्य के रूप में स्वीकारा गया। ईश्वर की कल्पना ‘भाववादी मूल्य’ के रूप में की गई। ‘अर्थ’ (धन) परिवर्तनशील कारक होने के बावजूद भी अनिवार्य मूल्य माना गया। ‘मोक्ष’ ही एकमात्र ऐसा मूल्य रहा जो शुद्ध आध्यात्मिकता का द्योतक है। तत्कालीन समाज में शोषित वर्ग आभिजात्य वर्ग के समक्ष टिक नहीं सकता था, किंतु उनकी जीवन- दृष्टि में परिवर्तन की झलक संत साहित्य से मिल जाती है। वैष्णव कवियों में यह परिवर्तन भिन्न रूप में, आस्था और आशा के संचार के रूप में नज़र आता है।
संत कवियों ने अध्यात्म को सामने रखकर भौतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता हेतु स्वर मुखरित किए ; धर्म को माध्यम बनाकर समता और बंधुत्व की भावना को पोषित किया। भक्त कवियों ने स्वस्थ समाज की कल्पना की जहाँ संबंधों के प्रति जीवंतता और लोकपक्ष के प्रति दायित्वबोध चैतन्य है। तुलसी का रामराज्य, कबीर का वर्णरहित समाज , जायसी का प्रेमलोक, सूर का ग्राम्य और लोक-संस्कृति से संबद्ध कृष्ण प्रेम, लोकाचारों में आरोपित मानवीय संबंधों की स्थापना, रहीम का मानव-प्रेम, मीरा का अध्यात्म से रंगा कोमल बाल प्रेम जो बढ़ती उम्र के साथ परिपक्व होता जाता है; गंगाबाई का वात्सल्य और सहजोबाई तथा दयाबाई का इष्ट के निर्गुण अस्तित्व को अध्यात्म के उच्चतम स्थान पर आसीन करना तत्कालीन स्थापित मूल्यों के विखंडन और नए मूल्यों की स्थापना करता है। हालाँकि कुछ वैष्णव कवि स्वयं को प्राचीन मूल्यों और मान्यताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाते, किंतु सूरदास,नंददायस, परमानंददास तथा अन्य कृष्णभक्त कवियों ने राधा और गोपियों को माध्यम बनाकर स्त्री को स्वतंत्रचेता के रूप में स्थापित किया है। वहाँ स्त्री भोग्या नहीं, सखी है, प्रेमिका है, माँ है, धायी है, बालकों पर मुक्त नेह लुटाने वाली पड़ोसिनें हैं। पूर्वमध्यकालीन और कुछ उत्तरमध्यकालीन कवियों ने भी प्रेम के हर एक सोपान का चित्रण करते हुए और स्त्री को पुरुष के समकक्ष रखते हुए प्रेम को अध्यात्म स्वरूप प्रदान किया है। इसीप्रकार, स्त्री से संबद्ध पुरुष के विविध रूपों को उभारा है, जहाँ पुरुष मित्र है, पिता है, भाई है, पड़ोसी है, सजग ग्रामीण और नागरिक है। मानवीय मूल्यों की स्थापना में कृष्णभक्त कवियों का श्रेय अधिक है, विशेषकर सूर का। सामंत परिवार की मीरा ने जिसप्रकार वर्जनाओं को तोड़ा और स्त्री चेतना को झकझोरा , वह समकालीन स्त्री विमर्श का आदि रूप है। आचार्य रामानंद की परंपरा मानव एकता के विकास की परंपरा है। उन्होंने सगुण और निर्गुण — दोनों उपासकों को ‘रामनाम’ का दीक्षामंत्र दिया और ईश आराधना सर्वसुलभ करके तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था पर चोट किया।एक ओर कबीर, दादू, मलूक, पीपा, रैदास, सुरसरि जैसे निम्नवर्णीय शिष्य हुए तो दूसरी ओर उच्चवर्णी भी। भोगवादी संस्कृति के विरुद्ध सामूहिक हितयुक्त समाज- निर्माण की जो भावना तत्कालीन काव्यों में उपलब्ध है, उसके लिए कवियों / कवयित्रियों के प्रत्यक्ष या परोक्ष संघर्ष भुलाए नहीं जा सकते।
सूफी एवं भक्त कवियों ने मानवीय संवेदना तथा संवेदनात्मक अनुभूतियों को अधिक प्रामाणिक तथा मानवीय हित के लिए उपयोगी माना है। भक्तिकाव्य के कारण लोक जीवन को आस्था एवं विश्वास प्राप्त हुआ। संत एवं भक्त कवियों ने सामंती और ब्राह्मणवादी संस्कृति के विरुद्ध जन संस्कृति की प्राण- प्रतिष्ठा की। प्रेमाख्यानों को माध्यम बनाकर जायसी, मंझन, कुतबन, आदि सूफी कवियों ने प्रेम को लौकिक धरातल से उठाकर पारलौकिक बना दिया। उनका लौकिक प्रेम भी अध्यात्म के रंग से रंगा था।
मध्यकाल को ‘जागरणकाल’ कहा जाना उचित होगा। इस काल को साहित्य में ‘स्वर्णयुग’ कहा भी गया है। निस्संदेह यह जागरण धार्मिक केंद्रों से अनुप्राणित एवं विकसित हुआ। प्रत्यक्ष रूप में धार्मिक आंदोलनों ने इसे अनुप्राणित किया किंतु परोक्ष रूप में यह सामाजिक आंदोलन ही था जिसे दिशा देने के लिए अध्यात्म का संबल दिया गया। इस काल में एक और बात हुई, वह यह कि इस काल में मनुष्य के संबंध जटिल सामाजिकता से युक्त हो गए और भिन्न- भिन्न समाजों में विकसित होने के कारण उनके मानवीय हित क्रमश: एक- दूसरे के विरोधी हो गए, जिसके कारण संघर्ष और विरोध की शुरुआत हुई।मध्यकालीन काव्यों में उद्भूत मूल्यों पर नज़र डालें तो कुछ एक बिंदु उभरकर सामने आते हैं :
वर्ण / संप्रदायवाद का विरोध एवं लोक संस्कृति की स्थापना : पूर्व मध्यकालीन हिंदी साहित्य एक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन है जिसमें तत्कालीन उद्भूत सभी वादों और धाराओं का समवेत स्वर सुनाई पड़ता है। भक्तिकाव्यों के संस्कार लोक संस्कारों में प्रतिबिंबित हो गए हैं। इस युग में कला पक्ष को प्रमुखता नहीं मिली। केशवदास की रामचंद्रिका इसका प्रमाण है। मध्यकालीन युगप्रवर्तक कवियों ने वर्गीय समाज की व्यक्तिवादिता का लगातार विरोध किया और लोकहित के विचारों को अपने काव्य में प्राथमिकता दी।
भक्ति का सामाजीकरण : भक्तिकाव्यों में कवियों की विचारधारा बौद्धिक एवं लौकिक जगत के प्रति सचेत रही। इन कृतियों में मनुष्य की संवेदनात्मक अनुभूतियों को विकास का पूर्ण अवसर मिला है। इस काल के सभी प्रमुख कवि सामाजिक विचारक के रूप में उभरे। भक्ति के अंतर्गत उन्होंने मनुष्य की संकीर्ण भावनाओं को परिष्कृत करके उनकी चेतना को विस्तार दिया।
पूर्व मध्यकालीन काव्य की सहजता : पूर्व मध्यकालीन काव्य मनुष्य की सहज और स्वाभाविक मन: स्थितियों का काव्य है जो स्वार्थ और अहंकार को व्यक्तित्व- विकास का बाधक मानता है :
“कबीर कहाँ गरबिये इस जोवन की आस।
टेसू फूले दिवस चारी, खंखर भए पलास।।”
तत्कालीन मुनि- तपस्वियों के प्रति तुलसीदास की व्यंग्योक्ति :
“नारि मुई गृह संपति नासी। मूड़ मुड़ाय भये संन्यासी।।”
कवि रहीम ने कहा है :
” जो बड़ेन को लघु कहे, नहिं रहीम घटि जाहिं।
गिरिधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाहिं।।”
इन कवियों ने साधना को माध्यम बेहतर संसार की कामना की है, जहाँ मानवमात्र में समानता हो और जीवमात्र में कोई क्लेश न हो।
सामाजिक संरचना का यथार्थ : पूर्व मध्यकालीन सगुण काव्यों के नायक राम और कृष्ण कई प्रकार के सामाजिक अंतर्विरोधों एवं उतार- चढ़ाव को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनते हैं। ये ही राष्ट्रीय एकता की रक्षा करते हुए जन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं । तुलसीदास जी ने सामंती मूल्यों का विरोध कलिकाल के संदर्भ में किया, साथ ही जनसामान्य की करुण और त्रासद स्थितियों को भी चित्रित किया है :
” ऊँचे नीचे करम धरम अधरम करि
पेट ही को पचत बेटा बेटकी।”
इसी स्थिति का उल्लेख कबीर ने भी किया है :
“कोइ लरका बेचई लरकी बेचै कोइ ।
सांझा करै कबीर स्यों हरी रंग बनज करेइ।।”
सूर ने सामंती संस्कृति के अनुरूप कृष्ण छवि को स्वीकृति नहीं दी। उनके कृष्ण श्रम संस्कृति के अनुरूप प्रेम का लोक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। सूर की लोक चेतना व्यापक है। उनका उद्देश्य मानव तथा प्रकृति के कण- कण विमल प्रेम को मुखरित करना है। वर्ण- व्यवस्था के पोषक तुलसी भी आगे चलकर जाति-पांति के भेद से ऊपर उठकर प्रेम और भक्ति की गंगा बहाते हैं। जायसी सहिष्णुता, समन्वय एवं प्रेम के कवि हैं। तात्कालिक समाज में हिंदू – मुस्लिम के बीच समन्वय स्थापित करने में जायसी एवं अन्य सूफी कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार, “संतों की प्रेम साधना का उद्देश्य केवल भक्ति-प्रदर्शन मात्र नहीं था और न उसके आधार पर इष्टदेव का गुणगान ही था। उन्होंने इसे अपने जीवन का विशिष्ट अंग बना डालने की चेष्टा की और उसे व्यावहारिक रूप देना चाहा।”
पूर्व मध्यकालीन कवियों ने लोकजीवन का अभावग्रस्त रूप प्रस्तुत किया।उन्होंने साधना को सामाजिक बनाने की कोशिश की और साधना – आराधना द्वारा मानवता के स्वर मुखरित किए।
प्रकाशचंद्र गुप्त मानते हैं कि ” संत कवियों ने भारतीय जनता के दुख से द्रवित होकर साहित्य रचा और निरंतर उनके साहित्य -दर्पण में हम भारतीय जीवन की पीड़ा का प्रतिबिंब देखते हैं। जीवन की व्यथा से आकुल होकर संत कवियों ने व्यक्तिगत सुख – दुख की भावना तज दी थी किंतु उनका साहित्य सामूहिक जीवन से वैराग्य न ले सका।”14)
शाश्वत प्रेम की प्रतिष्ठा : पूर्व मध्यकालीन काव्यों में एक ओर निर्गुणपंथी सूफी संत कवि-कवयित्रियों ने ईश-प्रेम की गंगा बहाई तो दूसरी ओर कृष्णभक्त कवि-कवयित्रियों ने शाश्वत प्रेम की प्रतिष्ठा की। उनका प्रेम लौकिक होते हुए भी अध्यात्म से सना था। गुण – ज्ञानहीन विप्र – पूजा की कड़ी आलोचना तुलसी ने मानस में प्रस्तुत की, कबीर ने कदम- कदम पर धर्माडंबर का विरोध किया और सूर ने प्रेमहीन शुष्क भाववादी ज्ञान की आलोचना गोपियों से कराई :
“ऊधौ जोग सिखावन आए।
सृंगी भस्म अघोरी मुद्रा, दे ब्रजनाथ पठाए।।”
मीरा कहती है :
“अविनासी सूँ बालमा है, जिनसू साँची प्रीत।
मीरा कूँ प्रभु मिला है, एही जगत की रीत।।”
सहजोंबाई प्रेम में ही जीवन की सार्थकता देखती है :
“प्रेम दिवाने जो भये , मन भयो चकनाचूर।
छकै रहै घूमत रहै, सहजो देख हुज़ूर।।”
दयाबाई प्रेम की पीड़ा अभिव्यक्त करने में मीराबाई के समीप नज़र आती हैं :
“पंच प्रेम को अटपटो कोइय न जानत बीर।
कै मन जानत आपनौ कै लागी जेहि पीर।।”
यह पद ,मीरा के पद “घायल की गति घायल जाने की जिन घायल होय” की याद दिला देता है, जबकि एक निर्गुण तो दूसरी सगुण ईश की आराधिका है।
मालिक मुहम्मद जायसी तो प्रेम के अनूठे चितेरे कवि ही माने गए हैं :
मुहम्मद चिनगी प्रेम के
सुनि महि गगन डेराइ।
धनि बिरही औ धनि हिया,
तह अस अगिनि समाइ।।”
धार्मिक कर्मकांडों का विरोध : सामंत- विरोधी शक्तियों का जन्म जाति – वर्णगत ढाँचे के गर्भ से हुआ था। इनका विरोध सामंती शोषण तंत्र एवं कर्मकांडी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से भी था। कबीर ने सामंती मूल्यों एवं वर्णगत धर्म की कट्टर रूढ़ियों का विरोध कर भाईचारे का मार्ग प्रशस्त किया :
“जो तू बाभन बभनी जाया तौ आन राह ह्वे काहे ना आया
जो तू तुरुक तुरुकनी जाया तौ भीतरे खतना क्यूँ न कराया ”
सामाजिक रूढ़ियों के कारण धर्म का रूप विकृत हो चला। धर्म संप्रदाय के अर्थ में रूढ़ होकर खेमे में बंट गया। ऐसे में कबीर ने लोक चेतना जाग्रत कर, मानवता को नए रूप में परिभाषित किया, दूसरी ओर जायसी ने धार्मिक सहिष्णुता को व्यापक आयाम दिया है।
मूल्य का यथार्थ बोध : पूर्व मध्यकालीन काव्य यथार्थादी मूल्यों की उद्भावना के लिए प्रतिबद्ध है। लोक संस्कार मूर्त रूप में यथार्थ हो गए। रामकाव्य में दीपोत्सव और कृष्णकाव्य में फाग – होली जैसे त्योहारों का वर्णन है। इसके साथ ही पूजा- संस्कार, जादू -टोना, पेशा , पेशा आदि का वर्णन कबीर, सूर और तुलसी ने विस्तार से किया है। आम जन की व्यथा- कथा, हर्षोल्लास, शोक – विषाद उस काल की लोक चेतना का परिणाम है। नारी एवं अछुतों के प्रति जो अमानवीय व्यवहार किए जाते रहे, उसका अनुमान तुलसी की इन पंक्तियों से किया जा सकता है :
“ढोल गँवार शूद्र पशु नारी
सकल ताड़ना के अधिकारी”
“कत विधि स्रजी नारि जग माही। पराधीन सपनेहु सुख नाही।।”
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन महत्वपूर्ण है : ” धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला- लँगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रहता है। …. कर्म और भक्ति ही सारे जनसमुदाय की संपत्ति होते हैं।” 15)
निर्गुण प्रेम : कबीर, मंझन, जायसी, रहीम, नानक, दादू, मलूक, रैदास, उमा, सहजोबाई, दयाबाई सहित तुलसी, सूर, मीरा आदि कई भक्त कवियों ने निराकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम की महत्ता स्वीकारी है।
“प्रेम न खेतौं नींपजे , प्रेम न हाट बिकाइ।
राजा परजा जिस रुचै , सिर देसो ले जाई।।”
“तीन लोक चौदह खंड
सबै परै मोहि सूझि।
प्रेम छाड़ि कछु और न लेना,
जो देखो मन बूझि।।”
आचार्य शुक्ल हालाँकि कबीर के वर्ण-विरोधी आचरण के विरोधी रहे, किंतु उनके प्रेम तत्व की उन्होंने सराहना भी की है : “इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ । इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊँचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया।16)
लोक जागृति : पूर्व मध्यकालीन काव्य उच्चवर्गों का साहित्य न होकर भारतीय श्रमिक और किसान वर्ग का साहित्य है। इसे लोक जागृति का काव्य इसलिए माना गया क्योंकि इसने शोषित, पीड़ित और वंचित जन समुदाय के अचेतन पड़े मन को झकझोर कर जगाया। मीरा और रहीम के अतिरिक्त कोई भी सामंती वंश का न था। अन्य सभी समाज के कमजोर वर्ग की चेतना लेकर पैदा हुए थे। कबीर, तुलसी, जायसी, सूर एवं रहीम के काव्य लोकमंगल की भावना से ओतप्रोत हैं। सामंती व्यवस्था का विरोध कर, इन सबने प्रेम और समता को ही ध्वनित किया और कविता की सार्थकता इसी में स्वीकारी है, जिसमें प्राणीमात्र का कल्याण हो। तुलसीदास की ये पंक्तियाँ :
” कीरति भनीति भूति भल सोई।
सुरसरि सम सब कर हित होई।।”
तुलसीदास ने अपने काव्य में लोकगीतों को स्थान देकर ‘बहुजन हिताय’ की भावना को व्यापकता प्रदान की। सूर के कृष्ण के कार्यक्षेत्र को इंगित करते हुए प्रेमशंकर ने लिखा है : “सूर ने गोपियों तथा कृष्ण के माध्यम से प्रेम के मूल्य का व्यापक धरातल पर सामाजीकरण किया है तथा इसी माध्यम से बहुत से सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्यों को सहज ही स्थापित किया है। वर्णयुक्त विषाक्तता को समाप्त करने के लिए कृष्ण के माध्यम से वर्ण -जाति के भेदभाव को समाप्त करते हुए समानता तथा स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई है।इसे विद्वानों ने ‘किसान चारागाही संस्कृति का काव्य’ कहा है।”17)
सुप्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने कहा है : ” सूर … तुलसी… आदि महान साहित्यकारों ने निम्न वर्गीय समाज में रहते हुए भी जो महान कृतियाँ दी हैं, उसका कारण गरीबी नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ की सच्ची पकड़ तथा मानव – जय के प्रति अदम्य विश्वास रहा है।”18)
नैतिक मूल्यों की स्थापना : मध्यकाल में व्यापक भावभूमि आप्लावित करती वैष्णव भक्ति का मूलाधार उसके नैतिक मूल्य हैं। कबीर ने अहिंसा, सहानुभूति, सत्संग, अहंकार त्याग आदि की महिमा का उल्लेख किया है। जायसी के पद्मावत में भी नैतिक आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। सूरदास ने ‘सूरसागर’ में वर्णित विनय के पदों में भी आचार, निष्ठा, नियम तथा आदर्श आदि मानवीय गुणों का प्रतिपादन किया है और तुलसीदास ने तो पग-पग पर नैतिकता का पूर्ण आख्यान किया है। रहीम ने आत्माभिमान की रक्षा पर बल देते हुए कहा है :
” रहिमन पानी राखिये , बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे मोती मानूष चून।।”
लोकभाषा को महत्ता : पूर्व मध्यकालीन काव्य एक युगांतर चेतना को जनसामान्य की बोली में रचनात्मक आधार बनाकर प्रस्तुत करता है। यह संस्कृतीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण बोली भाषा की सहगामिनी बनी। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी — सभी ने लोकभाषा को महत्व दिया। कबीर की भाषा में खड़ी बोली , पंजाबी, ब्रज एवं पूर्वी हिंदी का मिश्रण पाया जाता है जबकि जायसी सहित अन्य सूफी कवियों की भाषा ठेठ अवधी ही रही। पद्मावत के उपसंहार खंड में वे कहते हैं :
“केइं न जगत जस बेचा
केइं न लीन्ह जस मोल।
जो यह पढै कहानी
हस सँवरे दुइ बोल।।”
सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों ने ब्रजभाषा को अपनाया तो तुलसी ने ब्रज और परिष्कृत अवधी को जगह दी। मीरा के पद राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में हैं जबकि उस समय फ़ारसी को राजा का आश्रय प्राप्त था और संस्कृत को विद्वानों का । संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी तुलसीदास ने जनभाषा को अपनाया। कुछएक रचनाओं में प्राकृत-अपभ्रंश मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग दिखाई देता है। ये समस्त उपभाषाएँ लोक वर्ग से जुड़ी थीं और लोक मानस के निकट होने के कारण जागृति का शंख फूँकने में अपेक्षाकृत अधिक सहायक थीं। भाषा वस्तुत: एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस काल के कवि- कवयित्रियों ने देश में बिखरी जनभाषा को लोक सम्मत व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की। भाषा किसी भी क्रांति का संवाहक होती है और क्रांति की सफलता का महत्वपूर्ण स्तंभ भी, इस तथ्य से उस युग के संत और भक्त कवि भली – भाँति परिचित थे।इसलिए भिन्न- भिन्न मार्ग पर चलते हुए भी एक लक्ष्य के प्रति उनकी साधना आज सिद्ध हो चुकी है।
अत: पूर्व मध्यकालीन काव्य को ‘भक्तिकाव्य’ कहना उसकी विराटता को संकुचित सीमा में बाँधने जैसा होगा,जो उचित नहीं है। उस संक्रांत युग में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि पर साहित्य द्वारा जिन मूल्यों की उद्भावना हुई, वे न केवल धार्मिक , बल्कि नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं शाश्वत मानवीय मूल्य रहे , जहाँ जीवमात्र से प्रेम और सौहार्द्र भाव की स्थापना की जाती है। सत्या, अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, ईमान आदि शाश्वत मूल्यों की स्थापना / पुनर्स्थापना के साथ ही अहंकार, द्वेष, अतिशय काम भावना , अनाचार, लोभ, हिंसा, जातिवाद, धार्मिक आडंबर से संबद्ध तत्कालीन स्थापित मूल्यों को त्यागने पर बल दिया जाता है। चारों दिशाओं से गुंजित जो एक स्वर सुनाई देता है, वह है — मानवमात्र में एकता, समता, प्रेम, परस्पर सम्मान, और जीवमात्र के प्रति प्रेम और दया का भाव। ये ही वे शाश्वत मूल्य हैं जो समसामयिक परिस्थितियों में भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी रहेंगे।
संदर्भ :
मुक्तिबोध : एक साहित्यिक डायरी, पृ. 6
बलवीर सिंह गौंछवाल : प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स , पृ. 19
वीरेंद्र मोहन : भक्तिकाव्य और मानव मूल्य, पृ. 19
नेमिचंद जैन : बदलते परिप्रेक्ष्य, पृ. 13
संचेतना : विचार कविता अंक, वेणु गोपाल का लेख, पृ. 80
के. एस. लाल : स्टडीज़ इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, पृ. 214
अब्दुर्राहमान इब्ने खलदून : इब्ने खलदून का मुकदमा, पृ. 124-125
एस. एम. ज़फ़र : सम कल्चरल आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, पृ. – 20-21
सय्यद नूरल हसन : थॉट्स ऑन एग्रेरियन रिलेशंस इन मुग़ल इंडिया, पृ. — 3
अबुल फ़ज़ल : अकबरनामा, ज़िल्द 2, पृ. – 35
इरफ़ान हबीब : द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया , पृ. 90
प्रेमशंकर : भक्तिकाव्य की भूमिका, पृ. 35
परशुराम चतुर्वेदी : हिंदी काव्य में प्रेम प्रवाह, पृ. – 61
प्रकाशचंद्र गुप्त : साहित्यधारा, पृ. – 48
रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ. – 42
रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ. – 46
प्रेमशंकर : कृष्णकाव्य और सूर, पृ – 130
नामवर सिंह : इतिहास और आलोचना