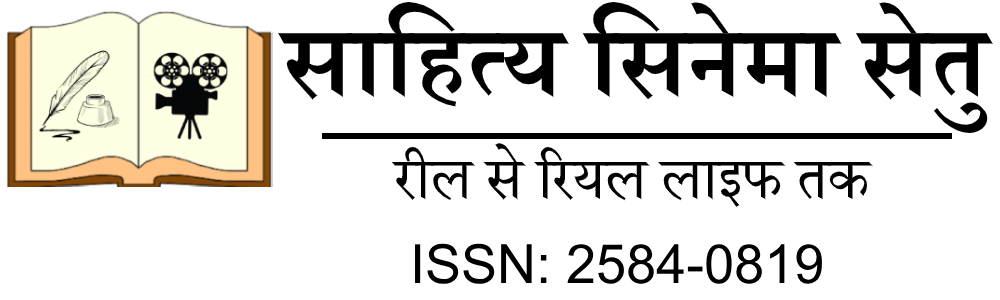आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है- आदिम युग में रहने वाली जातियां। मूलतः यह वे जातियां है जो 5000 वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता को संजोयें हुए है। आदिवासी भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी है। मूल निवासी होने के कारण इन्हें सामान्यतः आदिवासी कहा जाता है। आर्य ग्रंथों में इन्हें असुर, दास, दैत्य, राक्षस, दानव, यातुधानआदि नामों से पुकारा जाता था। आदिवासी राजा महाराजा यहाँ के शासक रहे है, इनके बड़े बड़े महल नगर हुआ करते थे उस महान सभ्यता के अवशेष आज मिलते है इसके साथ कुशल कारीगर और कलाकार भी थे, सभ्यता व संस्कृति में दक्ष तथा मने हुए शूरवीर योद्धा थे। जनजाति शब्द की उत्पत्ति तथा अर्थ के बारे में विभिन्न विचारको के अपने मत है। व्युपत्ति शास्त्र के अनुसार अंग्रेजी शब्द ‘ट्राईब’ (जनजाति) की उत्पत्ति त्रिभुज शब्द से मानी जाती है। जिसका अर्थ तीन अंगहै राजा, रक्षा और हस्त कलाकार रोमवासियों के लिए ‘ट्राईब’ एक राजनितिक संस्था के रूप में था।
आदिवासी रंगमंच में आदिवासियों के रहन-सहन, वेश-भूषा, बोली-भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति, उन्के विश्वासों, अंधविश्वासों, परिश्रम ज़िन्दगी, उनकी रुचिओं, उनके खेल, पर्व, त्यौहार, नृत्य, खेल, लोकगीत, लोककला, लोकसंगीत के प्रति उनका प्रेम, प्रकृति के साथ उनका निकट सम्बन्ध, अस्मिता एवं अस्तित्व के लिए उनका संघर्ष, बाहरी दुनिया के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा, उनकी सामूहिक संगठन शक्ति, उनकी सहजता व सरलपन, उनका भोलापन व मनुष्यता और अन्य समाज में स्वयं को स्थापित करने की विवशता, लोकधुनों में खोये रहने की प्रवृत्ति एवं शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता आदि इनके रंगमंच में निहित है।
आदिवासियों के बारे में बहुतेरे साहित्य लिखे गये, लिखे भी जा रहे हैं। उसका अपना महत्व है लेकिन साहित्य वे पढ़ नहीं पाते जबकि नाटक के जरिये वे सीधे संवाद स्थापित करते हैं और अपनी चुनौतियों को एक स्वर देने के लिए प्रेरित होते है। आदिवासी रंगमंच आदिवासी मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने का प्रयास है। आदिवासी रंगमंच की इसी अवधारणा एवं परिकल्पना को साकार रूप देने हेतू 2012 में झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा ने दलित एवं आदिवासी नाट्य समारोह आयोजित किया जिसमें देशभर के दलित-आदिवासी रंगमंच एवं साहित्य के वरिष्ठ एवं नवीन सृजनधर्मियों ने शिरकत की। आयोजन का उद्देश्य समाज एवं रंगमंच में उपेक्षित दलित-आदिवासी मुद्दों पर विमर्श तेज करना और समकालीन दलित-आदिवासी रंगभाषा को गति देना था जिससे कि वंचित भारतीय समाज के अधिकारों के लिए हो रहे संघर्ष और सृजन को मजबूती मिल सके। सामंती और पूंजीवादी पितृसत्तात्मक वर्चस्व की रंगमंचीय राजनीति के खिलाफ यह आयोजन हुआ। आयोजन में आदिवासी रंगमंच की रंगभाषा पर विशेष चर्चा हुई।
आदिवासी रंगमंच की विशेषता इसका प्रस्तुति स्वरुप है. आदिवासी मुद्दों पर केंद्रित इन नाट्य प्रस्तुतियों में आदिवासी समुदाय की भाषा कला एवं संस्कृति का मंचीय प्रयोग करते हुए आदिवासी मुद्दों को सशक्त तरीके से जनता तक पहुंचाया जाता है। कई नाट्य प्रस्तुतियों में कलाकार स्वयं उसी समुदाय से होने के कारण नाटक अत्यंत जीवंत हो जाता है। यही मुख्य बिंदु आदिवासी रंगमंच को अन्य रंगमंच से अलग करता है। झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा-अखड़ा झारखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा है। एक ऐसी सामूहिक पंरपरा जो सिर्फ सहअस्तित्व और सहभागिता में विश्वास ही नहीं रखता है बल्कि उसे जीता है। झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा इसी पारंपरिक विरासत और मूल्यबोध को बचाये रखने के लिए कृतसंकल्प है। आदिवासी चिंतक और रंगकर्मी अश्विनी कुमार पंकज कहते हैं- मेनस्ट्रीम के नाटकों में या तो आदिवासियों के मुद्दे उठते ही नहीं हैं या बहुत कम उठाए जाते हैं। जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के शोषण की सैकड़ों कहानियां हैं। उन्होंने बताया कि साल 2000 से पहले तक आदिवासियों के मुद्दों पर गिने- चुने नाटक होते थे। पर, नेशनल लेवल पर जो पहला नाटक आदिवासियों के लिए मंचित हुआ, वह 2009 में मंचित नाटक फेविकोल था।
हृषीकेश सुलभ हिंदी के जाने-माने नाटककार और रंगसमीक्षक हैं। ‘धरती आबा’ 2010 में प्रकाशित उनका प्रसिद्द नाटक है। परन्तु इसका मंचन सर्वप्रथम 2007 में संजय उपाध्याय द्वारा किया गया। भारत के युवा आदिवासी विद्रोही और उलगुलान के नायक बिरसा मुण्डा के जीवन पर केन्द्रित ‘धरती आबा’ एक महत्वपूर्ण नाट्यकृति है। ‘धरती आबा’ लेखक की अपनी जातीय, भाषिक व सांस्कृतिक भूमि से बिल्कुल भिन्न और प्रतिरोधी छोर पर अवस्थित समाज-संस्कृति के नायक की ऐतिहासिक गाथा है। आदिवासी पृष्ठभूमि पर केन्द्रित यह नाटक कई आयामों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। संजय उपाध्याय द्वारा निर्देशित ‘धरती आबा’ को मंचित करना उनके लिए स्वप्न की तरह था बिरसा उन व्यक्तियों में शामिल रहे है जिन पर केन्द्रित नाटक करने की चाहत निर्देशक के भीतर भी पलती रही। बिरसा के जीवन काल में ही उनको लेकर कई प्रथाएं प्रचलित थी। इन प्रचलित कथाओं के कुहासे को हटाकर नाटक का मंचन बिना एक सुगठित आलेख के संभव नहीं था। ‘धरती आबा’ नाटक के गठन में एक ऐसी रंगभाषा छिपी हुई है जो कई नाटकीय तनावों की रचना करती है संजय जी ने सहजता और सरलता को अपनी रंग संरचना का आधार बनाया है।
संगीत और नृत्य हमारे जनजातीय समाज के जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। ‘धरती आबा’ की प्रस्तुति में भी संगीत और नृत्य का एक साथक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। वस्त्र, वेशभूषा, केश-विन्यास और जनजातीय जीवन की स्थानीयता भी इस नाटक की युक्ति है। बिरसा के बहाने एक गुज़रे हुए कालखंड और जनजातीय समाज की स्वतंत्रता की लालसा ही नहीं, समस्त मानव समाज की मुक्ति की लालसा भी धरती आबा का लक्ष्य है। जीवन के दुःख संघर्षों को जन्म देते है और ऐसे संघर्षों से ही मनुष्यता की रक्षा होती है रंगकर्म के माध्यम से बिरसा मुंडा जैसे नायकों की समाज में पुनर्स्थापना आज समय की ज़रूरत है। ‘धरती आबा’ के माध्यम से हम केवल इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान को भी जानेंगे। जीतराई हांसदा झारखंड के कोल्हान इलाके से ताल्लुक रखते हैं। जीताराई हांसदा का नाटक ‘फेविकोल’ आदिवासियों की जमींनों का पूंजीपति द्वारा हड़पने तथा जमीन के लिए आदिवासी विद्रोह पर केन्द्रित है। आदिवासियों के मुद्दों को लेकर सटीक बैठता है। नाटक का परिवेश सीमित नहीं है इसमें सम्पूर्ण विश्व के आदिवासियों की व्यथा को सम्मिलित किया है। आदिवासी पृष्ठभूमि पर आधारित दोनों नाटक एक शताब्दी में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से हुए बदलाव को रेखांकित करते हैं। जहाँ ‘धरती आबा’ नाटक का कथ्य सुरेश सिंह की पुस्तक ‘बिरसा मुंडा और उनका आन्दोलन’ और महाश्वेता देवी के उपन्यास ‘जंगल के दावेदार’ पर आधारित है। वहीं जीतराई हांसदा का नाटक ‘फेविकोल’ नाट्यकार के स्वानुभूति एवं आस-पास के परिवेश से निर्मित है जिसमें नाट्यकार ने पूंजीवादी शोषण और अपने ही जड़-जंगल-जमीन से विस्थापित हो रहे आदिवासी समुदाय की त्रासदी को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है जो न केवल भारत अपितु सम्पूर्ण विश्व की आदिवासी संवेदना से जाकर जुड़ता है। जीतराय हांसदा कहते हैं कि मेनस्ट्रीम के मीडिया आदिवासियों के मुद्दे नहीं उठाते और उठाते भी हैं, तो उनमें रियलिटी की कमी होती है। वह कहते हैं- डेवलपमेंट का जो तथाकथित मॉडल है, वह आदिवासियों का विनाश कर रहा है। यही वजह है कि अपने हक के लिए हमें नाटकों का मंचन करना पड़ रहा है। फेविकोल में हमने आदिवासियों के विस्थापन और पहचान का मुद्दा उठाया था। इसमें छत्तीसगढ़, असम और ओडि़शा के आदिवासियों का दर्द दिया है, पर असल में यही दर्द सभी आदिवासियों का है। पिछले कुछ दशकों में जिस प्रकार नारीवादी रंगमंच, दलित रंगमंच इत्यादि बखूबी उभर कर आए उस दृष्टि से आदिवासी रंगमंच अत्यंत ही नवीन क्षेत्र है। पिछले दो दशकों से आदिवासी मुद्दों को केंद्र में रखकर नाटकों का लेखन हुआ जिसमें विभिन्न भाषाओँ के नाटककार शामिल है। मणिपुर, असाम, झारखंड, महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत के राज्यों में आदिवासी मुद्दों पर नाटकों की रचना हुई अपने सामाजिक परिवेश को इन नाटकों ने बखूबी रेखांकित किया। रंगमंच पर आदिवासी नाटकों की कई प्रस्तुतियाँ भी हुई इसको एक मंचीय अवधारणा के रूप में 2012 में झारखण्ड रांची में झारखंड आदिवासी अखाड़ा समिति ने आदिवासी रंगमंच के नाम से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें दलित रंगमंच की भांति आदिवासी रंगमंच के स्वरुप पर भी गंभीरता से सोचा गया। आदिवासी नाट्य साहित्य पर संपूर्ण भारत में कार्य हुए परंतु अकादमिक जगत में आदिवासी रंगमंच को केंद्र में रखकर कोई कार्य नहीं हुआ। आज भी इस पर आवश्यकता महसूस की जा रही हैं अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम के रूप में रंगमंच ने जनवादी स्वरुप की कल्पना को साकार करने का साथ तो दिया लेकिन आदिवासी समाज को सूचना शिक्षा मनोरंजन के अलावा व्यक्तित्व निर्माण में जनमाध्यमों की आवश्यकता हैं। जिससे आदिवासी समाज बौद्धिक वैचारिक रूप से सशक्त होकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। आदिवासी जीवन शैली के आधार पर समता मूलक समाज की स्थापना और भारतीय संविधान की आधारशिला भी समता न्याय बंधुता की नींव पर है।
निष्कर्ष:- इक्कीसवीं सदी में भी आदिवासी पृष्ठभूमि पर आधारित कई नाटकों की रचना हुई है। लेकिन इन नाटकों के लेखन और प्रस्तुतिकरण के बीच तथाकथित जातिवादी बुद्धिजीवियों का तबका जाति आधारित समाज की स्थापना पर विश्वास करते हुए रंगमंच में आदिवासी माध्यमों और उत्कृष्ट जीवन शैली को नजरअंदाज करने का बीड़ा उठा रहे है। लेकिन दलित आदिवासी बहुजन परंपरा के नायकों में फुले आंबेडकर बिरसा द्वारा किये गए कार्यों की छवि ने कई चर्चित निर्देशकों, कलाकारों का ध्यान इस ओर खींचा हैं। आदिवासी रंगमंच को मुख्य धारा के समाज में जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी यह मुख्य धारा के रंगमंच से सीधे रूप में नहीं जुड़ पाए है। आदिवासी रंगमंच प्रस्तुतियों पर शोध की अनिवार्यता का आभास किया जा सकता है। आज का आदिवासी रंगमंच अस्तित्व व अस्मिता का भी रंगमंच है। जिससे इस समुदाय की परम्परा रूढ़ियाँ, संस्कृति, अन्याय, वेदना, पीड़ा, आक्रोश, शोषण आदि सभी कुछ बयां हो रहा है। लोककला, संगीत, नृत्य, संस्कृति, भाषा, बोली आदि विभिन्न धरातल पर आदिवासी रंगमंच एक व्यापक रंगमंच की और भी अग्रसर हो रहा है।
संदर्भ सूची
पत्र पत्रिकाएँ
- रंग वार्ता- आदिवासी रंगमंच विशेषांक, 2012
- रंग विमर्श पत्रिका – भारंगम २०१५ (मात्रा के ढेर में गूढ़वत्ता ढेर )
- एक सिलसिला पत्रिका – सितम्बर २०१३ (रंगमंच की संभ्रांत दुनिया में आदिवासी सवालो की दस्तक )
- भारतीय रंगमंच –Https/:/hi.wikipedia.org/s/6dxa
- “दस्तक “ की ब्लॉग पत्रिका ‘मंडली ‘(मार्च ) २०१२
- मोहल्ला live पत्रिका (सांस्कृतिक संघार के विरुद्ध भाषा कर रहीं है दाब ) मार्च २०१३
- ADTR ब्लॉग अभिलेखा गार (आदिवासी न्रत्य रंगमंच)
- आदिवासी साहित्य पत्रिका- अक्टूबर २०१५-मार्च २०१६।
पुस्तक सूची
१. संपादक प्रफ्फुल शिलेदार , आदिवासी साहित्य अस्मिता बोध भुजुंग मेश्राम , लोक वाद्यम ग्रह , मुंबई प्रथम संस्करण अप्रैल २०१४.
२. डॉ. गारे गोविन्द, महाराष्ट्रातील आदिवासी जमाती , कॉन्टिनेंटल प्रकाशन , पुणे , प्रथम संस्करण २०००
३. गायकवाड़ दीपक , आदिवासी चळवळ स्वरुप व् दिशा , सुगावा प्रकाशन , पुणे, प्रथम संस्करण २००५
४. डॉ. गावित महेश्वरी , आदिवासी साहित्य विविधांगी आयाम , चिन्मय प्रकाशन , औरंगाबाद प्रथम संस्करण २०१५
५. सम्पादक वि कृषण , सिंह भीम , आदिवासी विमर्श , स्वराज प्रकाशन , नई दिल्ली प्रथम संस्करण २०१४
६. पाण्डेय गया , भारतीय जनजातिय संस्कृति , कांसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी , नई दिल्ली प्रथम संस्करण २००७
७. सम्पादक गुप्ता रमणिका , आदिवासी कौन ,राधा कृष्ण प्रकाशन , नई दिल्ली , प्रथम संस्करण २००८
८. निर्मल कुमार बोस, ‘भारतीय आदिवासी जीवन’, राष्ट्रीय पुस्तकन्यास, भारत, पहली आवर्ती, २०१४