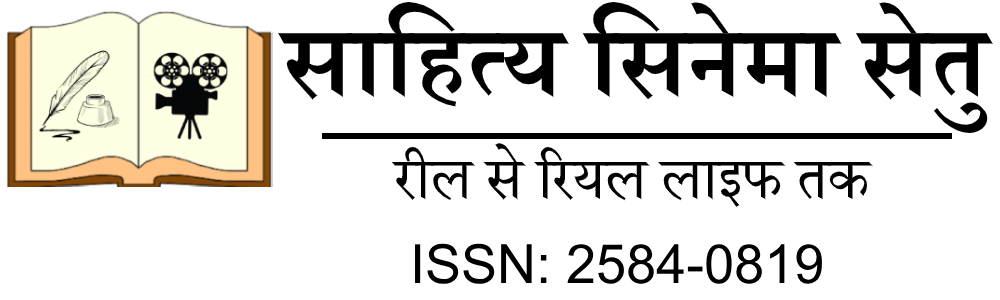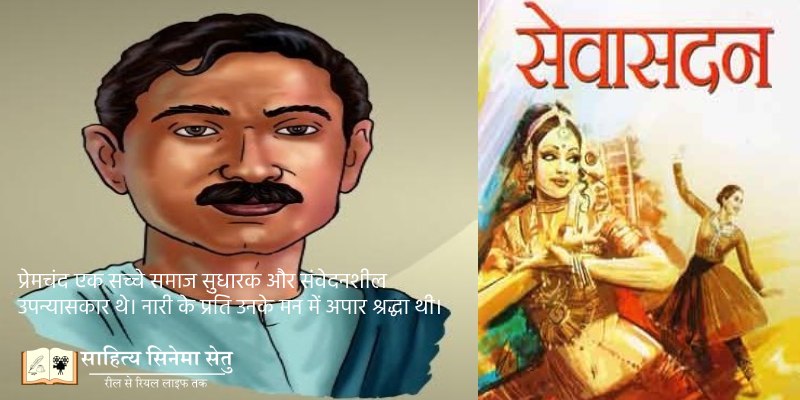सामाजिक सरोकारों से ओत-प्रोत प्रेमचंद द्वारा रचित ‘सेवासदन’ उपन्यास की रचना आज से लगभग सौ साल पहले 1918 में की गई थी। उर्दू में इस उपन्यास का प्रकाशन 1919 में ‘बाज़ारे-हुस्न’ के नाम से हुआ था। प्रेमचंद अत्यंत संवेदनशील उपन्यासकार थे, मानव जीवन के प्रति उनका अपना एक अलग नज़रिया था। जिसका प्रमाण उन्होंने अपने उपन्यासों में मानव चरित्र की स्वाभाविक सबलता और दुर्बलता का यथार्थ चित्रण कर दिया है। प्रेमचंद के सम्बन्ध में डॉ० कमल किशोर गोयनका लिखते है कि-“प्रेमचंद हिन्दी उपन्यास साहित्य में युगसृष्टा के रूप में विख्यात हैं। हिन्दी उपन्यास को तिलिस्म और जासूसी कथा-कहानी के कुहासे से बाहर निकालकर यथार्थ की भूमि पर अवस्थित करने का श्रेय उन्हीं को है। प्रेमचंद ने भारतीय जनजीवन को जिस रूप में देखा-परखा था, उसका यथावत सही चित्रण करने का बीड़ा उठाया और उसमें सफलता के चरम बिन्दु का स्पर्श भी किया।”1 हिन्दी साहित्य जगत में प्रेमचंद एक ऐसा नाम है, जो आज भी बच्चों से लेकर बूढों तक की जबान पर है। उनके पात्र इस बात की मजबूती से पुष्टि करते हैं कि चौथी, पाँचवी कक्षा में पढ़ी हुई उनके साहित्य के पात्र पाठकों के जेहन में आज भी अपनी जगह बनाए हुए है। प्रेमचंद हिन्दी के युग प्रवर्तक थे। नारी के प्रति उनके मन में स्वाभाविक श्रद्धा थी। जितनी शिद्दत से उन्होंने अपने साहित्य में समाज की कुरीतियों पर अपनी लेखनी चलाई, उतनी ही सूक्ष्म दृष्टि से नारी जाति की समस्याओं को पाठकों के सामने रखा। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में-“प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पेषित कृषकों की आवाज़ थे; पर्दें में कैद पद-पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबर्दस्त वकील थे; गरीबों और बेकसों के महत्त्व प्रचारक थे।”2
‘सेवासदन’ उपन्यास द्वारा लेखक ने भारतीय नारी जाति की परवशता, निस्सहाय अवस्था, आर्थिक एवम् शैक्षणिक परतंत्रता का अत्यंत निर्ममता एवम् वीभत्सता के साथ चित्रण किया है। नारी-जीवन की विविध समस्याओं के साथ-साथ धर्माचार्यों, सुधारकों के आडंबर, ढोंग, पाखंड, चरित्रहीनता, दहेज-प्रथा, बेमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, खोखले मान-सम्मान की रक्षा के लिए परिवार की तबाही, साम्प्रदायिक द्वेष इत्यादि सामाजिक विकृतियों का वर्णन इस उपन्यास में जगह-जगह देखने को मिलता है। उपन्यास की नायिका सुमन समाज के इसी द्वेष के कारण जीवन-भर संघर्ष करती नज़र आती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिन्दी उपन्यास साहित्य में वेश्या समस्या का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। लेकिन अन्तर केवल इतना है कि प्रेमचंद युग से पूर्व के उपन्यासकारों ने वेश्या का चित्रण घृणित पात्र के रूप में किया गया था, जबकि प्रेमचंद युग में उपन्यासकारों ने उसे सहानुभूति देकर, मानवतावादी दृष्टिकोण से उसका वर्णन किया। इसका जीता-जागता प्रमाण हमें प्रेमचंद के उपन्यास ‘सेवासदन’ में मिलता है जहाँ पहली बार मानवतावादी धरातल के आधार पर वेश्या का चित्रण हुआ और उसे सहानुभूति भी मिली। प्रेमचंद ने समाज के सामने इस तथ्य को उजागर किया कि घृणा की पात्र सुमन नहीं वरन् हमारा समाज ही है, जिसने उसे वेश्या बनने के लिए बाध्य किया। सम्पूर्ण उपन्यास उसी के चरित्र के ईद-गिर्द घूमता हैं। प्रेमचंद ने सुमन के स्वभाव का वर्णन इस प्रकार किया है-“बड़ी लड़की सुमन सुंदर, चंचल और अभिमानी थी। छोटी लड़की शांता भोली, गंभीर, सुशील थी। सुमन दूसरों से बढ़कर रहना चाहती थी। यदि बाजार से दोनों बहनों के लिए एक ही प्रकार की साड़ियाँ आतीं तो सुमन मुँह फुला लेती थी।”3
सुमन के पिता अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी। जब सुमन के विवाह की बात चली और वर पक्ष की ओर से दहेज़ की माँग सुनकर वे हिम्मत हार बैठते थे, क्योंकि इतना दहेज़ देने का सामर्थ्य उनमें नहीं था और दहेज़ समाज में ऐसा रोग था जो कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। दहेज़ की रकम चुकाने में सक्षम न हो पाने के कारण एक ईमानदार पिता को अपना ईमान तक बेचना पड़ा, क्योंकि शिक्षित सज्जनों को उनसे सहानुभूति तो थी पर बिना दहेज़ के कोई उसकी बेटी सुमन से शादी करने को तैयार नहीं था। एक सज्जन ने तो उसके पिता से यह तक कह दिया कि-“ महाशय, मैं स्वयं इस कुप्रथा का जानी दुश्मन हूँ। लेकिन करूं क्या अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, दो हज़ार रुपये केवल दहेज़ में देने पड़े, दो हज़ार खाने-पीने में खर्च पड़े, आप ही कहिए, यह कमी कैसे पूरी हो?”4 इस तरह दहेज़ के लोभ को पूरा करने के चक्कर में उसके पिता को रिश्वत लेना पड़ा और इसका भेद खुलने पर उन्हें ज़ेल जाना पड़ा।
इन सबके बीच सुमन का विवाह गरीब गजाधर प्रसाद से कर दिया जाता है। बेमेल विवाह और गरीबी के कारण पति-पत्नी के रिश्तों में मन-मुटाव शुरू हो जाता है और एक रात अपनी सेहली सुभद्रा के घर से आने में देरी होने के कारण संकीर्ण मनोवृत्ति वाले पति द्वारा निष्कासन मिला। सुमन ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की पर उसका पति उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था, इतना ही नहीं वह उसका नाम उसकी सेहली के पति पद्मसिंह से जोड़कर उसके चरित्र पर लांछन लगाने लगा। गजाधर के शब्दों में-“चल छोकरी, मुझे न चरा, ऐसे-ऐसे कितने भले आदमियों को देख चुका हूँ। वह देवता हैं, उन्हीं के पास जा। यह झोपड़ी तेरे रहने योग्य नहीं है। तेरे हौसले बढ़ रहे हैं। अब तेरा गुजारा यहाँ न होगा।”5
पति द्वारा निकाल दिए जाने पर अगर वह चाहती तो भोली बाई के कोठे पर जा सकती थी, पर उसके संस्कार ही थे जिसने उसे ऐसा करने से रोका। एक अबला स्त्री जिसे पति द्वारा घर से निकाल दिया गया हो, वह भला सड़कों पर सुरक्षित रह सकती थी। इसलिए सुमन ने अपनी सेहली सुभद्रा के पास जाना सही समझा, पर वहाँ भी वह अधिक दिन तक रह पाई, क्योंकि सुभद्रा के पति पद्मसिंह ने लोकोपवाद के डर से उसे अपने घर से जाने को बोल दिया। जब सब जगह ही द्वार बंद हो गए थे, ऐसे में भोली बाई ने उसे सहारा दिया। वह सिलाई का काम करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहती थी, पर पुरुष की कामुक प्रवृत्ति ने उसे वहाँ भी जीने नहीं दिया और समाज की खोखली नैतिकता ने उसे भी वेश्या बना दिया।
यहाँ उपन्यास हमें यह सोचने को विवश कर देता है कि सुमन को वेश्या बनाने के लिए आख़िर जिम्मेदार कौन है? क्या वह समाज जहाँ वह जन्मी और उसने अपने यौवन की दहलीज पर पाव रखा। पद्मसिंह इस समस्या के लिए उत्तरदायी मध्यवर्गीय समाज को मानते है। उनके कथनानुसार-“लोग वेश्याओं को बुलातें हैं, उन्हें धन देकर उनके सुख-विलास की सामग्री जुटाते और उन्हें ठाट-बाट से जीवन व्यतीत करने योग्य बनाते हैं, वे उस कसाई से कम पाप के भागी नहीं हैं जो बकरे की गर्दन पर छुरी चलाता….सैकड़ों स्त्रियाँ जो हर रोज़ बाज़ार में झरोखे में बैठी दिखायी देती हैं, जिन्होंने अपनी लज्जा और सतीत्व को भ्रष्ट कर दिया है, उनके जीवन का सर्वनाश करने वाले हमीं लोग हैं।”6 उपन्यास का एक अन्य पात्र अनिरुद्ध सिंह इसका दोष शिक्षित मध्यवर्ग को ही मानता है-“हमारे शिक्षित भाइयों की बदौलत दालमण्डी आबाद हैं, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक हैं? वह मीना बाज़ार हम लोगों ने ही सजाया हैं।”7
वेश्या रूप में सुमन को जीवन के कटु यथार्थ का आभास होता है। उसका सामना समाज के खोखलेपन और झूठे दिखावेपन से होता है। वह यह भली-भाँति देख लेती है कि-“जितना आदर मेरा अब हो रहा है उसका शतांश भी तब नहीं होता था। एक बार मैं सेठ चिम्मनलाल के ठाकुरद्वारे में झूला देखने गई थी, सारी रात बाहर खड़ी भीगती रही, किसी ने भीतर नहीं जाने दिया, लेकिन कल उसी ठाकुरद्वारे में मेरा गाना हुआ तो ऐसा जान पड़ा था मानों मेरे चरणों से वह मन्दिर पवित्र हो गया।”8 विठ्ठलदास सुमन से मिलने जाते है और उसे समझाने का प्रयास करते है कि वह जो कुछ कर रही है, वह ठीक नहीं है, उसकी वजह से हिंदू जाति का सिर नीचा कर दिया है। इस पर सुमन उन्हें इस प्रकार उत्तर देती है –आप ऐसा समझते होंगे; और तो कोई ऐसा नहीं समझता। अभी कई सज्जन यहाँ से मुजरा सुनकर गये हैं, सभी हिंदू थे, लेकिन किसी का सिर नीचा नहीं मालूम होता था। वह मेरे यहाँ आने से बहुत प्रसन्न थे। फिर इस मण्डी में मैं ही एक ब्राह्मणी नहीं हूँ, दो-चार का नाम तो मैं अभी ले सकती हूँ, जो बहुत ऊँचे कुल की हैं, पर जब बिरादरी में अपना निबाह किसी तरह न देखा तो विवश होकर यहाँ चली आयी। जब हिंदू जाति को खुद ही लाज नहीं है तो फिर हम जैसी अबलाएँ उसकी रक्षा कहाँ तक कर सकती है।”9 इसके साथ यहाँ आने के बाद वह इस सत्य को भी समझ चुकी थी कि भोगलिप्सा ही जीवन में सब-कुछ नहीं है। अभी तक उसके इस कोठे में कोई ऐसा भला मनुष्य नहीं आया था, जो उसे इस दलदल से निकालना चाहता हो, पर विठ्ठलदास को यहाँ देखकर उसे सच्चे समाज सुधारक के दर्शन हो गए थे। सुमन कहती है -“आप सोचते होंगे कि भोग-विलास की लालसा से कुमार्ग में आयी हूँ, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं ऐसी अंधी नहीं कि भले-बुरे की पहचान न कर सकूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने अत्यंत निकृष्ट कर्म किया है लेकिन मैं विवश थी, इसके सिवा मेरे लिए और कोई रास्ता न था।”10
सुमन विठ्ठलदास से कहती है कि वह भी यह सब छोड़ना चाहती है, पर फिर उसका जीवन निर्वाह किस प्रकार होगा, उसे इसके बारे में भी सोचना होगा। जीवन में ठोकर खाने के बाद अब वह सच्चाई को समझने लगी है। वह वेश्यावृत्ति को तृष्णा सागर कहती है। वह कहती है-“यहाँ या तो अंधे आते हैं या बातों के वीर। कोई अपने धन जाल बिछाता है, कोई अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का। उनके हृदय भाव-शून्य, शुष्क और ओछेपन से भरे हुए होते हैं।”11
परिणामसवरूप वह वेश्यालय को हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प लेती है। इसके साथ ही, वेश्या रूप में उसे प्रेम रूपी सत्य का आभास होता है। सदन नाम का युवक उसके कोठे पर आया करता था, जिससे उसे प्रेम हो गया था। “सुमन इस समय सदन के प्रेमजाल में फँसी हुई थी। प्रेम का आनंद उसे कभी नहीं प्राप्त हुआ था, इस दुर्लभ रत्न को पाकर वह उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। यद्दपि वह जानती थी कि इस प्रेम का परिणाम वियोग के सिवा और कुछ नहीं हो सकता।”12 इसलिए दालमंडी का त्याग करते हुए उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि प्रेम का आधार त्याग ही है। अंतत: वह यह निश्चय करती है कि स्वार्थ रहित प्रेम पाने की बजाय वह अपने प्रेमी की यादों को दिल में समेट रखेगी। वह सदन को बिना बताए दालमण्डी छोड़ने का फैसला लेती है।
विठ्ठलदास और पद्मसिंह के प्रयासों के कारण अब सुमन सब कुछ छोड़ कर विधवाश्रम में रहने लगती है। लोग अब उसकी कर्मनिष्ठा को देखकर चकित रह जाते हैं। वह अब अपने किये कर्मों पर पश्चाताप करती है। जिस प्रकार कोई रोगी क्लोरोफ़ार्म लेने के पश्चात होश में आकर अपने चींरे फोड़े के गहरे घाव को देखता है और पीड़ा तथा भय से फिर मूर्छित हो जाता है, वही दशा इस समय सुमन की था।”13 इतना कुछ होने के बाद भी सुमन के सामने एक बार फिर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी बहन का विवाह उसके प्रेमी सदन के साथ होना तय होता है, पर सुमन की वेश्या होने की खबर का पता चलने पर सदन के माता-पिता इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं और बिना शादी के बारात लौट जाती है। सुमन के पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते है, वह नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेमचंद ने उनकी इस आत्महत्या के पीछे छिपे धर्म के ठेकेदारों पर कटाक्ष करते हुए लिखा है-“आजकल धर्म तो धूत्तों का अड्डा बना हुआ है। इस निर्मल सागर में एक-से-एक मगरमच्छ पड़े हुए हैं। भोले-भाले भक्तों को निगल जाना उनका काम है। लम्बी-लम्बी जटाएँ, लम्बे-लम्बे तिलक छापे और लम्बी-लम्बी दाढ़ियां देकर लोग धोखे में आ जाते हैं, पर वह सब के सब महापाखण्डी, धर्म के उज्ज्वल नाम को कलंकित करनेवाले, धर्म के नाम पर टका कमानेवाले, भोग-विलास करने वाले, पापी हैं।”14
लेखक ने इस प्रसंग के माध्यम से समाज को यह समझाने की कोशिश की है, जिस धर्म के नाम पर सुमन के पिता ने आत्महत्या की, क्या यह वही धर्म है जिसने सुमन को वेश्या बनने पर मज़बूर कर दिया? सुमन की बहन शांता उसके साथ विधवाश्रम में रहें लगती है, पर दोनों वहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाते और रातों-रात उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए मज़बूर होना पड़ता है। उन्हें रास्ते में सदन मिल जाता है जो दोनों बहनों को अपने साथ रहने का आग्रह करता है। वह शांता को भी अपना लेता है, जिसे उसने समाज के आडम्बरों के कारण छोड़ दिया था। पर समय के साथ-साथ सदन और शांता के स्वभाव में बदलाव आने लगा था। “सदन इस प्रकार सुमन से बचता था, जैसे हम कुष्ठ-रोगी से बचते हैं, उस पर दया करते हुए भी उसके समीप जाने की हिम्मत नहीं रखते। शांता उस पर अविश्वास करती थी, उसके रूप लावण्य से डरती थी। कुशल यही थी कि सदन स्वयं सुमन से आँखें चुराता था, नहीं तो शांता इससे जल ही जाती। अतएव दोनों चाहते थे कि आस्तीन का साँप आँखों से दूर हो जाय, लेकिन संकोचवश वह आपस में इस विषय को छेड़ने से डरते थे।”15
सच्चाई कितने दिनों तक ही छिपी रह सकती है, सुमन को भी अब समझ आने लगी थी कि उसके बहन-बहनोई अब उससे छुटकारा पाना चाहते है। सुमन को यह सब देखकर बहुत दुःख होता था। सुमन के शब्दों में-“सब कुछ देखकर भी आँखों पर विश्वास नहीं आता। संसार मुझे चाहे कितना ही नीच समझे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वह मेरे मन का हाल नहीं जानता, लेकिन तुम सब कुछ देखते हुए भी मुझे नीच समझती हो, इसका आश्चर्य है।”16 यहाँ तक की उसकी बहन को अब सुमन से ज्यादा लोगों द्वारा अपनी बदनामी की परवाह होने लगी थी। सुमन खुद अपनी बहन के घर भारस्वरूप नहीं रहना चाहती थी, उसके घर में रहने का कारण केवल बहन के प्रति मंगल भाव था। शांता गर्भवती थी, ऐसी अवस्था में वह उसे कैसे छोड़े पर शांता के ससुर द्वारा अपने लिए अस्पृश्यता की बात सुनती है तो वह उस घर को हमेशा के लिए छोकर चली जाती है। “मुंशी जी ने सुमन के चरित्र से यह दिखा दिया है कि कोई मनुष्य स्वभाव से पतित नहीं हैं। समाज की असह्रदयता मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है और उसकी सह्रदयता उत्थान की ओर।”17
पश्चाताप होने पर वह आत्महत्या करने का भी प्रयत्न करती है पर गंगा तट पर गजाधर प्रसाद मिलता है, जो सुमन से अपने किये अपराध के लिए क्षमा माँगता है। उसे सामने पाकर सुमन के पुराने ज़ख्म फिर से हरा हो जाता है, उसके मन में आता है कि उसे फटकारूँ क्योंकि उसी की वजह से उसके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी और उसी की वजह से उसके जीवन का नाश हो गया। अपने पति गजाधर को साधुवेश में देखकर और उसके इस प्रकार क्षमा माँगता देख, वह उससे कहती है कि यह सब उसके ही कर्मों का फल है। गजाधर के शब्दों में-नहीं सुमन, ऐसा मत कहो, सब मेरी मुर्खता और अज्ञानता का फल है। मैंने सोचा था कि उसका प्रायश्चित कर सकूँगा, पर अपने अत्यचार का भीषण परिणाम देखकर मुझे विदित हो रहा है कि उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता।”18 वह सुमन को जीवन के महत्त्व के बारे में बताता है और उसे समझाता है कि जो ग़लती उसकी पिता ने की थी, वहीं ग़लती वह न करें। गजाधर प्रसाद के यह वाक्य-“अब तक तुम अपने लिए जीती थीं अब दूसरों के लिए जियों।”19 सुमन के जीवन को इस वाक्य से नई दिशा मिल जाती है, वह सेवासदन में अवैध बच्चों को शिक्षा देने का कार्यभार सँभालकर अपना पूरा जीवन सेवाभावना में समर्पित कर देती है। सुमन उपन्यास के अंत तक आते-आते हर भारतीय नारी के लिए यह संदेश छोड़ती है कि जिंदगी काँटों से भरी जरूर है, पर संघर्ष और प्रयास द्वारा नई और खुशहाल जिंदगी की पहल की जा सकती है।
अंतत: कहा जा सकता है कि प्रेमचंद एक सच्चे समाज सुधारक और संवेदनशील उपन्यासकार थे। नारी के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। समाज में उपेक्षित, अपमानित और पतिता स्त्रियों के प्रति उनका ह्रदय सदा सहानुभूति से परिपूर्ण रहा है। प्रेमचंद ने जहाँ एक ओर नारी की सामाजिक पराधीनता उसके फलसवरूप उत्पन्न समस्याओं को अपने इस उपन्यास में अभिव्यक्ति प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर यह भी दिखलाया है कि किस प्रकार उनके नारी-पात्र उपन्यास के अंत तक आते-आते सामाजिक अन्याय से मुक्ति पाने का मार्ग स्वयं ही खोज देते हैं। कठिन-से कठिन परिस्थितयों में भी वे उठने का साहस रखते हैं।
संदर्भ सूची:-
- गोयनका, डॉ० कमलकिशोर, प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान, इलाहबाद, सरस्वती प्रेस, पृष्ठ संख्या-5
- द्विवेदी, हजारी प्रसाद, हिंदी साहित्य : उद्भव और विकास, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 2003, पृष्ठ संख्या-229
- प्रेमचंद, सेवासदन, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ संख्या-6
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-7
- यथावत्, पृष्ठ संख्या- 35
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-115
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-192
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-66
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-65
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-66
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-72
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-80
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-182
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-25
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-227
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-229
- स्तोगी, डॉ० शैल, हिन्दी उपन्यासों में नारी, साहिबाबाद, वि० भू० प्रकाशन, 1977, पृष्ठ संख्या-77
- प्रेमचंद, सेवासदन, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ संख्या-183
- यथावत्, पृष्ठ संख्या-185