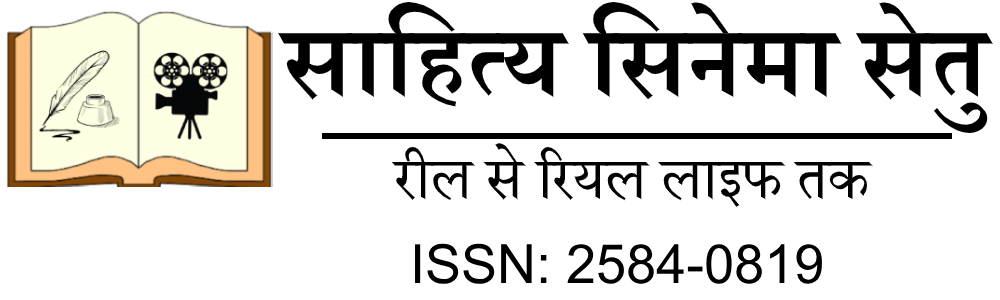अपने जातीय रूप की खोज करना, अपनी जातीय संस्कृति की मूल्यवान विरासत को पहचान और उस पर गर्व करना तथा अपनी जातीय संस्कृति के विकास के लिए अपने राष्ट्र को संगठित करने का संघर्ष चलाना। यह सब मानव समाज में प्राचीन काल से रहा है। आदिवासी संस्कृति की पहचान और उसे प्रतिष्ठित करने का जो संघर्ष है वह निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज सारी दुनिया में अस्तित्व के संघर्ष में हारी हुई जातियां अपनी अस्मिता को खोज रही है क्योंकि अपनी पहचान की खोज करने के लिए अपने अतीत को सर्वप्रथम खोजना जरूरी है आदिवासी की पहचान और संस्कृति से पहले आदिवासी कौन है? इस पर विचार करना आवश्यक पड़ता है।
आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि+वासी से मिलकर बना है आदि का अर्थ प्राचीन (मूल) और इसका अर्थ मूल निवासी होता है। ‘‘भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को अत्विका और वनवासी भी कहा गया है। संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में संथाल, गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बोड़ो, मील, खासी, सहरिया, गरसिया, मीणा, उरांव, बिरहोर आदि है।’’ (सं. मीणा, गंगा सहाय, 2014, आदिवासी साहित्य विमर्श दिल्ली पृ.108) आमतौर पर आदिवासियों को भारत में जनजातीय लोगों के रूप में जाना जाता है।‘‘आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक हैं जबकि भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक हैं जैसे मिजोरम। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में ‘‘अनुसूचित जनजातीयों’’ के रूप में मान्यता दी है।’’ (तलवार, वीर भारत 2008, झारखण्ड के आदिवासियों के बीच: एक एक्टीविस्ट के नोट्स, दिल्ली. पृ. 78)
‘‘आदिवासियों का अपना धर्म है। ये प्रकृति पूजक हैं और जंगल, पहाड़, नदियों एवं सूर्य की आराधना करते हैं।’’ (गुप्ता, रमणिका, 2004 आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी, दिल्ली, पृ. 121)| आधुनिक काल में जबरन बाह्य संपर्क में आने के फलस्वरूप इन्होंने हिंदू, ईसाई एवं इस्लाम धर्म को भी अपनाया है। अंग्रेजी राज के दौरान बड़ी संख्या में ये ईसाई बने तो आजादी के बाद इनके हिंदूकरण का प्रयास तेजी से हुआ है परन्तु आज ये स्वयं की धार्मिक पहचान के लिए संगठित हो रहे हैं और भारत सरकार से जनगणना में अपने लिए अलग से धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं।
आदिवासी समुदाय के संबंध में एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। द्वारिकादास गोयल निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हुए लिखते हैं-
‘‘वन्य जातियों से हमारा तात्पर्य ऐसे सामाजिक समूहों से है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए समान संस्कृति का अनुशील करते हैं। अर्थात् जिनकी भाषा, धर्म, रीति-रिवाज़ आदि विशिष्टता लिए हुए परस्पर सामान्य हो।’’ (गोयल, द्वारिकादास, भारतीय सामाजिक संस्थाएं, पृ.88)
आदिवासी संस्कृति पृथक संस्कृति रही है और इसको मानते हुए समाज वैज्ञानिक आदिवासी संस्कृति संरक्षण पर विशेष बल देते हैं पर यह निर्विवाद सत्य है कि बाह्य संसार में प्रवेश करने से शैनः शनैः इनकी संस्कृति का व्यापारीकरण होने लगेगा और वे समाज की व्यापक संस्कृति में मिल जायेंगे।
आदिवासी संस्कृति में ‘आदिवासी-धर्म’ की संकल्पना है उनका धर्म यानी प्रकृतिवाद। ये आदिवासी हिंदूधर्मिता के साथ हजारों सालों से रहते आए हैं लेकिन हिंदू धर्मियों ने उन्हें अपने में समा लेने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इतना ही नहीं उन्हें हिंदू-धर्म तथा जाति-व्यवस्था की चैखट में आदिवासियों को बैठाना भी नहीं आया। उन्हें पराया समझकर दूर रखा गया। ‘‘आदिवासी संस्कृति में गीत, लोकोक्तियां, कहावतों तथा कहानियों जिनमें लोककथाएं, अनुश्रुतियां तथा मिथक शामिल हैं। यह आदिवासियों के हर क्षेत्र में मिलते हैं।’’ (गुप्ता, रमणिका. 2004, आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी, दिल्ली, पृ. 103)
भारतीय संस्कृति और सभ्यता में आदिवासी परंपराएँ और प्रथाएं छाईं हुईं हैं फिर भी, इस तथ्य की जानकारी आम लोगों में नहीं है। ‘‘भारतीय दर्शन शास्त्र, भाषा एवं रीतिरिवाज में आदिवासियों के योगदान के फैलाव और महत्व को अक्सर इतिहासकार और समाजशास्त्रियों के द्वारा कम करके आंका और भुला दिया जाता रहा है।’’ (तलवार, वीर भारत 2008, झारखण्ड के आदिवासियों के बीच: एक एक्टीविस्ट के नोट्स, दिल्ली. पृ. 178)
सभ्यता व भौतिक विकास के अनुरूप संस्कृति अपना स्वरूप ग्रहण करती चलती है। इस रूप में संस्कृति मानव निर्मित होती है लेकिन मनुष्य का जीवन अंततः ‘प्रकृति का निर्भर होता है इसलिए प्रकृति तत्वों से संस्कृति का जुड़ाव अनिवार्य होना चाहिए। प्रकृति से लगाव और मानव सृजित होने की स्थिति के कारण संस्कृति का स्थान प्रकृति एवं कृत्रिमता के मध्य वहीं होता है। जिन मानव-समुदायों की संस्कृति का स्थान प्रकृति एवं कृत्रिमता के मध्य कहीं होता है। ‘‘मानव-समुदायों की संस्कृति प्रकृति से निकट का संबंध बनाकर विकसित होती है वे अधिक सौंदर्यबोधी, आनन्ददायक व कल्याणकारी होती है और जो संस्कृति प्रकृति से दूर हटती जाती है वे शास्त्रीय, व्याकरणीय औपचारिक, प्रतिमान आधारित, समाजवटी तथा नीरस बनती चली जाती है।’’ ( यादव, अभिषेक कुमार, आदिवासी जीवन- संघर्ष और परिवर्तन की चुनौतियाँ (आलेख),)
लोक व भद्र समाज की संस्कृतियों का मूलतः आधारित रहती आयी है। इस पृष्ठभूमि में आदिवासी संस्कृति को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों के परस्पर संपर्क से पैदा होने वाला प्रभाव आदान-प्रदान की स्थिति लाता है। इस प्रक्रिया में एक-दूजे द्वारा सीखने का नज़रिया संस्कृति को उन्नत करता है।
‘‘आदिवासी पारम्परिक मेलों के अवसर पर इकट्ठा होते हैं, उनमें अविवाहित युवक-युवतियों की संख्या काफी होती है मेले के उत्सव-उमंग, नाच-गान व मौज-मस्ती में वे उल्लास के साथ भाग लेते हैं। इस दौरान जान-पहचान व दोस्ती होती है। विपरीत लिंगाकर्षण से उत्पन्न स्वाभाविक प्रीति भी पनपती है। जो युगल शादी करने का मानव बना लेते हैं वे मेला स्थल से भागकर ऊँची पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से अपने ‘एक हो जाने’ का एलान करते हैं। संबंधित युवक-युवतियों के परिवार व संबंधियों में बुजुर्ग लोगों को यह पता चलता है तो वे गोत आदि व पृष्ठभूमि की कोई वैमनस्यता की बाधा न होने पर शादी की स्वीकृति दे देते हैं और वहीं सगाई की रस्म निभा दी जाती है। किसी कारणवश शादी न हो पाए तो दोनों भागकर अपना घर बसा लेते हैं। दोनों की स्थितियों में मेला स्थल से भाग जाने की वजह से इस परम्परा को ‘भगोरिया’ नाम दिया गया है।’’ (मीणा, हरिराम, आदिवासी संस्कृति- वर्तमान चुनौतियाँ का उपलब्ध मोर्चा.)
‘‘छत्तीसगढ़ के मुड़िया और झारखण्ड के मुण्डा व अन्य आदिवासियों में ‘घोटुल’ की प्रथा को बाकायदा परम्परागत मान्यता दी हुई है। ‘घोटुल’ अर्थात् सामूहिक वास-स्थल। प्रथा का लक्ष्य सामूहिक जीवन शैली के संस्कार विकसित करना रहा है। इस बहुआयामी गतिविधि का एक पक्ष यह भी है कि स्थानीय आदिवासी युवक-युवतियां अपनी मनपसंद और सहमति के आधर पर ‘घोटुल’ में यौन-संबंध बनाते हैं और इसके बाद मनपसंद जोड़े बनाकर शादी के लिए सहमति देते हैं जिसे अन्यथा कोई कारण सामने न आये तो समाज स्वीकार करता है। मनपसन्दगी से प्रेम और विवाह की ‘भगोरिया’ व ‘घोटुल’ जैसी परंपराएं उदात्त सांस्कृतिक जीवन के उदाहरण हैं जिन्हें तथाकिथत सभ्य समाज उल्टे नजरियये से देखता है। उस तथाकथित सभ्य समाज के भीतर कितनी यौन विकृतियाँ एवं अपराध पनपते हैं, यह नहीं देखा जाता।’’ ((मीणा, हरिराम, आदिवासी संस्कृति- वर्तमान चुनौतियाँ का उपलब्ध मोर्चा.)
आदिवासी लोक गीत परंपरा में विषय-वस्तु; बवदजमदजद्ध के स्तर पर वनोपज, कृषि-कर्म, श्रम, पालतू पशु-पक्षी, पर्व-उत्सव, शादी-ब्याह, जन्म-मृत्यु, पनघट, घरेलू औजार-पाती, पुरखे, मिथक, गणचिह्न, प्रकृति, ऋतुएं, मानवेतर अन्य प्राणी-जगत, प्रेम-प्रसंग, आत्म सम्मान के लिए विरोध-संघर्ष-बलिदान आदि तो रहते आये ही हैं, जमाने के बदलाव के साथ नयी बातें भी जुड़ती गयीं। आजादी के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू हुई। वोट देना नयी बात आयी जो पहले नहीं थी। उस पर भी गीतों का सृजन हुआ।
‘‘वोट देवा चालेंगा जोड़ा सू जूती खोलेंगा…।’’
(मीणा, हरिराम, आदिवासी संस्कृति- वर्तमान चुनौतियाँ का उपलब्ध मोर्चा.)
परम्परागत आदिवासी संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न उठाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रगति व विकास की धारा में मौलिक संस्कृति में परिवर्तन होना अनिवार्य है। लोग यह भी कहते हैं कि मौलिकता को बचाने के चक्कर में विकास अवरूद्ध होता है। ‘‘आदिवासी जीवन दर्शन में निरन्तरता एवं गत्यात्मकता; कलदंउपेउद्ध रही है। यही वजह है कि इस संस्कृति के शास्त्रीय प्रतिमान नहीं बनाये जा सकते हैं।’’ (श्रीवास्तव, चन्दन, ग्लोबल गाँव और गायब होता ‘देश’. आलेख) परम्परा की धारा में कोन, क्या जोड़ता जा रहा है, यह अज्ञात रहता है। सृजनकर्ता पहचान के पीछे नहीं भागता। रचना सामूहिकता में रम जाती है। आदिवासी संस्कृति इतनी खुली रही है कि विकास के सुखदायक पहलुओं को आत्मसात् करती हुई समृद्ध होती जायेगी। इसलिए विकास के साथ इसका विरोध हो ही नहीं सकता।
आदिवासी भौतिक दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़े और आदिम शैली का जीवन जीने वाले अण्डमान के आदिवासियों का दृष्टांत हम देख सकते हैं। ‘‘जारवा और सेंटेनली जैसी दो प्रजातियां हैं वहाँ अलग-थलग जंगलों में रहते हैं इन प्रजातियों के लोग। गैर आदिवासियों को वे शत्रु मानते हैं चूँकि उन्होंने बहुत सताया इतिहास में। सन् 1859 की अबेर्दीन की लड़ाई ताजा ऐतिहासिक वास्तविकता है। वे आदिवासी अभी भी पका हुआ खाना नहीं खाते, कपड़े नहीं पहनते, कृषि या बागवानी या कोई और कुटीर उद्योग – उत्पादन नहीं करते, झोंपड़ी नहीं बनाते, संपत्ति की अवधारणा से कोसों दूर है।’’ (मीणा, हरिराम, आदिवासी संस्कृति- वर्तमान चुनौतियाँ का उपलब्ध मोर्चा.) शिकार करके खाते हैं।
मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लम्बे दौर में मानवीय संबंधों में सामुदायिक मूल्य आधारित सामाजिक व्यवस्था वाला समाज अस्तित्व में आया, जो आदिम काल से आदिवासी समाज को विकसित, समृद्ध करता आया है और बहुत हद तक आज भी कायम है।
प्रकृति प्रेम और मानव स्वभाव सभी आदिवासी समूहों में एक समान कारक मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी अंचल के आदिवासी हों, उनका एक इतिहास भी सामने आना चाहिए।
आदिवासी संस्कृति की पहचान प्राचीन काल से रही है। इनको ‘दूसरी दुनिया’ की संज्ञा भी दी जाती रही है। इनके यहाँ स्त्री-पुरुष को बराबर का दर्जा और निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त रहा है। इनकी प्रथाएँ बहुत प्राचीन और अलग रही हैं। शिकार में निपुण होते हैं। इनके यहाँ खान-पान, रहन-सहन से लेकर जीवन-जीने के तरीके बहुत अलग और आदिवासी संस्कृति में जीवन को महत्त्व अधिक है और जीवन से जुड़े रहने के साथ-साथ अपने नियम बहुत आसानी से स्वीकार करते हुए उस पर अमल करते चलते हैं। इस परंपरा को निरंतर जिंदा रखते हैं। आदिवासी में एक अपनेपन की संस्कृति देखी जाती है।
आदिवासी संस्कृति में प्रकृति-प्रेम, आदिम सौंदर्य-बोध, नृत्य-गीत, कलात्मकता, उत्सव-पर्व-मेले, धूमिल आस्थाएं, सामाजिक संस्कार, मिथक, गणचिन्ह, कथा-कहावत, पहेली-मुहावरे, खेल-कूद एवं मनोरंजन की अन्य क्रियाएँ भद्र संस्कृति की तरह फुरसत के क्षणों को भरने वाली चीजें न होकर संपूर्ण जीवन, यथा मनोविज्ञान, आचरण, सिद्धांत एवं परंपरा, सृजनात्मकता, मूल्य-व्यवस्था से गहरा संबंध रखने वाली क्रियाशील प्रयोजनधर्मी सहज एवं आत्मीय अभिव्यक्तियाँ हैं। सार्वभौमिक मूल्य बचे रहने चाहिए तभी सब कुछ सुरक्षित रह सकेगा।
संदर्भ ग्रंथ
1. डॉ. अमरनाथ. (2015). हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
2. सं. मीणा, गंगा सहाय. (2014). आदिवासी साहित्य विमर्श. दिल्ली: अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लिमिटेड.
3. जोशी, रामशरण (अनुवादक: अरूण प्रकाशन). (1967). आदिवासी समाज और शिक्षा. दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.
4. सं. रणेन्द्र (2008). झारखण्ड एनसाइक्लोपीडिया मंदार की धमक और गुलईचि की खुशबू. दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
5. गुप्ता रमणिका. (2004). आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी. दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
6. गुप्ता रमणिका (2008). आदिवासी साहित्य यात्रा. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
7. तलवार, वीर भारत. (2008). झारखण्ड के आदिवासियों के बीच: एक एक्टीविस्ट के नोट्स. दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ.
8. डॉ. मुण्डा, रामदयाल. (2012). आदिवासी अस्तित्व और झारखण्डी अस्मिता के सवाल. प्रकाशन संस्थान.
पत्र पत्रिकाएँ
1. मीणा, गंगा सहाय. आदिवासी अस्मिता और साहित्य.
2. वरवाल, सुरजीत सिंह. आदिवासी विमर्श: एक शोचनीय बिन्दु. साहित्य. कुंज पत्रिका.
3. श्रीवास्तव, चंदन. ग्लोबल गांव और गायब होता ‘देश’.
4. यादव, अभिषेक कुमार. आदिवासी जीवन-संघर्ष और परिवर्तन की चुनौतियाँ.
5. विद्याभुसन. भारत में आदिवासी प्रश्न.
6. मीणा, हरिराम. आदिवासी संस्कृति – वर्तमान चुनौतियों का उपलब्ध मोर्चा.