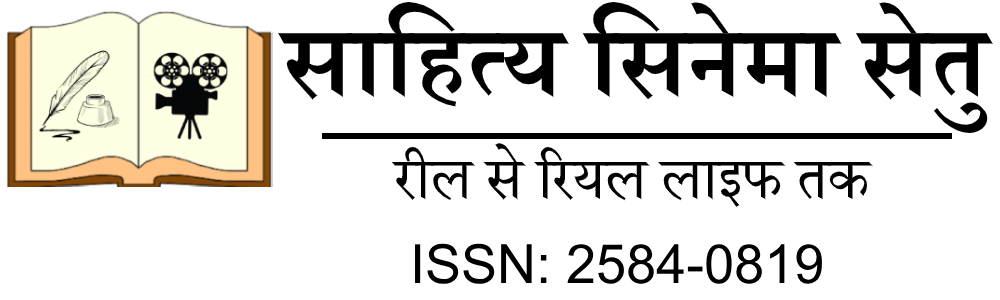“अब जब तुम देखोगे चेहरा अपना
पहचान जैसा सब कुछ, कुछ नहीं होगा कहीं भी,
बदली-बदली है विश्व संरचना इन दिनों”
बदलती हुई इस विश्व संरचना के दौर में जहाँ दुनियाँ तेजी से बदल रही है। वहीं उसके भीतर की संवेदना पर भी बदलाव का असर साफ तौर पर नज़र आने लगा है। जिसका परिणाम यह हुआ कि बदलाव को रेखांकित कर उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत करने वाले दो महत्वपूर्ण अस्त्र सिनेमा और साहित्य ने भी अपनी पुरानी केंचुल उतार कर नया परिधान धारण किया है। यह परिधान भले ही बाहरी तौर पर बहुत आकर्षण दिखाई देता है। पर उसके भीतर कि संवेदना इस नए लबादे के बोझ तले झूलती नज़र आती है। यूँ तो कहने को साहित्य कि उम्र सिनेमा से काफी बड़ी है पर जब हम आधुनिक हिंदी साहित्य कि बात करते हैं, जो 1900 ई. के आस-पास अपना प्रभाव छोडना शुरू करता है। तो हमारे लिए साहित्य और सिनेमा के सफर पर एक साथ यात्रा करना आसान हो जाता है। एक ऐसी दिलचस्प यात्रा जहाँ हम दोनों को समांतर रखकर उनके प्रेम संबंधों, समंजस्य विषय, प्रयोगों, भावनाओं, संवेदनाओं और समय के साथ इनमें तेजी से आते हुए उन परिवर्तनों को चिहनित भी कर सकते हैं, जिनके कारण आज के हाइटेक युग में दोनों अपने भीतर कि संवेदना को बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई पड़ते हैं।
1930 के दशक में जब फिल्में अपने मूक युग से बाहर आकार कुछ कहने को तत्पर हुई तब यह उसकी उम्र का पहला पड़ाव था। जहाँ कथा, संवाद, आभिनय सब दृष्टि से कुछ अटपटापन दिखाई देता है। जबकि साहित्य ने इस दौर में अपने पैर गहराई तक जमा लिए थे। समाज कि स्थिति उसके पन्नों में दर्द बनकर उभर रही थी। भारतेन्दु भारत की दुर्दशा को देख आँसू बहा रहे थे। गुप्त की यशोधरा, हरीऔध के प्रियप्रवास की राधा, सुभद्रा कुमारी चौहान की ‘झाँसी की रानी’ समाज के भीतर समाज सुधार, करुणा और देशभक्ति का संचार कर रही थी। वहीं सिनेमा ने भी शैशवास्था के पड़ाव को पार कर परिपक्वता की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। उसके पत्येक नए कदम को साहित्य ने जमीन दी और नयी दिशा की ओर अग्रसर किया। 1936 में ‘अछूत कन्या’, हंटरवाली, रोटी, किस्मत, जय भारत, बेरोजगार, भारत का लाल, परिवर्तन, संगदिल समाज, दलित कुसुम आदि फिल्मों में सामाजिक विसंगतियों, दलित उद्धार, आजादी की कोशिश जैसी समसामयिक समस्याओं को फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत कर सिनेमा जगत में हलचल मचा दी थी। वहीं साहित्य छायावादी रूमानी कविता, गोदान जैसे उपन्यासों के माध्यम से साहित्य जगत में सफलता के नए मानदंड स्थापित कर रहा था। यह साहित्य और सिनेमा के प्रेम-संबंधों का वह पड़ाव था, जहाँ दोनों के भीतर संवेदना लहर मार रही थी। यह युग साक्षी था उन कलाकारों का जो उन मूल्यों, आदर्शों, संवेदनाओं को दर्शक समाज तक पहुँचना चाह रहे थे। जिनके लिए सिनेमा की छवि मूल्यों और आदर्शों से सरोकार थी। यह 1950 और 60 के दशक का वह समय है जब आजादी आंदोलन से जन्मा आदर्शवाद साहित्य और सिनेमा पर छाया हुआ था। जहाँ ‘जागृति’ जैसी फिल्में, मनोज कुमार जैसा हीरो, ‘तू हिन्दू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा’ जैसे गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर बोल रहे थे। हालांकि हिंदी सिनेमा एक उद्योग था। जिस पर बाज़ार पूरी तरह से हावी था, पर प्रारंभिक दौर पर वह अपने बाजारीकरण को नकारता रहा पर किस्मत, दाग, बैज़ूबावरा, मदर इंडिया, आवारा जैसी फिल्मों की परंपरा के चरम ने प्रेम, नैतिकता जैसे भावों पर प्रश्न चिह्न लगा दिया। लगभग 60 के दशक सिने उद्योग हेलेन के कैब्रेडांस, अंडरवर्ल्ड के ग्लैमराइजकरण, स्विमिंग कास्ट्यूम, चमकती रेसिंग कार आदि के इर्द-गिर्द चक्कर लगाने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ की हिंदी सिने उद्योग मुनाफे का काला चश्मा चढ़ाकर डिस्को की तेज धुनों पर थिरकने लगा। जहाँ अब उसे ‘हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के (जागृति), सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है’ (शहीद) जैसी फिल्मों के गीत दिखने सुनने बंद हो गए। यह संवेदनहीनता का वह दौर था जब आदर्शवादी राज कपूर ने ‘सत्यम् शिवम् सुंदरम्’ व ‘राम तेरी गंगा मैली हो गई’ तथा मनोज कुमार ने अपनी ‘भारत’ छवि को उतरकर ग्लैमर, सेक्स व अंग प्रदर्शन को लगभग अपनी सभी फिल्मों में भुनाया। वहीं साहित्य अब भी संवेदनाओं को समेटे ‘वह तोड़ती पत्थर’ कई दिनों तक चूल्हे और चक्की के उदास रहने की कथा कहता हुआ समाज में चूर होती संवेदनाओं का दर्द समेटे ‘निकल गली से फिर हत्यारा, हाथ तौलकर चाकू मारा, उसे पता था उसकी हत्या होगी” के रूप में अपनी व्यथा समाज तक पहुँचा रहा था। महत्वपूर्ण यह था कि साहित्य जहाँ विघटित मूल्य व्यवस्था में भी अपने भीतर कि संवेदनाओं को पकड़े हुए लगातार कविता, कहानी, उपन्यास आदि के माध्यम से अपने विकास पथ पर अग्रसर होकर नाय कीर्तिमान स्थापित करता चला जा रहा था। वहीं सिनेमा ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। उसके भीतर के संस्कारों ने उसे अनेक साहित्य कृतियों – तमस, सूरज का सातवाँ घोड़ा, आँधी, शतरंज के खिलाड़ी, रूदाली, तीसरी कसम, काली आँधी, रजनीगंधा, देवदास आदि फिल्में बनाने के लिए विवश कर दिया। इन फिल्मों ने भले ही व्यावसायिक दृष्टि से सिनेमा को फायदा न पहुँचाया हो पर उसके भीतर कि संवेदनाओं को मरने से जरूर बचा लिया।
70-80 के दशक में सिनेमा एक और कदम आगे बढ़ता है। जहाँ सामाजिक, रोमानी, मानवीय संवेदनाओं का प्रतिनिधि सिनेमा कमर्शियल स्टार सिस्टम व स्टार कैटागरी ब्रेकअप (नंबर वन स्टेटस) का शिकार हो कर हिंसा, मारधाड़, अंग प्रदर्शन, बोल्डनेस की पंक्ति में खड़ा हो जाता है। जहाँ हीरो एंग्रीमैन में बदलता है तो हीरोइन बाथटब से निकलती जल सुंदरी में। जहाँ दर्शक सिनेमा में अपना दुश्मन से बदला लेकर कुछ पल के लिए कुछ न कर पाने की लाचारी भूल जाता है। 80 के दशक तक भी इस तरह की फिल्मों का दौर छाया रहा जहाँ एक ओर धूम धड़का और उसी के समानान्तर ‘उमराव जान’ जैसी सुबोध फिल्में भी दर्शक को आकर्षित करती रहीं।
पर 90 के दशक और उसके बाद जब हम सिनेमा के स्वरूप पर नज़र डालते हैं तो वह बिलकुल नयी तस्वीर पेश करता है। उसका स्वरूप इतना बहुआयामी दिखाई पड़ता है कि हमारे व्यक्तित्व का हर पक्ष उसमें प्रतिबिंबित हो उठता है। एक तरफ जहाँ वह पारिवारिक मूल्यों को ‘हम आपके हैं कौन’, ‘हम साथ-साथ हैं’, ‘कभी खुशी कभी गम’, बागवान, विवाह जैसी फिल्मों के माध्यम से बचाए रखने का प्रयास करता है तो वहीं दूसरी तरफ नशे में धुत्त, देह कि नुमाइश प्रेम के नाम पर ‘ठग लेने’ की संस्कृति, सिगरेट के धुएँ के छल्ले उड़ता स्टेटस सिंबल, आधी रात की माँग करता हीरो, जिसका मूल-मंत्र ‘घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएँगे, ऐश कारेंगे और क्या’ है। वह समाज को किस दिशा की ओर ले जा रहा है। यह सोचने की वस्तु है। हिंदी सिनेमा पर बाज़ारीकरण की काली का यह प्रभाव तो कुछ नहीं है। पर जब यह मनोरंजन के नाम पर अपराध को जन्म देता है। तो यह और भी हिंसक दिखाई देने लगता है। जब बाज़ीगर का हीरो शाहरुख़ ख़ान अपनी प्रेमिका को मल्टीस्टोरी बिल्डिंग से धक्का दे देता है, स्पेशल 26 की टीम लोगों को क्राइम ब्रांच के नाम पर ठगने का नया फॉर्मूला देती है। ‘राजनीति’ की राजनीति संबंधों पर कुर्सी का रंग चढ़ाती है तो ‘तीस मार खाँ’ देश भक्ति के नाम पर देश की ट्रेन लुटवा देता है। अपराध की दुनिया को न जाने कितने ऐसे फॉरमूले इन फिल्मों से मिलते हैं। जिनका प्रयोग आज समाज में धड़ल्ले से होता है। और इनके आगे संवेदनाएँ धराशायी हो जाती हैं। सिनेमा में संवेदनाओं का यह संकट उस सौ करोड़ के पैमाने की देन है, जिसने सिनेमा को संवेदना के दायरे से खींच कर सेक्स और हिंसा के उस मापदंड पर खड़ा कर दिया है, जिस पर खरा उतरना हर फिल्म की कसौटी बन गया है। और आइटम सॉन्ग उसकी जरूरत। भले ही फिर इसके लिए शीला की जवानी को उभारा जाए या मुन्नी बदनाम हो जाए, बीड़ी को माचिस के बजाए जिगर से जलाना जरूरत बन जाए या आइटम गर्ल सोने की हो और पूरी दुनिया पीतल में कन्वर्ट हो जाए। पर सेक्स का फेविकोल हर फिल्म में लगा होना जरूरी हो जाता है तभी तो फिल्म से दर्शक चिपकेगी। यह फिल्मी सेक्स जहाँ हमारी भीतरी मनोवृत्ति को तृप्त करता है। वहीं बाहरी इमेज का प्रश्न भी सिनेमा से अलग नहीं है। इसीलिए हिंसा का पेस्ट हर किसी को फ्रेशनेस देता है। लगातार चलने वाली गोलियाँ, बिल्डिंग से कूदता हीरो, हाथ से गाड़ी को उठा देने वाली मर्दांगी, एक का दस पर भरी पड़ने वाला ढाई किलो का हाथ, जादुई स्टंट, सुपरमैन से सुपर हीरो और हीरोइन में कन्वर्ट होने वाला सिनेमा लगातार जिस छवि में सामने आ रहा है वह समाज को हिंसा के दलदल में घसीटता नज़र आता है। इस दलदल को गहरा बनाने का काम सिनेमा में प्रयोग की जाने वाली हाइटेक तकनीक ने किया है। जो बटन दबाते ही खतरनाक कामों को इतनी आसानी से पल भर में अंजाम देती है कि दर्शक दांतों तले अंगुली दबा लेता है। रोबोट, कृष-2, धुम, रा-वन, सिंघम न जाने कितनी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इन तकनीकों के बलबूते सिनेमा को सौ करोड़ के जीतने करीब लाया है, संवेदना को उतना ही पीछे धकेल दिया है। संवेदना का यह हाल साहित्य में भी दिखने लगा है। जहाँ समाज कि समस्याओं को निस्वार्थ भाव से लिखने वाला रचनाकार आज पुरस्कारों, उपाधियों, सम्मानों के प्रति रचना से अधिक निष्ठा करना प्रतीत होता है। उसके भीतर का वह फककडपन और निरालापन खोता नज़र आता है। जिसने साहित्य के क्षेत्र में रचनाशीलता का संकट उत्पन्न कर दिया है। संवेदनशीलता के संकट का यह प्रश्न अपने आप में बहुत गंभीर है। पर संतोष इस बात का है कि डिजिटल होती चीजों के इस युग में तकनीक भले ही इन संवेदनाओं पर हावी दिखाई देती है। पर महत्वपूर्ण यह है कि साहित्य और सिनेमा दोनों कि जड़ें संवेदना से पूर्ण रूप से रिक्त नहीं हुई है। साहित्य पुरस्कारों कि दौड़ में भी जहाँ अपनी रचनाओं में संवेदना संभाले हैं वहीं सिनेमा भी कला फिल्मों के रूप में अपनी जीवित संवेदना कि बानगी देता है। दस्तक से शुरू हुआ कला फिल्मों का दौर अंकुर, मंथन, मोहन जोशी हाजिर हों, अर्धसत्य, अर्थ, आधारशिला, पार, दामुल, अंकुश, डोर, मातृभूमि, धारावी, वाटर आदि के रूप में दर्शकों के समक्ष व्यावसायिक फिल्मों के झूठ को नंगा कर देता है। पर दुख इस बात का है कि चकाचौंध की इस दुनिया में लोगों की मानसिकता कला फिल्मों को लेकर ये बन गई है की ये दर्शकों को सभ्यता की अंधी गली में छोड़ देती है, जबकि व्यावसायिक फिल्में उन्हें आनंद प्रदान कर हॉल से बाहर निकलते हुए होठों पर प्रेम का वह तराना छोड़ देती है, जिसकी स्फूर्ति को वह आने वाले शुक्रवार तक अनुभव कर सकता है। आज आवश्यकता साहित्य और सिनेमा की संवेदना पर छाए उस संकट को दूर करने की है, जो सिर्फ हमारी मानसिकता के परिष्कार से दूर होगा। इसके लिए साहित्य को जहाँ अपनी रचनाशीलता को प्रलोभनों से मुक्त रखना होगा तो सिनेमा को व्यावसायिक फिल्मों में ही ऐसे प्रयोग करने होंगे जो दर्शकों को आनंद देने के साथ-साथ उसकी चेतना का परिष्कार भी करें। थ्री इडियट्स, तारें जमीं पर, चक दे इंडिया, क्वीन, हाइवे जैसी फिल्में इस दिशा में किया गया प्रयास है। वरना वह दिन दूर नहीं जब विश्व सिनेमा का बाज़ार और प्रलोभनों का दवाब हिंदी सिनेमा और साहित्य पर हावी होकर उसे पूर्णतः यांत्रिक बना देगा। जहाँ मानवीय संवेदनाएँ उसके तले दम तोड़ती नज़र आएंगी।