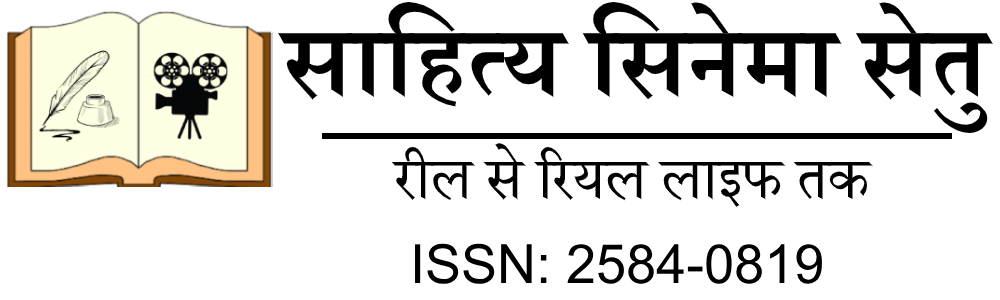यह शत प्रतिशत सत्य है कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की साहित्यिक दृष्टि को समझे बगैर हिन्दी साहित्य को समझ पाना आज भी आकाश कुसुम जैसा है। उनकी स्थापनाओं से टकराए बगैर न तो समीक्षक आगे बढ़ सकते हैं और न ही उन्हें हृदयंगम किए बिना साहित्यिक पाठक हिन्दी साहित्य के विकासक्रम तथा कवि-लेखकों के विषय में अपना मन्तव्य स्थापित कर सकते हैं। एक बहुज्ञ विद्वान के रूप में उनकी स्थापनाएँ भारतीय दृष्टि तथा पाश्चात्य पथ के मध्य स्थित गलियारे पर सरपट दौड़ती हैं एवं भारतीयता के पक्ष को पुष्ट करती नज़र आती हैं। एतदर्थ, भारतीयता के आग्रही होने के परिणामस्वरूप स्वाभाविक तौर पर भाषा की दृष्टि से भी आचार्य शुक्ल हिन्दी के प्रबल पक्षधर के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। नागरी प्रचारणी सभा ने जिस समय काशी से ‘हिन्दी’ मासिक पत्र निकालने की योजना बनायी, उस समय सम्भवतः इस पत्र के पीछे आचार्य शुक्ल की ही प्रेरणा काम कर रही थी क्योंकि उस समय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ही सभा के सभापति थे। इस पत्र को निकालने हेतु उन्होंने सभापति के रूप में ‘हिन्दी प्रेमियों से अनुरोध’ शीर्षक से एक पत्र लिखा था, जिससे उनकी हिन्दी के प्रति भावना देखी जा सकती है-
‘‘हमारी परम्परागत भाषा को हमारे व्यवहारों से अलग करने का प्रयत्न बहुत दिनों से चल रहा है, पर अपनी स्वाभाविक शक्ति से यह अपना स्थान प्राप्त करती चली आ रही है। इधर जब से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की चर्चा छिड़ी है, तब से इसके विरोधी प्रचण्ड वेग से इसकी गति रोकने के अनेक उपाय रचने में लग गए हैं। इस अवसर पर अपनी भाषा की रक्षा का भरपूर उद्योग हमने न किया तो सब दिन के लिए पछताना पड़ेगा। पर हममें से अधिकतर लोगों को यह भी पता नहीं है कि हिन्दी को उखाड़ फेंकने के लिए कितने चक्र किन-किन रूपों में कहाँ-कहाँ चल रहे हैं। यही देखकर ‘हिन्दी’ पत्रिका निकाली गयी है, यह इस बात पर बराबर दृष्टि रखेगी कि अनिष्ट की आशंका कहाँ-कहाँ से है और समय-समय पर अपनी सूचनाओं द्वारा हिन्दी प्रेमियों से स्थिति पर विचार करने और आवश्यक उद्योग करने की प्रेरणा करती रहेगी।
हमें पूरा विश्वास है कि समस्त देशभक्त और मातृभाषा प्रेमी सज्जन इस पत्रिका की सहायता हर प्रकार से-धन से, लेख से, आवश्यक बातों की सूचना से, अवसर के अनुकूल परामर्श से-करेंगे और यह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करेगी।’’1
यद्यपि यह योजना कार्यरूप न ले सकी, किन्तु इस पत्र से शुक्ल जी की हिन्दी के प्रति दृष्टि तथा हिन्दी के विकास के प्रति उनकी तीव्र स्पृहा को देखा जा सकता है। यदि यह पत्र प्रकाशित होता तो निश्चय ही हिन्दी के विकास में सरस्वती की भाँति इसका भी नामोल्लेख होता।
हममें से अधिकांश आचार्य शुक्ल के कवि रूप से प्रायः अपरिचित रहे हैं। उनकी कविताएँ परिमाण में भले अत्यल्प हों तथा उनकी चर्चा नगण्यप्राय होती हो परन्तु अपनी अनेक कविताओं में वे हिन्दी के प्रति अपने अनुराग को लक्षित करते हैं। ‘हमारी हिन्दी’ नामक कविता में तो उन्होंने खुलकर अपने मनोभाव प्रकट किए हैं, जिसका एक अंश उद्धृत है-
‘‘मन के धन वे भाव हमारे हैं खरे।
जोड़-जोड़ कर जिन्हें पूर्वजों ने भरे।।
उस भाषा जो है इस स्थान की।
उस हिन्दी में जो है हिन्दुस्तान की।।
उसमें जो कुछ रहेगा वही हमारे काम का।
उससे ही होगा हमें गौरव अपने नाम का।।’’2
हिन्दी के उन्नायक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को उनकी जयंती पर स्मरण करते हुए ‘भारतेन्दु-जयन्ती’ कविता में वे कहते हैं-
‘‘पल्ला पकड़ विदेशी भाषा का दौड़े कुछ वीर।
नए-नए विज्ञान कला की ओर छोड़कर धीर।।
पिछड़ गया साहित्य शिथिल तन लिया न उसको संग।
पिया ज्ञान रस आप, लगा वह नहीं जाति के अंग।।
इसी बीच ‘‘भारतेन्दु’’ कर बढ़े विशाल उदार।
हिन्दी को दे लगाया नए पंथ के द्वार।।
जहाँ ज्ञान-विज्ञान आदि के फैले रत्न अपार।
संचित करने लगी जिन्हें है हिन्दी विविध प्रकार।।3
भारतेन्दु जी पर ‘भारतेन्दु हरिश्चन्द्र’ नाम से लिखी एक अन्य कविता में भी वे भारतेन्दु जी की हिन्दी सेवा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहते हैं-
‘‘शिष्ट शराफत में थे लगे,
यह चन्द औ सूर की बानी बड़ी।
केवल तानों में जाती तनी,
मुँह में मँगतों के थी जाती सड़ी।
राज के काज को त्याग सभी,
फिर धर्म की धार पै आके अड़ी।
श्री हरिचन्द जो होते न तो,
रह जाती वहाँ की वहाँ ही पड़ी।।4
बाबू देवकीनन्दन खत्री के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए ‘श्रीयुत् बा. देवकीनन्दन खत्री का वियोग’ कविता में वे खत्री जी की हिन्दी सेवा को नमन करते हुए लिखते हैं-
‘‘है यह शोक समाज आज उसके लिए।
जिसने हिन्दी के अनेक पाठक किए।।
रचा तिलस्मी जाल फँसे जिसमें बहुतेरे।
टो-टो पढ़ने वाले औ उर्दू के चेरे।।
चन्द्रकान्ता हाथ न उनकी ओर बढ़ाती।
ढूँढे उनका पता कहीें हिन्दी फिर पाती?’’5
हिन्दी की काव्य भाषा की चार विशिष्टताओं पर शुक्ल जी मोहित रहे हैं। उनके मतानुसार इन गुणों से हिन्दी कविता की प्रभविष्णुता में अभिवृद्धि हुई है। पहली, कविता में कही गयी बात को चित्र रूप में सामने लाना, दूसरी कविता में विशेष रूप व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना, तीसरी, वर्णविन्यास या नाद सौन्दर्य और चौथी विशेषता मनुष्य नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या व्यापार की ओर संकेत किया जाना।6
आचार्य शुक्ल के लेखन के समय सम्पूर्ण भारत में हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रश्न खड़ा था और इसकी लिपि के विषय में भी पर्याप्त मंथन किया जा रहा था। उस समय गाँधी जी (उनसे पूर्व राजा शिवप्रसाद ‘सितारे हिन्द’) हिन्दुस्तानी के पक्ष में खड़े दिखते हैं तो शुक्ल जी दृढ़तापूर्वक हिन्दी के पक्ष में क्योंकि उनकी दूरदर्शी दृष्टि ने यह महसूस कर लिया था कि हिन्दुस्तानी जैसी कृत्रिम तौर पर विकसित की जा रही रेख़्ता मिश्रित भाषा का लक्ष्य उर्दू भाषियों के अहं को तुष्ट करना मात्र है और इससे गहन साहित्यिक चिंतन तथा सघन अनुभव की व्यापकता से युक्त साहित्य सृजन नहीं किया जा सकता।7 हालांकि यह दुखद है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी इस पर लीपापोती करते नज़र आते हैं। चतुर्वेदी जी लिखते हैं, ‘‘पर रामचन्द्र शुक्ल यदि हिन्दी के फारसीकरण का विरोध करते हैं तो संस्कृत के अनुचित दबाव का भी।’’8 इन पंक्तियों के लेखक ने आचार्य शुक्ल के समस्त लेखन में इस ‘संस्कृत के अनुचित दबाव’ को खोजने का प्रयास किया, परन्तु यह दबाव कहीं नहीं दिखा। अपने दावे के समर्थन में वे जिस सन्दर्भ को उद्धृत करते हैं, वह है-‘‘ हाँ, जिन विचारों के लिए हिन्दी वा संस्कृत शब्द न मिलें उनको प्रकट करने के लिए हम विजातीय शब्द लाकर अपनी भाषा की वृद्धि मान सकते हैं।’’9 इन शब्दों में शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि हिन्दी अथवा संस्कृत के शब्द उपलब्ध न होने पर ही अन्य किसी भाषा के शब्द लिए जाएँ न कि वे संस्कृत के अनुचित दबाव को न मानने की बात कह रहे हैं। कालान्तर में भारत सरकार द्वारा स्थापित ‘वैज्ञाानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग’ ने भी विभिन्न पारिभाषिक शब्दों के निर्माण हेतु मार्गदर्शक सूत्र के रूप में शुक्ल जी के इसी सिद्धांत को स्वीकार किया।
‘अपनी भाषा पर विचार’ लेख में वे राजा शिवप्रसाद की ‘मुसलमानी हिन्दी’ का विरोध करते हुए कहते हैं, ‘‘ राजा शिवप्रसाद मुसलमानी हिन्दी का स्वप्न ही देखते रहे कि भारतेन्दु ने स्वच्छ आर्य हिन्दी की शुभ्र छटा दिखाकर लोगों को चमत्कृत कर दिया। लोग चकपका उठे, यह बात उन्हें प्रत्यक्ष दीख पड़ी कि यदि हमारे प्राचीन धर्म, गौरव और विचारों की रक्षा होगी तो इसी भाषा के द्वारा। स्वार्थी लोग समय-समय पर चक्र चलाते ही रहे किन्तु भारतेन्दु की स्वच्छ चन्द्रिका में जो एक बेर अपने गौरव की झलक लोगों ने देख पायी वह उनके चित्त से न हटी। कहने की आवश्यकता नहीं कि भाषा ही जाति के धार्मिक और जातीय विचारों की रक्षिणी है; वही उसके पूर्व गौरव का स्मरण कराती हुई, हीन से हीन दशा में भी, उसमें आत्माभिमान का स्रोत बहाती है। किसी जाति को अशक्त करने का सबसे सहज उपाय उसकी भाषा को नष्ट करना है। हमारी नस-नस से स्वदेश और स्वजाति का कैसे लोप हो गया? क्या यह भी बतलाना पड़ेगा? भारतवर्ष की भुवनमोहिनी छटा से मुँह मोड़कर शीराज और इस्फहान की ओर लौ लगाए थे; गंगा जमुना के शीतल शान्तिदायक तट को छोड़कर इफ़रात और दजला के रेतीले मैदानों की ओर लालायित हो रहे थे; हाथ में अलिफ लैला की किताब पड़ी रहती थी, एक झपकी ले लेते थे तो अलीबाबा के अस्तबल में जा पहुँचते थे। हातिम की सख़ावत के सामने कर्ण का दान और युधिष्ठिर का सत्यवाद भूल गया था; शीरीं-फरहाद के इश्क ने नल-दमयन्ती के सात्विक और स्वाभाविक प्रेम की चर्चा बन्द कर दी थी।’’10
तत्कालीन निजाम की राजधानी हैदराबाद में ‘यंग मेंस इम्प्रूवमेंट सोसाइटी’ की एक सभा में डाॅक्टर निशिकांत चटर्जी ने उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी। उर्दू को राष्ट्र पर थोपने की उनकी मांग का ज़ोरदार विरोध करते हुए आचार्य शुक्ल ने ‘उर्दू राष्ट्रभाषा’ शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें उन्होंने चटर्जी महोदय के एक-एक तर्क को पूरी तरह से काटते हुए हिन्दी का पक्ष रखते हुए लिखा, ‘‘हिन्दी शब्दों के सिवाय जो शब्द उर्दू में हैं, वे अरबी, फारसी, तुर्की आदि के हैं। ये विदेशी शब्द अधिकतर सीख-सीखकर भाषा में भरे जाते हैं, इसमें तो कुछ सन्देह ही नहीं। उन संस्कृत शब्दों की ओर जिनका प्रचार न केवल सारे हिन्दुस्तान ही में वरन् सिंहल द्वीप, ब्रह्मदेश और श्याम आदि में है, उर्दू भूलकर भी नहीं ताकती। और कहाँ तक कहें संस्कृत के उन साधारण शब्दों के लिए भी जो गाँव-गाँव घर-घर सुनने में आते हैं, उर्दू में जगह नहीं। जैसे-सुख-दुःख, माया, प्रेम, प्रीति, कलह, शोक, शोभा, रीति, प्रण, जीवन, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैभव, मुख्य अतिथि, चिन्ता, अस्तित्व, पाप, पुण्य, धन आदि। हिन्दी उन फारसी वा अरबी शब्दों को अपनाने में जरा भी संकोच नहीं करती जो लोगों के व्यवहार में आ गए हैं। यह प्रवृत्ति उसकी अपनी है। सूरदास और तुलसीदास आदि अरबी-फारसी के शब्दों को जो देश में बस गए हैं, पूरा-पूरा ग्रहण करते हैं। बहुत से ऐसे ठेठ हिन्दी के साधारण शब्द जिनके बिना हमारा नित्य का व्यवहार नहीं चल सकता पर जिनके बिना अरबी फारसी का काम बड़े मजे से चला आता है, उन्हें हम क्या समझें! यही न उर्दू साहित्य से और हमारे सांसारिक जीवन से बहुत कम लगाव दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिक दार्शनिक और गम्भीर विषयों को समझाने के लिए हिन्दी संस्कृत से सहायता लेते हैं, जिसके समझने और जानने वाले इस देश में अरबी-फारसी की अपेक्षा दस गुने अधिक हैं। दूसरी बात यह है कि उर्दू हिन्दुस्तानी, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि किसी की शब्द परम्परा से नहीं मिलती अतः वह इन भाषाओं के बोलने वालों के बीच प्रचार कैसे पा सकती है? पर हिन्दी से उनका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। कहीं-कहीं तो केवल क्रिया आदि के रूपों बदलने से ही दो भाषाएँ एक हो जाती हैं।’’11
शुक्ल जी यदि एक ओर उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाए जाने तथा उर्दू के अप्रचलित शब्दों का विरोध करते हैं तो दूसरी ओर वे संस्कृत के पुराने उपमानों को हिन्दी में ज्यों का त्यों रखे जाने का भी विरोध करते हैं। वे लिखते हैं,‘‘कुछ दिन पहिले हमारी हिन्दी की स्थिति ऐसी हो गयी थी कि उसका विचार क्षेत्र अग्रसर होना कठिन देख पड़ता था। बने-बनाए समास, जिनका व्यवहार हजारों वर्ष पहिले हो चुका था, लाकर भाषा अलंकृत की जाती थी़……………..जहाँ इनसे आगे कोई बढ़ा कि वह साहित्य में अनभिज्ञ ठहराया गया अर्थात् इन सब नियत उपमाओं का जानना भी आवश्यक समझा जाता था। पाठक् ! यह भाषा की स्तब्धता है, विचारों की शिथिलता है और जाति की मानसिक अवनति का चिह्न है।’’12 इसे संस्कृत का विरोध न समझकर हिन्दी हेतु मौलिक उपमानों की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाना समझा जाना चाहिए। कालांतर में अज्ञेय ने ‘आज ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इनके प्रतीकों से कर गए हैं कूच’ कहकर इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य किया।
उपर्युक्त विचारों के क्रम में कोई स्वतः ही यह गलतफहमी पाल सकता है कि हिन्दी का समर्थन करते हुए शुक्ल जी मुस्लिम और उर्दू विरोधी थे। हिन्दी बनाम उर्दू की इस गलतफहमी को दूर करने तथा इस सम्बन्ध में आयी आपत्तियों को दूर करने के उद्देश्य से शुक्ल जी ने Hindi and Musalman शीर्षक से अंग्रेज़ी में एक विस्तृत लेख लिखा, जिसमें उन्होंने उर्दू को पश्चिमी हिन्दी की एक शाखा बताते हुए स्पष्ट लिखा, ’’ भारत की सभी भाषाओं मे इस समय उर्दू अकेली भाषा है जो ईर्ष्या वश संस्कृत शब्दों से परहेज करती है और केवल अरबी तथा फारसी से खास तौर पर शब्द उधार लेती है। इस प्रकार सभी भाषाओं में व्याप्त सामग्री के अभाव में इसका पृथक अस्तित्व नियत है। (षडयंत्र के तहत यदा-कदा बहक जाने के) वैशिष्ट्य से युक्त उर्दू हिन्दी से पूरी तरह मेल खाती है। घुलने-मिलने की स्वाभाविक प्रक्रिया से भाषा के संघटन में शामिल हो चुके अरबी-फारसी के शब्दों का हिन्दी बेधड़क प्रयोग करती है। हर विद्वान जानता है कि उर्दू कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है। यह पश्चिमी हिन्दी की शाखा मात्र है जिसे मुसलमानों द्वारा अपनी एकांतिक रुचियों और पूर्वाग्रहों के अनुकूल एक निजी रूप दे दिया गया है। इस प्रकार हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा के दो रूप हैं।’’13
हिन्दी और हिन्दुस्तानी में किसे स्वीकार किया जाए, यह प्रश्न उस समय बड़े जोर-शोर से उठाया जा रहा था और यह स्वाभाविक भी था कि शुक्ल जी इस सम्बन्ध में अपना मंतव्य देते। सन 1938 में फैजाबाद के प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन में अभिभाषण देते हुए उन्होंने अपना मार्ग स्पष्ट कर दिया था। कालांतर में यह अभिभाषण प्रारम्भिक दो पैराग्राफ हटाकर नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ‘हिन्दुस्तानी का उद्गम’ शीर्षक से अगले वर्ष छापा गया। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि विदेशी ढांचे की भाषा और साहित्य से भारतीय जनता का भला होने वाला नहीं। वे कहते हैं, ’’ हमारे व्यावहारिक और भावात्मक जीवन से जिस भाषा का सम्बन्ध सदा से चला आ रहा है वह पहले चाहे जो कुछ भी कही जाती रही हो, अब हिन्दी कही जाती है। इसका एक-एक शब्द हमारी सत्ता का व्यंजक है, हमारी संस्कृति का संपुट है, हमारी जन्मभूमि का स्मारक है, हमारे हृदय का प्रतिबिम्ब है, हमारी बुद्धि का वैभव है। देश की जिस प्रकृति ने हमारे हृदय में रूप-रंग भरा है उसी ने हमारी भाषा का भी रूप-रंग खड़ा किया है। यहाँ के वन, पर्वत, नदी, नाले, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी सब इसी बोली में अपना परिचय देते हैं और अपनी ओर हमें खींचते हैं। इसकी सारी रूप छटा, सारी भाव भंगी हमारी भाषा में और हमारे साहित्य में समाई हुई है। यह वही भाषा है जिसकी धारा कभी संस्कृत के रूप में बहती थी, फिर प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में और इधर हजार वर्ष से इस वर्तमान रूप में-जिसे हिन्दी कहते हैं-लगातार बहती चली आ रही है। यह वही भाषा है जिसमें सारे उत्तरीय भारत के बीच चन्द और जगनिक ने वीरता की उमंग उठाई, कबीर, सूर और तुलसी ने भक्ति की धारा बहाई; बिहारी, देव और पद्माकर ने श्रृंगार रस की वर्षा की, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र ने आधुनिक युग का आभास दिया और आज आप व्यापक दृष्टि फैलाकर सम्पूर्ण मानव जगत के मेल में लाने वाली भावनाएँ भर रहे हैं। हजारों वर्ष से यह दीर्घ परम्परा अखण्ड चली आ रही है। ऐसी भव्य परम्परा का गर्व जिसे न हो वह भारतीय नहीं।’’14
इसी अभिभाषण में वे हिन्दी को उर्दू से लड़ाने की अंग्रेजों की दुरभिसन्धि की भी विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं और बताते है कि दिल्ली तथा दक्खिन के बादशाह फारसी कविता का भी आनन्द लेते थे और परंपरागत हिन्दी कविता का भी। वे बताते है कि अकबर ही नहीं औरंगजेब के दरबार में भी हिन्दी के कवि कविता सुनाया करते थे। ‘करबल कथा’ (करबला की कथा), वजही कृत ‘मसनवी कुतुब मुश्तरी’, नसरती, वली, सौदा, नूर मुहम्मद जैसे कवियों-कृतियों के उदाहरण देकर वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि शुरूआत में हिन्दी का मुसलमानों से कोई अलगाव नहीं था, बाद में इसे दूर करने की सोची-समझी साजिश की गयी।15
आज तक हिन्दी को राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा प्राप्त न हो पाने की चर्चा बहुधा की जाती है। शुक्ल जी ने इस पर भी विचार किया था और यह सिद्ध किया था कि हिन्दी वर्षों से इस देश की राष्ट्रभाषा है। ‘हिन्दी की पूर्व और वर्तमान स्थिति’ निबन्ध में उन्होंने अनेक उदाहरण देकर इसकी पुष्टि की है। वे लिखते हैं, ‘‘हिन्दी सारे उत्तरीय भारत की राष्ट्रभाषा पुराने समय में भी थी। मैथिल कवि विद्यापति ठाकुर ने अपने पदों को हिन्दी से मिलती-जुलती भाषा में लिखने के अतिरिक्त कुछ कविताएँ शुद्ध हिन्दी में भी रची हैं। बंग भाषा के पुराने कवि भारतचन्द राय ने भी हिन्दी में कुछ कविताएँ की हैं। इससे प्रतीत होता है कि उत्तरीय भारत में हिन्दी किसी समय साहित्य की परिष्कृत भाषा समझी जाती थी। गुजराती के पुराने नाटकों में पहिले पात्रों का कथोपकथन ब्रजभाषा में कराया जाता था। अब भी गुजरात में ब्रजभाषा का व्यवहार बहुत है। तुलसी, सूर आदि महाकवियों के पद बहुत दूर-दूर तक फैले। जम्मू में ‘सुदामा मन्दिर देख डरे’ आदि पद स्त्रियों में बराबर प्रचलित थे। महाराष्ट्र के राजदरबारों में हिन्दी कवियों का बड़ा मान होता था। हिन्दी पद्य महाराष्ट्र देश में बड़ी चाह से सुने जाते थे। पहिली ही भेंट में भूषण के कवित्तों को सुनकर शिवाजी का प्रसन्न होना यह सूचित करता है कि शिवाजी लिखने पढ़ने की हिन्दी अच्छी तरह जानते थे। पूना, नागपुर, इंदौर आदि के मरहठे दरबारों में हिन्दी के कवियों के रहने का पता बराबर लगता है। अतः यह मान लेने में कोई संकोच नहीं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का रूप पहिले से प्राप्त है।’’16
इन सब बातों के बावजूद शुक्ल जी इस बात से चिन्तित थे कि साहित्येतर विषयों में हिन्दी की व्याप्ति अपेक्षाकृत सन्तोषजनक नहीं है। वे ‘भाषा की उन्नति’ निबन्ध में लिखते हैं,”हिन्दी में अभी जिन-जिन विषयों के अभाव हैं, उनको पूरा करना भिन्न-भिन्न वर्गों के लोगों के हाथ में है। आधुनिक विज्ञान, दर्शन, शिल्प, शासनशास्त्र आदि के पारगामी जो हमारे प्रसिद्ध देशी भाई हैं, हिन्दी की उनसे प्रार्थना है कि वे अपने-अपने विषयों के अच्छे सर्वांगपूर्ण ग्रन्थ या तो स्वयं लिखें या उनकी तैयारी में सहायता दिया करें… क्या सब दिन इस बात की ज़रूरत बनी रहनी चाहिए कि हम पहिले एक विदेशी भाषा सीखने का श्रम उठाएँ तब जाकर कहीं किसी वैज्ञानिक या औद्योगिक विषय का आरम्भ करें। निश्चय समझिए कि विज्ञान और कला आदि जब तक दूसरे की भाषा में हैं तब तक वे दूसरे की सम्पत्ति हैं। फिर हम क्यों न इन विषयों को अपनी पूँजी और अपना सहारा बना लें। इनके बिना पृथ्वी पर की कोई जाति अब अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती।’’17
वे चाहते थे कि देशी भाषाओं को देश के शिक्षण का माध्यम बनाया जाए और उनका अभिमत था कि इसके लिए हिन्दी को अगुआई करने हेतु आगे आना होगा। The Indian People पत्र के 6 जुलाई सन 1905 के अंक में उन्होंने इस हेतु The state of a vernacular शीर्षक से एक विस्तृत लेख लिखा था। इस लेख की शुरूआत में ही वे लिखते हैं, ‘‘मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के दावे पर प्रश्न खड़ा करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसके विपरीत मैं तो उन भाषाओं को एकमात्र ऐसा भण्डार मानता हूँ जिसमें भावी पीढ़ियों के उपयोग के लिए हम विश्वासपूर्वक अपनी अपेक्षाएँं संचित कर सकते हैं। इसके व्यावहारिक परिणाम के रूप में हिन्दी की स्थिति ने कुछ समय पूर्व से मेरा ध्यान आकृष्ट किया है।’’18 लेकिन वे इस बात से दुखी भी थे कि हिन्दी के तथाकथित विद्वान आत्ममुग्धता में निमग्न हैं तथा व्यक्तिगत उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटते हुए हिन्दी के विकास की धार को कहीं न कहीं अवरुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं।
आचार्य शुक्ल समस्त भारत के लिए एक भाषा के पक्षपाती थे। ‘एक नया आन्दोलन’ निबन्ध में वे इसका समर्थन करते हुए संस्कृत और अंग्रेज़ी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरूद्ध मत व्यक्त करते हुए संस्कृत का व्याकरण अत्यधिक जटिल होने तथा अंग्रेज़ी के विदेशी भाषा होने का ज़िक्र करते हैं। इसके विपरीत हिन्दी का व्याकरण सीधा और सरल होने तथा सम्पूर्ण देश में इसकी व्याप्ति होने के कारण हिन्दी को देश की एक भाषा के रूप में रखे जाने की वजह स्वीकारते हैं।19
स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल हिन्दी के मुखर और प्रबल समर्थक थे। उन्होंने बगैर किसी लाग लपेट के हिन्दी के विकास के लिए देश के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आने का आह्वान किया और हिन्दी बनाम उर्दू की बहस को व्यर्थ बताते हुए हिन्दी के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध की। उनका यह मन्तव्य था कि यदि देश को एकता के सूत्र में बाँधना है तो हिन्दी परस्पर सम्पर्क की भाषा बनकर यह कार्य सुगमतापूर्वक कर सकती है। समय ने उनके विचारों को सत्य सिद्ध करने का कार्य किया और आज हिन्दी का ध्वज समस्त विश्व में शान से लहरा रहा है।
सन्दर्भ सूत्र :
1. सिंह, ओमप्रकाश आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली, भाग-8, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, वर्ष 2000, पृष्ठ 243
2. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, हमारी हिन्दी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, काशी, सितम्बर-दिसम्बर 1917 अंक।
3. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, भारतेन्दु-जयन्ती, इन्दु पत्रिका, सितम्बर 1913 अंक।
4. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, नागरी प्रचारणी पत्रिका, काशी, अगस्त 1912 अंक।
5. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, श्रीयुत् बा. देवकीनन्दन खत्री का वियोग, इन्दु पत्रिका, अगस्त 1913 अंक।
6. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, रसमीमांसा, नागरी प्रचारणी सभा, काशी, संवत् 2048, षष्ठ संस्करण, पृष्ठ 29-34
7. चतुर्वेदी, रामस्वरूप, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल: आलोचना का अर्थः अर्थ की आलोचना, लोकभारती, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2001, पृष्ठ 81
8. चतुर्वेदी, रामस्वरूप, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल: आलोचना का अर्थः अर्थ की आलोचना, लोकभारती, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2001, पृष्ठ 82
9. चतुर्वेदी, रामस्वरूप, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल: आलोचना का अर्थः अर्थ की आलोचना, लोकभारती, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2001, पृष्ठ 83
10. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, अपनी भाषा पर विचार, आनन्दकादम्बिनी, ज्येष्ठ अग्रहायण संवत् 1964 वि., सन 1907 अंक, चिंतामणि भाग-3
11. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, उर्दू राष्ट्रभाषा, नागरी प्रचारणी पत्रिका, काशी, दिसम्बर 1909 अंक।
12. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, अपनी भाषा पर विचार, आनन्दकादम्बिनी, ज्येष्ठ अग्रहायण संवत् 1964 वि., सन 1907 अंक, चिंतामणि भाग-3
13. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, हिन्दी और मुसलमान, द लीडर, इलाहाबाद में 19 अप्रैल सन 1917 को अंग्रेज़ी में प्रकाशित, जिसका अनुवाद विवेकानंद उपाध्याय तथा आलोक कुमार सिंह ने किया तथा सिंह, ओमप्रकाश आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली, भाग-4, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, वर्ष 2000, पृष्ठ 56 में संकलित।
14. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सन 1938 में फैजाबाद के प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन में दिया गया अभिभाषण, जो ‘हिन्दुस्तानी का उद्गम’ शीर्षक से नागरी प्रचारणी सभा, काशी द्वारा लघु पुस्तिका के रूप में छापा गया तथा सिंह, ओमप्रकाश आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली, भाग-4, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, वर्ष 2000, पृष्ठ 63-64 में संकलित।
15. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सन 1938 में फैजाबाद के प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन में दिया गया अभिभाषण, जो ‘हिन्दुस्तानी का उद्गम’ शीर्षक से नागरी प्रचारणी सभा, काशी द्वारा लघु पुस्तिका के रूप में छापा गया तथा सिंह, ओमप्रकाश आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली, भाग-4, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, वर्ष 2000, पृष्ठ 65-72 में संकलित।
16. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, ‘हिन्दी की पूर्व और वर्तमान स्थिति’, नागरी प्रचारणी पत्रिका, काशी, मार्च 1911 अंक।
17. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, ‘भाषा की उन्नति’, नागरी प्रचारणी पत्रिका, काशी, जनवरी 1910 अंक।
18. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, ‘देशी भाषा की दशा’, द इण्डियन पीपुल’ में 6 जुलाई सन 1905 को तथा 30 जुलाई 1905 को ‘एडवोकेट’ में अंग्रेज़ी में प्रकाशित, जिसका अनुवाद आलोक कुमार सिंह ने किया तथा सिंह, ओमप्रकाश आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली, भाग-4, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, वर्ष 2000, पृष्ठ 3 में संकलित।
19. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, ‘एक नया आन्दोलन’, नागरी प्रचारणी पत्रिका, काशी, दिसम्बर 1909 अंक।