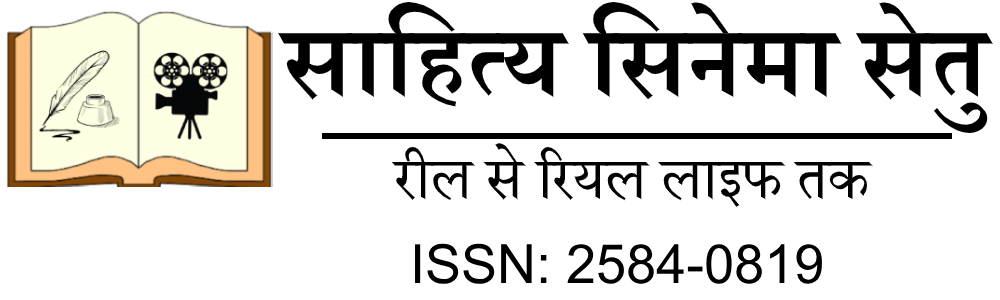हिंदी में अजब घटतौली है। कमोवेश हर जगह। क्या प्रकाशक, क्या संपादक, क्या अखबार या पत्रिकाएं। सब के सब एक लेखक नाम के प्राणी को गरीब की जोरु को भौजाई बनाने का सुख लूट रहे हैं। जाने कब से। पहले जब लिखना शुरू किया था तब लगता था कि लिख कर हम अपने को कागज पर रख रहे हैं। सब के सामने आने के लिए। एक स्वर्गानुभुति भी कह सकते हैं। छपने का तो शुरू में सोचते भी नहीं थे। लिखना ही लिखना था। बाद के दिनों में कहीं छपना भी एक सपना हुआ करता था। छपना ही। पैसा नहीं। पैसे का सपना नहीं। लिख कर पैसा भी मिलेगा ऐसा कभी तब सोचा भी नहीं था। पर जब पहली बार एक कविता आज अखबार में छपी तो लगा कि क्या पा गए हैं।
दस रुपए का मनीआर्डर भी बाद में आया। तब के दिनों में दस रुपए की नोट का आकार भी आज के सौ रुपए के लगभग हुआ करता था। और उस का मूल्य तो आज के सौ रुपए से निश्चित ही ज़्यादा था। यह १९७७ या १९७८ की बात है। बहुत दिनों तक क्या कई महीनों तक वह दस रुपए भी कभी इस किताब, उस किताब के पन्नों में सहेज कर रखे रहा था। जल्दी ही आकाशवाणी से युववाणी कार्यक्रम में कविता पढ़ने पर पचीस रुपए का चेक मिला। रेडियो पर कविता पढ़ने का सुख अलग और पैसा पाने का सुख अलग। कवि सम्मेलनों में तो कभी कभार सौ रुपए तक मिले। मार्ग व्यय अलग। पर कविता पढ़ने और छपने का ही सुख ज़्यादा बड़ा था। पैसे का नहीं। क्यों कि मुझे याद है कि वह पहला चेक भी जो आकाशवाणी से मिला था, बहुत दिनों तक सहेज कर रखे रहा था। बाद में लोगों ने बताया कि तीन महीने बाद चेक की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तब कहीं स्टेट बैंक जा कर वह चेक भुनाया था। तब विद्यार्थी था और कोई ऐसी वैसी आदत थी नहीं कि पैसे उड़ा देता। बाद के दिनों में तो छपना भी नियमित हो गया। और पारिश्रमिक कहिए, मानदेय कहिए वह बढ़ कर कहीं पचीस तो कहीं तीस रुपए का हो गया। आज, दैनिक जागरण या इन की कंचनप्रभा या अवकाश पत्रिकाओं में भी। नवभारत टाइम्स या हिंदुस्तान अखबार में भी। आकाशवाणी पर भी चालीस रुपए मिलने लगे। नाटक लिखने के तो डेढ़ सौ रुपए मिलने लगे। और १९७८ में ही सारिका में प्रेमचंद पर एक फ़ीचर छपा तो डेढ़ सौ रुपए मिले। धर्मयुग, दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान से भी कभी डेढ़ सौ रुपए से कम का भुगतान नहीं मिला। रविवार ने तभी दो सौ रुपए का भी चेक भेजा था। बावजूद इस सब के तब भी पैसा नहीं, रचना का छपना ही मह्त्वपूर्ण था।
नया प्रतीक में अज्ञेय जी ने एक गीत छापा उन्हीं दिनों। सव्यसाची ने उत्तरार्द्ध में कविता छापी। एक पैसा नहीं मिला। पत्रिका भी खरीदनी ही पड़ी। लेकिन यहां छपने का सुख और ज़्यादा था। उन्हीं दिनों एक रिपोर्ट दिनमान को भेजी थी। वह मत सम्मत में छप गई। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ने तब रघुवीर सहाय को एक चिट्ठी लिख कर अपना कड़ा प्रतिरोध दर्ज करवाया था। मैं ने लिखा था कि संपादक के नाम पत्र नहीं रिपोर्ट भेजी थी आप को। और आप ने उसे पत्र बना दिया। सहाय जी का जवाब आया था। उन्हों ने लिखा था कि दिनमान का मत सम्मत भी महत्वपूर्ण होता है। आप की रिपोर्ट तभी छापनी ज़रुरी लगी और अन्यत्र जगह थी नहीं, बाद में विलंब हो जाता इस लिए मत सम्मत में प्रकशित की गई। आप निश्चिंत रहें आप को पारिश्रमिक भी समय से भेजा जाएगा। समय से मुझे डेढ़ सौ रुपए का चेक मिला भी। उन दिनों लगभग परंपरा सी थी तब सभी जगह कि रचना छपने के तीन महीने बाद ही भुगतान मिल जाता था। किसी से कुछ कहना या लिखना नहीं होता था। मुझे याद है कि अमृत प्रभात तो तब मनीआर्डर का कमिशन भी काट लेता था। पोस्टमैन को दिक्कत होती थी चालीस रुपए के पेमेंट में सैंतीस रुपए कुछ पैसे देने में। दिल्ली प्रेस की पत्रिकाएं तो रचना स्वीकृत करने के साथ ही डेढ़ सौ रुपए का चेक भेज देती थीं। रचना चाहे जब छपे। बाद के दिनों मैं गोरखपुर से दिल्ली चला गया सर्वोत्तम रीडर्स डाइजेस्ट में नौकरी करने लगा। वहां यह देख कर मुदित हो गया कि एक लेख के पांच हज़ार रुपए से भी अधिक का पारिश्रमिक मिलता था। यह १९८१ की बात है। बाद में जनसत्ता गया नौकरी करने। १९८३ में। तो वहां भी एक लेख के तब तीन सौ से पांच सौ तक का पारिश्रमिक दिया जाता था। और पूरे सम्मान से। न संपादक घिघियाते थे न लेखक। हां यह ज़रुर कई बार देखा कि अगर लेखक को ज़रुरत है तो रचना या लेख छपते ही संपादक एक चिट्ठी प्रबंधन को लिख देते थे और उस का भुगतान तुरंत मिल जाता था। मुझे खुद कई बार ऐसा सुख मिला है। दिनमान में रघुवीर सहाय और सारिका में कन्हैयालाल नंदन ने ऐसी कई चिट्ठियां मेरे लिए लिखीं और मुझे तुरंत भुगतान मिल गया।
यही हाल प्रकाशकों का भी तब के दिनों था। मेरा पहला उपन्यास दरकते दरवाज़े १९८३ में प्रभात प्रकाशन के श्यामसुंदर जी ने छापा था। उपन्यास स्वीकृत होते ही उन्हों ने अनुबंध किया और ढाई हज़ार रुपए तुरंत नकद दिए। यही काम हिंदी पुस्तक संस्थान के प्रकाशक ने किया। जिस ने मेरा पहला कहानी संग्रह संवाद और दूसरा उपन्यास जाने अनजाने पुल छापा था। किताब छपने के पहले ही पैसा दे दिया। हिंद पाकेट बुक्स के दीनानाथ जी ने भी यही किया। पर अब? अब यह सब बीते समय की बातें हैं। कहें कि बीता युग है। प्रकाशक कहते हैं कि किताब अब बिकती नहीं। पैसा कहां से दें? हालत यह है कि प्रकाशक कागज़ से लगायत छपाई, बाइंडिंग तक के पैसे कई बार ऐड्वांस दे देता है। दुकानदारों को ४० से ५० प्रतिशत कमिशन देता है। सरकारी खरीद के लिए अफ़सरों को अस्सी प्रतिशत तक रिश्वत देता है। खरीद के पहले ही। कई बार यह पैसा डूब भी जाता है तो भी देता है। पर नहीं देता तो सिर्फ़ लेखक को सो काल्ड रायल्टी नहीं देता। उस को पसीना आ जाता है। तमाम किस्म की दिक्कतें आ जाती हैं। और वह घुमा देता है। तो क्यों? और तो और अब तो बहुतायत में लोग लोग प्रकाशक को पैसा दे कर किताबें छपवाने लगे हैं। सारा खर्च लेखक का और सारा फ़ायदा प्रकाशक का। निर्मल वर्मा ने अपने निधन के कुछ समय पहले राजकमल प्रकाशन से अपनी रायल्टी का हिसाब मांगा। उन का निधन हो गया पर राजकमल वाले माहेश्वरी बंधु ने उन की रायल्टी का हिसाब नहीं दिया। उन के निधन के बाद उन की पत्नी गगन गिल ने हिसाब मांगा। राजकमल के स्वामी ने देश भर के लेखकों को चिट्ठी लिख कर दुनिया भर की बातें बताईं पर गगन गिल को रायल्टी का हिसाब नहीं दिया। राजकमल वालों ने अपने पत्र में गगन जी की चरित्र हत्या तक की कोशिश की। और प्रकारांतर से यह जताने की कोशिश की कि गगन गिल निर्मल वर्मा की पत्नी नहीं रखैल हैं। चिट्ठी में कहा कि निर्मल जी की व्याहता पत्नी की एक बेटी भी है। गगन गिल को भी मजबूर हो कर देश भर के लेखकों को चिट्ठी लिख कर अपनी सफाई देनी पड़ी। गगन जी को विवश हो कर लिखना पड़ा कि मैं निर्मल वर्मा की व्याहता पत्नी हूं। और कि वह अपनी वसीयत में सब कुछ मुझे सौंप गए हैं। किताबों की कापीराइट भी। और कि उन की बेटी को भी किसी बात पर ऐतराज़ नहीं है। फिर भी राजकमल ने उन्हें रायल्टी नहीं दी। फिर तो हर पुस्तक मेले में वह निर्मल जी की किताब ले कर राजकमल के खिलाफ़ खडी होने लगीं, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। फिर कहीं राजकमल से निर्मल जी की सारी किताबें उन्हों ने वापस लीं। निर्मल वर्मा ने अपने निधन के पहले एक लेख भी लिखा था इस मामले पर। इस लेख में उन्हों ने बताया था कि दिल्ली में हिंदी के कई प्रकाशकों को वह व्यक्तिगत रुप से जानते हैं। जिन के पास हिंदी की किताब छापने और बेचने के अलावा कोई और व्यवसाय नहीं है। और यह प्रकाशक कह्ते हैं कि किताब बिकती नहीं। फिर भी वह यह व्यवसाय कर रहे हैं। न सिर्फ़ यह व्यवसाय कर रहे हैं बल्कि मैं देख रहा हूं कि उन की कार लंबी होती जा रही है, बंगले बडे़ होते जा रहे हैं, फ़ार्म हाऊसों की संख्या बड़ी होती जा रही है तो भला कैसे?
निर्मल जी के इस सवाल का किसी प्रकाशक ने आज तक पलट कर जवाब देने की ज़रुरत नहीं समझी। एक बार नेशनल बुक ट्रस्ट के पुस्तक मेले में रवींद्र कालिया ने कहा कि प्रकाशक अब पांच सौ से तीन सौ प्रतियों के संस्करण पर आ गए हैं। बाद में जब वह मंच से उतर कर चाय वाय पीने लगे तो मैं ने उन से कहा कि उत्तर प्रदेश में आप के कुछ मित्र आई. ए. एस. अफ़सर हैं। कुछ सरकारी खरीद की जानकारी मैं आप को दे रहा हूं। आप चाहें तो अपने दोस्तों से कह कर यह तो पता करवा ही सकते हैं कि किस किस खरीद में आप की कौन- कौन सी किताब कितनी- कितनी खरीदी गई है। पता चल जाएगा कि किताब कितनी छपती है? पर जाने क्यों कालिया जी ने बात को सुन कर अनसुना कर दिया। कुछ बोले नहीं। शायद वह हमाम का नंगापन जानते रहे होंगे तभी चुप रहे। सचाई यह है कि प्रकाशक किसी किताब का पहला संस्करण ज़रुर पांच सौ का छापते हैं। पर यह बेचने के लिए नहीं। सिर्फ़ सबमिशन के लिए। इतनी योजनाओं में इतनी खरीदें हैं कि यह पांच सौ किताबें भी सबमिशन के लिए कम पड़ जाती हैं प्रकाशकों को। फिर तो जैसे -जैसे आर्डर मिलता जाता है किताबें छपती जाती हैं। एक- एक हफ़्ते में कई -कई संस्करण एक किताब के छप जाते हैं। लेकिन प्रकाशक के यहां लेखक के लिए वही पहला संस्करण दिखता रहता है। दस साल बाद भी अगर उसी किताब का पहला संस्करण बिल्कुल ताज़े कागज़ पर दिख जाए तो हैरत में बिलकुल नहीं पड़ें। आप का ही कहानी संग्रह आप ही के नाम से किसी और प्रकाशक या किसी और शीर्षक से छपा मिल जाए तो भी मत चौंकिए। सरकारी खरीद का गुणा-भाग मान लीजिए इसे। लेखक छोटा है या बड़ा इस से भी इन बातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पहला उपन्यास जब छपा था तो कह सुन कर उस की समीक्षा कई जगह छपवा ली। अच्छी-अच्छी। कुछ जगह अपने आप भी छप गई। तो मेरा दिमाग थोड़ा खराब हुआ। मन में आया कि अब मैं बड़ा लेखक हो गया हूं। कोई पचीस-छब्बीस साल की उम्र थी, इतराने की उम्र थी, सो इतराने भी लगा। प्रभात प्रकाशन के श्यामसुंदर जी ने इस बात को नोट किया। एक दिन मेरे इतराने को हवा देते हुए बोले, ‘अब तो आप बडे़ लेखक हो गए हैं! अच्छी-अच्छी समीक्षाएं छप गई हैं।’ मैं ने ज़रा गुरुर में सिर हिलाया। और उन से बोला, ‘आप का भी तो फ़ायदा होगा!’
‘वो कैसे भला?’
‘आप की किताबों की सेल बढ़ जाएगी !’ मैं ज़रा नहीं पूरे रौब में आ कर बोला।
‘यही जानते हैं आप?’ श्यामसुंदर जी ने अचानक मुझे आसमान से ज़मीन पर ला दिया। अमृतलाल नागर, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर आदि तमाम बडे़ लेखकों की किताबों के साथ मुझ जैसे कई नए लेखकों की कई किताबें एक साथ मेज़ पर रखते हुए वह बोले, ‘इन में से सभी लेखकों की किताबें बेचने के लिए मुझे एक जैसी तरकीब ही लगानी पड़ती है।’
‘क्या?’ मैं चौंका।
‘जी!’ वह बोले, ‘बिना रिश्वत के एक किताब नहीं बिकती। वह चाहे बड़ा लेखक हो या घुरहू कतवारु। सब को रिश्वत दे कर ही बेचना होता है। बाज़ार का दस्तूर है यह। बड़ा लेखक दिखाऊंगा तो दो चार किताबें खरीद ली जाएंगी। तो उस से तो हमारा खर्च भी नहीं निकलेगा।’
हकीकत यही थी। मैं चुप रह गया था तब। पर तब श्यामसुंदर जी, दीनानाथ जी या अन्य प्रकाशक भी लेखक को रायल्टी के नाम पर कुछ पैसा देते ज़रुर थे। उन दिनों यह एक चलन सा था कि अगर हज़ार पांच सौ रुपए की तुरंत ज़रुरत हो तो बच्चों की पांच सात छोटी-छोटी कहानियां लिख कर प्रकाशक के पास चले जाइए पैसा मिल जाता था। श्रीलाल शुक्ल बताते थे कि एक बार वह दिल्ली गए तो राजकमल प्रकाशन की मालकिन शीला संधु मिलने आईं। नई किताब मांगी। बेटे ने एडवांस के रुप में पचास हज़ार मांग लिया। दूसरे दिन शीला जी ने पचास हज़ार रुपए भिजवा भी दिए। यह अस्सी के दशक की बात है। अब मैं खुश कि हिंदी के लेखक की यह हैसियत हो गई है कि एक किताब के पचास हज़ार रुपए एडवांस भी मिल सकते हैं। पर बाद में पता चला कि यह खुशी बेकार ही थी। साल के आखिर में जब किताबों की रायल्टी का हिसाब हुआ तो वह पचास हज़ार रुपया उस में एड्जस्ट हो गया। एक घटना और। श्रीलाल जी बाद में प्रकाशकों और अखबार वालों की कृपणता से इतने उकता गए कि एक बार अमर उजाला में उन का इंटरव्यू छपा तो उन्हों ने बाकायदा अखबार को नोटिस दे कर उस इंटरव्यू का पैसा मांग लिया। हिंदी में अभी तक यह चलन नहीं है कि आप किसी को इंटरव्यू लेने के लिए पैसे दें। हां उलटे कुछ फ़िल्म स्टार या कुछ व्यवसायी ज़रुर ऐसा करते हैं कि पैसा दे कर इंटरव्यू छपवाते हैं। पर कई सारी भाषाओं में चलन है कि इंटरव्यू लेने के लिए भी संबंधित व्यक्ति को पैसे देने पड़ते हैं। याद कीजिए फूलन देवी के इंटरव्यू जिस पत्रकार ने लिए थे और उस की बायग्राफी लिखी थी उस ने फूलन देवी को बाकायदा और अच्छा खासा भुगतान दिया था, एडवांस। साथ में रायल्टी भी शेयर की थी। तो श्रीलाल जी ने नोटिस दे कर पैसा मांगा। अखबार के हाथ पांव फूल गए। रिपोर्टर को तलब किया गया। सब कुछ किया गया पर अंतत: श्रीलाल जी को अखबार ने पैसा नहीं दिया तो नहीं दिया। माफी मांग कर इतिश्री कर ली। श्रीलाल जी को जब लगातार कुछ पुरस्कार मिले तो वह एक बार बहुत प्रसन्न हो कर कहने लगे कि इतना पैसा तो रायल्टी में भी नहीं मिला अब तक। एक बार मनोहर श्याम जोशी को एक अखबार ने एक पुरस्कार योजना के निर्णायक मंडल में मनोनीत किया तो उन्हों ने छूटते ही पूछा कि पैसा कितना मिलेगा? सुनने वालों को यह अच्छा नहीं लगा। लोगों को लगा कि हिंदी का लेखक पैसा भी मांग सकता है? यह सब हिंदी के लेखकों के साथ ही क्यों होता है भला?
सोचिए कि उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान के ८३ पुरस्कारों में से ८० पुरस्कार मायावती ने एक झटके में खत्म कर दिए। अशोक वाजपेयी ने इस के विरोध में भारत भारती जैसा संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया। पर मायावती सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगा। जब कि यहीं उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का एक भी पुरस्कार छूने की हिम्मत मायावती की नहीं हुई। उलटे पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी कर उसे पांच लाख का कर दिया। जब कि हिंदी में भारत भारती ढाई लाख का ही है। यही नहीं आप देख लीजिए कि हिंदी में दिए जाने वाले साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या व्यास सम्मान धनराशि के मामले में भी बुकर, मैगसेसे या नोबल के आगे किस कदर बौने की हैसियत में भी खडे़ नहीं हो पाते। तब जब कि यह दुनिया में सब से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और तो छोडिए कौन बनेगा करोड़पति समेत जाने कितने शो हैं जिस में लोग आनन फानन जाने लाखों रुपए पा जाते हैं। बताते हुए खुशी होती है कि कहानी उपन्यास आदि की मेरी कोई १८ किताबें हैं। पर प्रकाशक से जब कभी रायल्टी की बात चलाता हूं तो बस एक ही जवाब होता है। प्रकाशक कहता है कि आप की रायल्टी तो यह अफ़सर खा जाते हैं। इन अफ़सरों से छुट्टी दिलवाइए तो आप को रायल्टी देता हूं। इस में सारा संकेत यह होता है कि मैं अपनी किताबों की सरकारी खरीद खुद करवाऊं कह सुन कर या जैसे भी। तो वह कमीशन या रिश्वत जो सरकारी अमला खाता है उस का कुछ टुकड़ा मेरे हिस्से भी आ जाएगा। सो मैं हाथ जोड़ लेता हूं। और बिना रायल्टी के ही संतोष करता हूं। पैसा दिए बिना किताब छप जाती है यही सोच कर खुश हो लेता हूं।असल में हुआ यह कि इधर के दिनों में तमाम सरकारी अफ़सर-कर्मचारी भी लेखक हो चले हैं। सो वह किताब छापने के लिए पैसे भी देते है, खरीद भी करवाते हैं। खुद भी कमाते हैं और प्रकाशक को भी कमवाते हैं। पहले के दिनों में ऐसा ऐसा कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यापक करते थे। पाठ्यक्रम की चार किताबों के साथ अपनी कोई कविता कहानी की किताब भी थमा देते थे। खरीद समितियों में भी वह होते ही होते थे। सो प्रकाशक उन्हें उपकृत करते रहते थे। पर यह सब कुछ दबे ढंके था। पर अफ़सरों के लेखक बनने और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को प्रोन्नति किताब के आधार पर कर देने से खुला खेल फरुखाबादी हो चला है। बहुतेरे प्रकाशक तो लेखकों से किताब छापने का पैसा ले कर डकार भी जाते हैं। किताब नहीं छापते। पैसा भी वापस नहीं देते। कई बार कुछ प्रकाशक पैसा ले कर भाग भी जाते हैं। अकसर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। लेखकों में खेमेबाज़ी का नमो अंधकारम अलग है। रिश्वत अब ग्लोबलाइज़ है। हिंदी किताबें भी इस का शिकार हैं। लेकिन यही भर कह देने से काम नहीं चलता। हकीकत यह है कि यही हिंदी प्रकाशक जब अरुंधति राय या तसलीमा नसरीन को छापने पर आते हैं तो उन के पास घुटने टेकते हुए पहुंचते हैं और एडवांस और मुंहमांगी रायल्टी दे कर किताब का आनन फानन अनुवाद एडवांस दे कर सर के बल हो कर करवाते हैं। तो क्या हिंदी में किताब बिकती है? कोई इन प्रकाशकों से नहीं पूछता। सोचिए कि बांगला के विमल मित्र तक के परिवार के लोगों को यही हिंदी प्रकाशक रायल्टी देते नहीं अघाते। तो फिर यह सारी नौटंकी सिर्फ़ हिंदी लेखकों के लिए ही है?
कारण साफ है कि सरकार भी नहीं चाहती कि लोग पढ़ें। वह चाहती ही है कि लोग टी.वी. के सास बहू, लाफ़्टर चैलेंज, बिग बास टाइप के फालतू कार्यक्रम देख कर नपुंसक विचारों के हवाले हो जाए। क्यों कि अगर लोग पढ़ेंगे तो सोचेंगे। सोचेंगे तो सिस्टम और सरकार के खिलाफ ही तो सोचेंगे? पर लोग हैं कि लिखना छोड़ नहीं रहे। तो सरकार लोगों के लिखे को सरकारी लाइब्रेरी में कैद करती जा रही है। प्रकाशक मालामाल होते जा रहे हैं। अफ़सरों की ज़ेब भरती जा रही है। अब कितने लोग जानते हैं कि सिर्फ़ साक्षरता की हिंदी किताबों के नाम पर ही एक-एक ज़िले में करोडों रुपए का बजट हर साल स्वाहा हो जाता है! बाकी की तो खैर बात ही क्या? हालत यह है कि सभी प्रदेशों में तमाम विभागों के अलग-अलग बजट हैं हिंदी किताबों खातिर। मानव संसाधन विभाग राजा राममोहन राय योजना की खरीद में हर साल न सिर्फ़ करोडों-करोड़ रुपए हिंदी किताबों की खरीद पर खर्च करता है बल्कि किताब रखने के लिए आलमारी तक खरीदने का बजट भी देता है। जो लेखक या अधिकारी इस की खरीद समिति में आते हैं एक ही साल में मालामाल हो जाते हैं। बहुतेरे विदेशी भाषाओं की किताबें भी प्रकाशक इस खरीद में पाट देते हैं। वह किताबें जो रायल्टी से फ़्री हैं। टालस्टाय, हेमिंग्वे से लगायत प्रेमचंद, शरतचंद आदि भी। यानी जो रायल्टी से फ़्री हो गई किताब हो प्रकाशक को मुफ़ीद पड़ती है। नामा और नाम दोनों ही उन के हिस्से आ जाते हैं। सरकारी अमला आंख मूंद कर खरीद जारी आहे! की मुनादी करता रहता है। बताते हुए तकलीफ़ होती है कि एक बार तो इस खरीद समिति के अध्यक्ष एक नामवर आलोचक बनाए गए थे। सारी खरीद उन्हों ने अपने एक चहेते प्रकाशक को ही थमा दी। इतनी कि दाल में नमक हो गया। जांच शुरु हो गई। जेल जाने की नौबत आ गई। कि एक नामवर कवि और आलोचक ने अपने प्रशासनिक अधिकारी होने का हुनर दिखाया। और अध्यक्ष महोदय बच गए। बचाने वाले को ज़िंदगी भर खारिज़ किए रहे थे, उस से उपकृत हो कर उसे साहित्य अकादमी से नवाज़ दिया। बात चर्चा-कुचर्चा में ही निपट गई। यह और ऐसे तमाम प्रसंग किताब खरीद के किस्सों से रंगे पडे़ हैं। रेलवे, सेना, बैंकों और दूतावासों में भी हिंदी किताबों की भारी खरीद होती है। और हमारे प्रकाशक लोग जब लेखकों को रायल्टी देने की बात आती है तो कहते हैं कि क्या करें किताबें बिकती ही नहीं। और गुस्सा तब आता है जब इन खरीद कमेटियों में शामिल मठाधीश लेखक भी यह सब कान में तेल डाल कर न सिर्फ़ सुनते रहते हैं बल्कि यथास्थितिवादी बन आंख भी मूंदे रहते हैं।
एक समय जब दूरदर्शन का ज़माना था तब के दिनों धारावाहिकों में काम करने वाले कलाकारों का शोषण बहुत बढ़ गया था। ज़्यादातर निर्माता कलाकारों का पारिश्रमिक घाटा हो गया के नाम पर मार देते थे। जब अति हो गई तब दूरदर्शन ने एक नियम बना कर निर्माता को कलाकारों की तरफ़ से एन.ओ.सी. देना अनिवार्य कर दिया। अगर कोई कलाकार निर्माता के खिलाफ अगर झूठ भी शिकायत कर देता तो उस का प्रसारण और भुगतान रोक दिया जाता था। कलाकारों का शोषण लगभग रुक गया। अब कोई शोषण करवाने पर ही आमादा हो तो बात और है। तो क्या यह सरकारें भी ऐसा कुछ नहीं कर सकतीं? कि लेखकों की एन.ओ.सी. कि किताब की रायल्टी मिली, तभी किताबों का भुगतान करे। और कि यह भी ज़रुर सुनिश्चित करे सरकार कि उस किताब का सचमुच ही पहला संस्करण है और कि वह अनुदित किताब नहीं है। अनूदित किताब का कोटा भी सुनिश्चित कर दिया जाए। न सही पूरी तरह अधिकांश समस्या तो खत्म होगी ही। नहीं अपने देश में हिंदी के लेखकों की हैसियत किसानों मज़दूरों से भी गई बीती है। कि उन्हें अपने काम की मज़दूरी नहीं मिलती बल्कि इस बारे में प्रकाशक, लेखक, सरकार या समाज सोचता भी नहीं। यह कौन सा समाज हम गढ़ रहे हैं? इस पर अब सोचना बहुत ज़रुरी हो गया है।
अब दखिए इन दिनों एक अखबार निकला है लखनऊ से जनसंदेश टाइम्स। सुभाष राय इस के संपादक हैं। खुद कवि, लेखक हैं सो अखबार में भी साहित्य के लिए, विचार के लिए भरपूर स्पेस रखते हैं। शुरु के दिनों में ज़्यादातर लिफ़्ट कर के छापते थे। अब कुछ लोगों को जोड़ कर कुछ नया भी करने लगे हैं। अखबार में विज्ञापन नहीं के बराबर है सो खाली जगह का स्पेस वह साहित्य से भरने की कोशिश करते हैं। लगभग अति उत्साह में हैं कि वह कुछ नया और हटके कर रहे हैं। ऐसा वह जब -तब यत्र -तत्र लिख कर जताते भी रहते हैं। अपनी संपादकीय में, ब्लाग पर, फ़ेसबुक आदि पर भी। इधर लगभग दूसरी बार उन्हों ने लिख कर लेखकों से कहा है कि वह सब को पारिश्रमिक नहीं दे पा रहे और कि देर सवेर देंगे ज़रुर। उन्हों ने अपनी पीठ भी ठोंकी है साथ में अपने एक सहयोगी हरे प्रकाश उपाध्याय का नाम भी नत्थी किया है और कहा है कि मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे लिए और हरे के लिए ही लिखते हैं, आदि आदि। और फिर वही कि पैसा नहीं दे पा रहे हैं। एक बार ऐसा वह अखबार के संपादकीय में भी लिख चुके हैं, अब की फ़ेसबुक पर लिखा देखा। और फ़ेसबुकियों को तो आप लोग जानते ही हैं, सब साथ हो लिए हैं उन की इस पैसा न दे पाने की मुहिम में कंधा देने को, शहीद बनने को पूरे वीर रस में तैयार! एक सज्जन तो जाने कितना वेतन पाते हैं कि अपना वेतन देने को भी तैयार बता गए हैं। अजब है यह सब! एक आदमी है कि मंहगाई के विरोध में शरद पवार को थप्पड़ रशीद कर देता है। और यह जनाब हैं कि ऐसे में अपना वेतन बलिदान कर देने पर आमादा हैं। खुद क्या खाएंगे और परिवार को क्या खिलाएंगे इस की फिकर नहीं है। अखबार छपता रहे इस के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं। खैर। लेकिन पूछने को मन करता है सुभाष राय से उन की सारे नेक इरादे के बावजूद कि यह अपील सिर्फ़ लेखकों से ही क्यों कर रहे हैं? हाकरों से भी क्यों नहीं करते कि बिना कमीशन लिए अखबार बेचें। कागज़ जहां से खरीदते हैं उस से भी यह अपील क्यों नहीं दुहराते। या ऐसे ही तमाम तमाम और लोगों से जो अखबार छापने के मद्देनज़र खर्च करवाते हैं उन से भी यह अपील क्यों नहीं करते कि भैय्या हम साहित्य संस्कृति को छाप रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं आप हम से कुछ नहीं लें या थोड़ा लें या बाद में लें! अदभुत है यह। एक गया गुज़रा अखबार भी छापने में रोज लाखों रुपए खर्च होते ही हैं, यह सब जानते हैं। और लेखक के मद में कोई अखबार ज़्यादा से ज़्यादा दो चार पांच हज़ार से ज़्यादा कम से कम हिंदी में तो नहीं ही खर्च करता। तो यह क्या है? अरे आप मत दीजिए एक भी पैसा लेखक को। पर यह बार-बार लिख कर आप क्या जताना चाहते हैं? हिंदी के तमाम अखबार और पत्रिकाएं नहीं देते लेखकों को एक भी पैसा। प्रकाशक भी नहीं देते तो क्या लोग लिख नहीं रहे? लिखना क्या खत्म हो गया? कि हो जाएगा? यह सारा उपक्रम सिर्फ़ ऐसे लेखकों के लिए है जो बाज़ार में नहीं हैं। नहीं कौन नहीं जानता कि कुछ व्यंग्यकार और लेखक बिना पैसे लिए कहीं नहीं लिखते। और वह जनसंदेश टाइम्स में न सिर्फ़ छप रहे हैं बल्कि नियमित छप रहे हैं। यह सब उन्हीं लेखकों से आप कह सकते हैं जो पैसे के लिए नहीं लिखते, या फिर सिर्फ़ छपास के मारे हुए हैं। सब से नहीं। देवेंद्र कुमार की एक कविता है, ‘ अब तो अपना सूरज भी / आंगन देख कर धूप देने लगा है।’ तो माफ़ कीजिए सुभाष राय जी आप का जनसंदेश भी आंगन देख कर ही भुगतान कर रहा है, यह आप के कलियोगी गणेश भी जानते ही होंगे। तो यह सब बार- बार लिख- लिखा कर अपना मन क्यों खराब करते रहते हैं? आप का प्रबंधन अखबार में साहित्य को इतना स्पेस देने को तैयार है इस संकट के समय में यही बहुत है। हालां कि अगर आप प्रबंधन को यह समझा सकते हैं कि अखबार दो रुपए का करने से ज़्यादा बिक सकता है तो यह भी समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि लेखकों को उन की मज़दूरी भी क्यों न दी जाए? लेकिन लेखक चूंकि सब से कमज़ोर कड़ी है गरीब की लुगाई है सो भौजाई है ही सब की।
एक समय था कि अखबार लेखकों न सिर्फ़ मान देते थे बल्कि ज़्यादातर अखबारों में लेखक ही संपादक भी होते थे। इलाचंद्र जोशी, रामानंद दोषी, गोपाल प्रसाद व्यास से लगायत अज्ञेय, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, कन्हैयालाल नंदन, राजेंद्र अवस्थी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भैरव प्रसाद गुप्त, अमरकांत आदि की एक लंबी सूची है। किस किस का नाम गिनाएं। वह तो जब से संपादक का काम दलाली और लायजनिंग हो गया तो यह परंपरा टूट गई। छूट गया अखबारों से यह साहित्य, संस्कृति आदि का स्पेस। इस की भी कथा बहुत पुरानी नहीं है। हुआ यह कि जब अखबारी सिस्टम भी ग्लोबलाइज़ेशन के हत्थे चढ़ गया तब संपादक नाम की संस्था प्रबंधन के हाथ लाचार हो गई। संपादक नाम की संस्था का क्षरण हो गया। मैनेजर लोग तय करने लगे कि क्या छपेगा और क्या नहीं। यह पेड न्यूज़ का घड़ा जो बीते दिनों फूटा है वह तो बहुत दिनों से चल रहा था। शुरुआत अंगरेजी अखबारों में कामर्स की खबरों से हुई। उन्हीं दिनों क्रिकेट में भी पैसे का ज्वार आया तो क्रिकेट के अपने सचिन तेंदुलकर टाइप लोग भी सक्रिय हो गए। और देखिए न कि सिर्फ़ पैसे के लिए जीने वाले लोग भगवान होने लगे। तो यह सब प्री पेड न्यूज़ का ही चमत्कार था। फ़िल्मों में प्रायोजित खबरों का चटखारा पहले ही से था। सोचिए कि राजेश खन्ना जैसे अभिनेता देवयानी चौबल जैसी पत्रकार को रखैल बना कर रखते थे और अपने मन मुताबिक खबरें प्लांट करवाते थे। ऐसी अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी हैं। बाद के दिनों में तो पी आर एजेंसियों का चलन ही हो गया और खुल्लमखुल्ला। तो इन पी आर एजेंसियों ने ऐड एजेंसियों से फ़िल्मी पन्ने बनवा कर अखबारों को प्रायोजित करना शुरु किया। धीरे-धीरे आग फैल गई। सभी अखबार इस आग की चपेट में आ गए। संपादक जो बिठाए गए थे इन अखबारों में प्रबंधन की हां में मिलाते रहे। टी.वी धारावाहिकों के प्रायोजित पन्ने भी अखबारों पर धावा बोल बैठे। अब नंगी अधनंगी औरतों की फ़ोटो आम हो गई हर अखबार में। अब साहित्य कौन सी चिडिया थी, कौन सी गौरैया थी जो इन अधनंगी फ़ोटुओं में फ़ुदकने की हिमाकत करती भला? प्राण ले लिए अखबारों ने इस गौरैया के, इस चिडिया के। अब देखिए न कोई फ़िल्म रिलीज़ होती है तो फ़ौरन सभी चैनलों पर उन के प्रमोशन कार्यक्रम के तहत सारे हीरो हिरोइन बैठ जाते हैं। एक से एक बकवास फ़िल्में करोड़ों रुपए बटोर कर चंपत हो जाती हैं।
राजनीति में भी अमर सिंह और राजीव शुक्ला जैसे लोगों की आमद हो गई। तो इन लोगों ने नमक में दाल की रवायत राजनीतिक खबरों में भी चला दी। कि एक ग्राम सच में कुंटल भर का गप्प। इसे प्रायोजित खबर का नाम दिया गया। धीरे-धीरे इसे पेड न्यूज़ का नाम दे दिया। खास कर चुनावी दिनों में। कुछ अखबार तो रेट कार्ड छाप कर घूमने लगे। अब खुला खेल फरुखाबादी हो गया तो भांडा फूट गया। प्रभाश जोशी जैसे लोग खडे़ हो गए। इस पेड न्यूज़ के खिलाफ। अब काटजू ही क्या जिस को देखिए वही पेड न्यूज़ के नाम पर शुरु हो जाता है। अब काटजू की हिप्पोक्रेसी देखिए कि पेड न्यूज़ जिस की नींव इतनी पक्की हो गई है कोई अभी हाल फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकता पर उस पर वह बोल रहे हैं। लेकिन मजीठिया वेज बोर्ड को सभी अखबार मालिक धता बताए बैठे हैं, उस पर वह सांस नहीं ले रहे। चाहिए तो उन को यह कि मजीठिया वेज बोर्ड को ले कर हल्ला बोल दें। पर नहीं पेड न्यूज़ की फटी ढोलक बजाना उन्हें ज़्यादा मुफ़ीद लग रहा है। क्यों कि इस में मालिकों से सीधे उन्हें टकराना नहीं पडे़गा। तो पेड न्यूज़ की प्याज खा रहे हैं फ़िलहाल। नहीं मुझे याद है कि जब पहले पालेकर और फिर बाद में बछावत लगा था तो कोशिश यही थी कि एक सब एडिटर का वेतन कम से कम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बराबर तो हो ही। पर अब क्या है? एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक भी पहली तनख्वाह बीस हज़ार रुपए की पाता है। विश्वविद्यालयों में तो लोग लाखों का वेतन पाने लगे हैं। पर दिल्ली जैसी जगह में बडे -बडे अखबारों में लोग पांच -पांच हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं। लखनऊ में तो दो-दो हज़ार रुपए में। सोचिए कि आज की तारीख में मनरेगा में काम करने वाला मज़दूर भी इस से ज़्यादा ही कमा लेता है, वह भी अपने गांव घर में बैठ कर ही। एक रिक्शा वाला भी इस से ज़्यादा कमा लेता है। काटजू साह्ब इस पांच हज़ार या दो हज़ार की पगार पाने वाले से आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वह अर्थशास्त्र और इतिहास भी जाने ही जाने। हां एक से एक स्वनामधन्य भी हैं जो लाखों रुपए महीने की पगार पा रहे हैं। और कि मीडिया को बरबाद कर रहे हैं। हालां कि एक समय था कि डेढ, दो सौ या ढाई सौ रुपए पा कर भी वह पत्रकार सिर पर स्वाभिमान टांगे घूमते थे और सेठों की नौकरियों को जब चाहते थे लात मार कर निकल जाते थे। नौकरी की खाक परवाह नहीं करते थे। और वह लोग अर्थशास्त्र या इतिहास ही नहीं और भी बहुत कुछ जानते थे। अपने अपने फ़ील्ड के टापर लोग थे। पर आज एक से एक चश्मे नूर हैं कि साक्षर होने के बूते ही लाखों की सेलरी पा कर भी स्वाभिमान किस चिडिया का नाम है जानते ही नहीं। और काटजू साहब हैं कि उन से अर्थशास्त्र और इतिहास भी जान लेना चाहते हैं। यहां तो एक से एक रणबांकुरे हैं कि बीच क्रिकेट मैच में मैन आफ़ द मैच की फ़ोटो मांग बैठते हैं फ़ोटोग्राफ़र से और ग्रुप एडीटर की कुर्सी पर शोभायमान हो जाते हैं। यह समस्या अपनी हिंदी में ही कुछ क्या बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में हमारे सुभाष राय लेखकों को पैसा न दे पाने के दुख में मरे जा रहे हैं। तब जब एक से एक स्वनामधन्य संपादक हैं कि अपनी तनख्वाह बढ़वाने के चक्कर में चार छह लोगों को नौकरी से ऐसे निकलवा देते हैं गोया देह से चिल्लर निकलवा रहे हों।
अब यह घटतौली भी कैसे जाए भला? वह भी हिंदी से? यह सब तब है जब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भले न हो बाज़ार की सब से बड़ी भाषा है इस दुनिया में। हिंदी से ज़्यादा न सिनेमा बनता है, न धारावाहिक, न अखबार हैं हिंदी से ज़्यादा, न हिंदी से ज़्यादा किताबें छपती हैं इस देश में न हिंदी से ज़्यादा खुदरा बाज़ार है यहां। फिर भी हिंदी का लेखक रायल्टी नहीं पाता। गिनती के कुछ लोग पाते भी हैं तो कैसे और कितना पाते हैं, वह ही जानते हैं। सच यह है कि पाठ्यक्रम जो न हो हिंदी का तो रायल्टी शब्द भी हिंदी किताबों की दुनिया से उठ जाए। हिंदी फ़िल्मों के पटकथा और संवाद लेखकों की हैसियत कुछ बहुत अच्छी नहीं है। हिंदी पत्रकारों की तो और बुरी गत है। देश के किसानों के लिए सरकार कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो घोषित करती है, हिंदी के पत्रकारों को तो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। एक रिक्शे वाले से भी कम वेतन है उस का। और बहुत सारे संवाद सूत्रों को तो वेतन भी नहीं मिलता। मुफ़्त में काम करते हैं। और अब यह नई मार है हिंदी अखबारों में लिखने वाले लोगों पर कि ऐलानिया उन से यह अपील कर दी जा रही है कि आप बिना पैसे के लिखें! हद है सुभाष राय जी, यह क्या कर दिया आप ने? तमाम पत्रिकाएं और अखबार लेखकों को पैसा नहीं देते, ये तमाम ब्लागर या साइटें भी किसी को एक पैसा नहीं देते। हां, पाठक संसार देते हैं। लेखक पैसे के लिए लिखते भी नहीं पर वह अखबार या पत्रिका या साइटें ऐलान कर के नहीं कहते कि हम पैसा नहीं दे पा रहे। पर आप ऐलान कर के कह रहे हैं। बार -बार कह रहे हैं। क्या जनसंदेश टाइम्स का प्रबंधन हंस से भी गया गुज़रा है? हंस एक तरह से एकल प्रयास है। व्यावसायिक नहीं है। राजेंद्र यादव २५ बरस से भी ज़्यादा समय से इसे अकेले अपने बूते निकाल रहे हैं। और बताते हुए अच्छा लगता है कि वह अपने रचनाकारों को किसी भी अखबार से खराब पारिश्रमिक नहीं देते। लिखते ज़रुर हैं चिट्ठी में कि यह पारिश्रमिक नहीं है, बस यूं ही है। आप खर्च समझ लें। तो हंस क्या सहित्यिक स्पेस नहीं देता? हां पर लेखकों के साथ घटतौली नहीं करता।