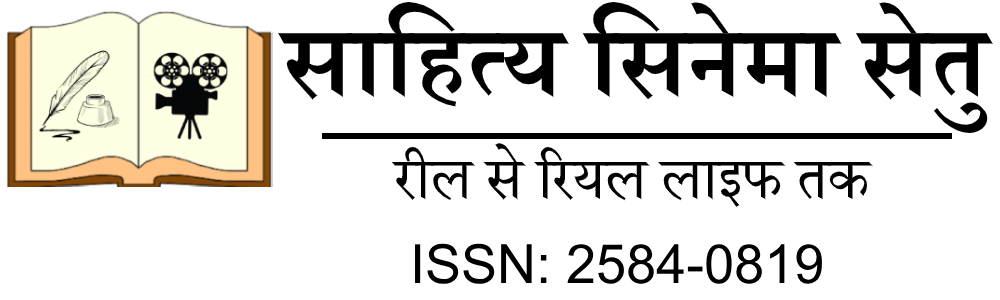स्त्री-भागीदारी को लेकर हमेशा उदासीन रहा हिंदी सिनेमा अब जागरूक हो चुका है। निःसंदेह यह जागरूकता फिल्म उद्योग की खुद की नहीं है बल्कि महिलाओं द्वारा किए खुद में परिवर्तनों के आधार पर आई है। ऐसा भी नहीं कि स्त्रियाँ पहले सशक्त और प्रतिभाशाली नहीं थीं, बस किनारे खड़ी अपनी पारी के इंतजार में थी, जल्द ही उन्हें पता चल गया कि लाइन में खड़े होकर कभी मौका नहीं मिलेगा लिहाजा वह भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़ने पर विवश हुई, ठीक वैसे ही जैसे लड़के करते आ रहें हैं वर्षों से। सिनेमा के इतिहास को पलट कर देखें तो इन सौ वर्षों के लंबे समय में आवश्यक प्रस्थान बिंदु होते हुए भी स्त्रियाँ हमेशा हाशिए पर रहीं। वजह यही है कि पुरुषों ने उन्हें हमेशा कमजोर समझा। उनकी कार्यक्षमता को कम आँका गया।
ऐसा भी नहीं है कि हिंदी में स्त्री-समस्या केंद्रित फिल्मों का निर्माण हुआ ही नहीं। दरअसल अधिकतर हिंदी फिल्मों में स्त्री को आदर्शवादी और ममतामयी माँ, बहन, भाभी, पुत्री, पत्नी और प्रेमिका के रूप में ही अधिक चित्रित किया जाता रहा है जो विद्रोह भी करती है तो क्षण भर के लिए। भावना या विरोध के कारण अंततः समर्पण ही करती आई है। सवाक फिल्मों आरंभिक दौर से लगभग 1980 तक ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जिसमे स्त्री अपने अधिकारों और अस्मिता के लिए तनकर खड़ी तो होती है परंतु जल्द ही अपने सामाजिक बंधनों कि जकड़न में आ जाती है। ऐसी फिल्मों में – चित्रलेखा, महल, दहेज, बिरज बहू, मदर इंडिया, सुजाता, मैं चुप रहूँगी, बंदिनी, काजल, ममता, साहब बीबी और गुलाम, पाकीजा, परिणीता, गुड्डी, आँधी, जूली, मौसम, राम तेरी गंगा मैली, तवायफ, निकाह, उमराव जान, अभिमान आदि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1980 के बाद जरूर स्त्री-चेतना से लैस फिल्मों का निर्माण आरंभ हुआ जिसमें बहुत भूमिका निभाई – ‘समानांतर सिनेमा’ ने। समानांतर सिनेमा ने स्त्री कि उन्मुक्त भावनाओं को नया आसमान दे दिया जिसमे विचरण कर उन्हे अपनी आजादी के नए रंग दिखने शुरू हुए, अपने अधिकारों की नई सूची उनके हाथ लग गई। ऐसी फिल्मों में – मंडी, बाजार, भूमिका, मिर्च मसाला, महायात्रा, इजाजत, प्रतिघात, रिहाई आदि। 1990 के बाद का हिंदी सिनेमा भूमंडलीकरण और उदारीकरण के प्रभाव से तेजी से बदला है। नए निर्देशकों ने अपनी नई विचारधाराओं के द्वारा हिंदी सिनेमा को तमाम सहित्यिक विमर्शों से जोड़ दिया। हिंदी सिनेमा और साहित्य में एक सामंजस्य स्थापित हुआ है। स्त्री विमर्श को हिंदी सिनेमा में हमेशा ही स्पेस मिलता रहा है। ‘दिशा’, ‘तर्पण’, ‘बवंडर’, ‘गॉड मदर’, ‘वाटर’, ‘फायर’, ‘अर्थ’, ‘कामसूत्र’ ‘मातृभूमि’ ‘सत्ता’, ‘चमेली’, ‘अस्तित्व’, ‘जुबैदा’, ‘चाँदनी बार’, ‘फैशन’, ‘हीरोईन’ , ‘नो वन किल्ड जेसिका’, ‘इश्किया जैसी फिल्मों ने स्त्री विमर्श को नया आयाम दिया है। इतना ही नहीं इन फिल्मों में स्त्री की बदलती छवि को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है।
वर्ष 2014 को स्त्री-सिनेमा के विकास में विशेष रूप से इसलिए रेखांकित करने का मन होता है क्योंकि इस वर्ष लगभग एक दर्जन ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जिसने स्त्री छवि को पूरी तरह बदल दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब हमने हिंदी सिनेमा में स्त्री के उस रूप को बड़े स्तर पर देखा गया जिस रूप को वह वर्षों से अंदर-अंदर जी रही थी। उनकी तमाम दमित भावनाओं को कई रूपों में देखने के लिहाज से यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष प्रदर्शित फिल्मों के नामों पर जरा गौर फरमाएँ – ‘डेढ़ इश्किया’, ‘हाईवे’, ‘गुलाब गैंग’, ‘क्वीन’, ‘कांची’, ‘रिवाल्वर रानी’, ‘मरदानी’ ‘हैदर’, ‘लक्ष्मी’, ‘अनुराधा’, ‘सुपर नानी’, ‘रंगरसिया’, ‘मेरीकाम’। ये तो उन फिल्मों की सूची है जिसमे स्त्री जीवन के उत्कर्ष का उत्सव है। अभी कई ऐसी फिल्में भी हैं – जिनमे हैं तो स्त्री मुक्ति के स्वर लेकिन उनकी प्राथमिकता पैसा कामना मात्र है – ऐसी फिल्मों में आप बिपाशा बसु, सनी लियोन, पूनम पांडे, नीतू चंद्रा, शर्लिन चोपड़ा जैसी कुछ अधिक उन्मुक्त नायिकाओं की फिल्मों को शुमार कर सकते हैं।
2014 में प्रदर्शित फिल्मों पर गौर फरमाएँ तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि इस वर्ष जिन स्त्री केंद्रित फिल्मों का निर्माण हुआ उसके केंद्र किसी दबाई, सताई और घबराई स्त्री का चेहरा नहीं है बल्कि पुरुषों को चुनौती देती उस स्त्री का अक्स है जिसमें अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली है। वर्ष के आरंभ में ही आई निर्माता विशाल भारद्वाज निर्देशक अभिषेक चौबे की ‘डेढ़ इश्किया’। जो लोग इसका पहले हिस्सा ‘इश्किया’ देख चुके होंगे उन्हें जरूर अंदाजा हो गया होगा कि स्त्री किस हद तक शातिर हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या शातिर होना या स्त्रियों को भोगने का पास सिर्फ पुरुषों के पास ही है? उत्तर होगा नहीं। क्योंकि ‘डेढ़ इश्किया’ एक ऐसे ही औरत की कहानी है जिसे अपनी ताकत और मजबूती दोनों का गहन अंदाजा है। जिस यौनिकता को पुरुषों ने हमेशा पर्दे के अंदर भोगा उसी को ढाल बना कर ‘डेढ़ इश्किया’ की नायिका ने खुलेआम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया किया। प्रेम के नाम पर संभोग के लोलुप चाचा-भतीजों की बाट लगा दी।

डेढ़ इश्किया
‘डेढ़ इश्किया’ एक नहीं तीन महिलाओं की कहानी है। माधुरी और हुमा कुरैशी ने पर्दे पर जिस चरित्र को जिया है वह साधारण स्त्री की कहानी नहीं है पर उनकी इच्छाओं से परे भी नहीं है। माधुरी दीक्षित और हुमा कुरैशी ने पूरी फिल्म में उन्मुक्त होती स्त्री के जीवन के तमाम पहलुओं बहुत ही बखूबी से चित्रित किया है। विवाह – निकाह के लिए अभी तक स्त्री को ही पुरुष की मानसिकता पर खरा उतरने की पाबंदी थी पर यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ माधुरी दीक्षित ने एक ऐसी स्त्री की भूमिका को जीवंत किया है जो अपने जीवन के अकेलेपन को तोड़ने के किसी मर्द के कंधों का सहारा आसानी से नहीं ले लेती बल्कि बाकायदा स्वयंबर रचाती है। जिसमें सैकड़ों छोटे-बड़े हैसियत के मर्द शामिल होते हैं। इन मर्दों का एक स्त्री को मात्र लेने के लिए अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखाने के संघर्ष करते देख सुखद अनुभूति होती है। ‘डेढ़ इश्किया’ पूरी तरह से सेक्स और इश्क में आकंठ डूबी फिल्म है जिसके केंद्र में स्त्री है। हालाँकि भाषा और संगीत की कठिन बुनावट कहीं-कहीं बोर भी करती है पर यह सिनेमा का दूसरा पक्ष है। स्त्री अस्मिता की दृष्टि से यह एक नए स्वाद की फिल्म है।

हाइवे
‘डेढ़ इश्किया’ के कुछ दिन बाद ही इम्तियाज अली की ‘हाईवे’ प्रदर्शित हुई जिसकी चर्चा उसके विषय वस्तु को लेकर कम और अलिया भट्ट के अभिनय को लेकर अधिक हुई। ‘हाइवे’ एक तरह से हमारे ही घर की कहानी है, उस हर घर की कहानी है जिस घर में स्त्रियों को अन्याय सहते देखा जाता है और उसकी वेदना को महसूस भी किया जाता है लेकिन समाज के तिरस्कार के दर चुप करवा दिया जाता है।
‘हाइवे’ हमें हमारे घर के अंदर झाँकने का मौका देती है। अपने घर में आने वाले रिश्तेदारों, संगी-साथियों और पड़ोसियों, जो हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं पर नजर रखना सिखाती है। अलिया भट्ट ने अपने घर में यौन शोषण की शिकार लड़की के चरित्र को जिस मासूमियत और गंभीरता से जिया है वह उनके वर्तमान फिल्मी जीवन का सर्वोत्तम अभिनय तो है संभव है फिर दुबारा उन्हे ऐसा चरित्र न मिले। इम्तियाज अली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह अपने स्त्री-पात्रों को उन्मुक्त होने का पूरा अवसर देते हैं। उसकी भावनाओं को बाँधते नहीं हैं। एक चीज और ‘प्रेम’ उनके यहाँ मात्र भोगने कि वस्तु नहीं, पर बंधन भी नहीं है। ‘लव-आजकल’ की नायिका पहले प्रेम करती नहीं, करती है तो टूटने पर खुद नहीं टूटती बल्कि बाकायदा ‘ब्रेक-अप पार्टी’ मनाती है। यह दृश्य चाहे भले ही बहुत सादगी से प्रस्तुत किया गया परंतु नेपथ्य में संदेश यही है कि लड़कियाँ ब्रेक-अप पर अब यह नहीं सोचती कि ‘अब मेरा क्या होगा’ बल्कि उन्हें पता है उनके पास भी अब विकल्प की कमी नहीं है। अगर लड़के नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं तो लड़कियों को कौन सा श्राप मिला हुआ है। ‘रॉक स्टार’ भी पहले खुलती नहीं और जब खुलती है तो कहती है – ‘मिलकर खूब गंध मचाएँगे’। हिंदी सिनेमा के पूरे अध्याय को कायदे से पढ़ा जाए तो साफ पता चल जाएगा कि ‘गंध’ मचाने की सारी क्रियाएँ सिर्फ नायकों के लिए विकसित की गई हैं। इम्तियाज अली उसे खींचकर नायिकाओं के हिस्से में भी लाते हैं। ‘हाइवे’ एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके हिस्से की खुशी सामाजिक बंधनों में फँसी हुई है। अपने ही घर में बाधक बनी एक लड़की जो मानसिक रूप से मुक्त होना चाहती है और दैहिक रूप से भी। यह कितनी बड़ी बिडंबना है अपने अपहरण हो जाने से वह खुश है अपहरण करने वाले के पास खुद को ज्यादा सेफ महसूसू करती है क्योंकि यहाँ वह ज्यादा उन्मुक्त है। इम्तियाज अली ने एक ऐसी लड़की की कहानी को पर्दे पर बुना है जो हमारे ही आस-पास रहती है पर हमें दिखती नहीं है और दिखती है तो चुप रहने की सलाह देते हैं। तमाम तनाव और अवरोधों के बीच स्त्री जीवन के लिए मुक्ति के नए सूत्र प्रस्तुत कर देने में इम्तियाज माहिर हैं।

गुलाब गैंग
‘हाइवे’ के ठीक बाद प्रदर्शित ‘गुलाब गैंग’ विवादित और कमर्शियल फिल्म की तरह याद की जा सकती है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ कि मुझे फिल्म की कहानी और उसकी प्रस्तुति से अधिक मतलब इस बात से है कि वह फिल्म स्त्री-जीवन के किस पक्ष को कितने सही तरीके से प्रस्तुत कर सकी है ‘गुलाब गैंग’ के बारे में सभी को पता है कि वह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है इसलिए उसके प्रदर्शन के साथ ही उसे उसकी मूल घटना से हूबहू जोड़कर देखना लाजिमी भी है पर हम मान लें कि हम फिल्म देख रहे हैं जिसका एक पक्ष व्यवसायिक भी है तो गैर जरूरी भी है।घटना को छोडकर सिर्फ फिल्म के लिहाज से देखें तो यह याद नहीं आता कि पिछली किस फिल्म में एक झुंड में, एक रंग में लिपटी खड़ी 8-10 औरतों को एक साथ 12-15 गुंडों को पीटते दिखाया गया हो। हिंदी सिनेमा में स्त्री की इज्जत बचाकर कई गुंडों को एक साथ पीट-पीटकर वाहवाही लुटने और तालियाँ बजवाने का यह श्रेय सिर्फ नायकों को जाता रहा है, पर याद रखें यह दौर स्त्री जीवन के सिर्फ ऊपरी हिस्से को देखकर मादक होने या उनसे बिस्तर तक ले जाने का कुत्सित विचार मन में लाने भर का का नहीं है। बिना उनकी स्वीकृति के गलती से भी ऐसा विचार आया तो तो गुलाबी रंग में रँगी यह स्त्रियाँ आपको नपुंसक बना देने में ज्यादा समय नहीं लेंगी। ‘गुलाब गैंग’ की नायिका माधुरी दीक्षित हैं जो इस तरह की भूमिकाओं में पारंगत हैं। जिन्होंने उनकी बेटा, लज्जा, मृत्यदंड, अंजाम और आजा नचले आदि फिल्में देखीं होंगी उन्हे आभास हो गया होगा कि यह फिल्म माधुरी के माध्यम से चेतनशील और विद्रोही होती स्त्री की गजब की प्रस्तुति है। इस फिल्म में यह बखूबी दिखाया गया है कि स्त्रियाँ पहले प्यार से अपना हक माँगती है। प्यार से मिलता है अपना आप पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देती हैं। नहीं मिलता तो देख लीजिए साहब वह विद्रोह करना सीख गई हैं। घर से उठाकर लाएँगी और आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगी। अगर आपने फिर भी बत्तमीजी कि तो बीच बाजार, गाँव, कस्बा, जहाँ भी उन्हें मौका मिलेगा आपको नंगा कर देंगी। ‘गुलाब गैंग’ देखते हुए यह भी महसूस होता है कि स्त्री सह ले तो घर में भी शोषित होती है और अगर विद्रोह कर लें तो गाँव के प्रधान से लेकर शहर के मंत्री तक उसके चौखट पे आकर झुक जाएँ। अपने हक को लाठी-डंडों के बल पर हथियाने निकली ‘गुलाब गैंग’ की ये स्त्रियाँ आपको चकित और अविश्वसनीय लग सकती हैं पर दिल पे हाथ रख कर कहिए कि क्या आप नहीं चाहते कि कोई आपकी माँ, बहन, बेटी, बहू और पत्नी के साथ खिलवाड़ करे तो वे भी इन्हीं कि तरह तन कर खड़ी हो जाएँ? और दे दें चुनौती इस सड़ी गली व्यवस्था को जिसकी चित-पट दोनों पुरुषों की है।

क्वीन
‘क्वीन’ का प्रदर्शन यह चिह्नित करता है कि महिलाओं के जीवन का एकमात्र उद्देश्य मात्र पति-परमेश्वर नहीं है बल्कि उसकी अपनी इच्छाएँ भी हैं। ‘क्वीन’ की नायिका साधारण सी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है। वह हनीमून मनाने के सपने सजाती-सकुचती और पर लगाकर उड़ जाने को आतुर है। उसकी भावना हर उस मध्यमवर्गीय लड़की की भावना है जिनका मकसद चाँद को छूने का नहीं होता बल्कि जो होता है उसी में खुश रहने का होता है। वह महत्वाकांक्षी नहीं होती पर स्वाभिमान को डगमगाने नहीं देती। इस फिल्म की नायिका अपने शादी को लेकर उत्साहित है और जब शादी का सपना पूरा नहीं होता तो वह अपना दूसरा सपना तोड़ने को राजी नहीं होती। खुद अकेले निकल जाती है हनीमून मनाने। दरअसल यह एक ऐसी मासूम और भावनात्मक लड़की की कहानी भी है जो सिनेमा के प्रचलित शब्दों में ‘देशी’ है और जिससे उसकी शादी होने वाली है उसका स्वाद बिगड़ चुका है क्योंकि वह योरोप में रहता है। एक झटके से टूटे सपने को आँसू पोछकर झटके से खड़ी हुई लड़की के चरित्र को कंगना राणावत ने जी लिया है। इस फिल्म से उनकी ग्लैमरस और उबाऊ छवि का अंत भी हो जाता है वह एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में चिह्नित हो जाती जाती हैं। भारत का सामाजिक ढाँचा इस तरह का है लड़कियाँ न घर के बाहर सुरक्षित हैं न तो घर में हैं। ‘क्वीन’ की नायिका तो अपने जीवन की शुरुआत योरोप में शुरू करती है। फिर वहाँ शुरू होता है स्त्री-संघर्ष का नया अध्याय। एक ऐसी लड़की जो पूरी तरह से भारतीय परिपाटी में रची बसी है उसका अचानक विदेश में जाकर नया जीवन शुरू करना थोड़ा चकित करता है परंतु सिनेमा की एक ताकत यह भी है कि वह हमेशा वर्तमान नहीं दिखाता कभी-कभी भविष्य के लिए सचेत करके रास्ते भी खोलता है।
‘क्वीन’ की नायिका की विदेशी यात्रा तमाम मुश्किलें पैदा करता है पर वह बहुत आसानी से उन्हे अपना कवच बना लेती है। मुश्किलों को अपने अनुभवों में तब्दील कर लेती है। कोई भी देश हो, समाज हो, संगठन हो उससे सब लोग निष्ठुर नहीं होते। कुछ लोग प्रेमी भी होते हैं। नायिका तमाम संघर्षों और समस्याओं से जूझती हुई आत्मविश्वासी हो रही है, कुछ अच्छे दोस्त भी बनते हैं और जब वह इस दुनिया के तौर-तरीके सीख कर जीना सीख जाती है तो उसे लगता है जहाँ खुशी मिले उससे बेहतर जगह कोई नहीं होती। तमाम हिंदी मसाला फिल्मों की तरह नायिका को बदला हुआ देख नायक का हृदय परिवर्तन भी इस फिल्म में होता है परंतु लड़की ‘क्वीन’ है वह अपने ठुकराए जाने का एहसास बहुत अंदर तक महसूस कर चुकी है लिहाजा शादी से मना कर देती है। आम हिंदी फिल्मों की तरह ‘क्वीन’ का समापन नहीं होता। एक दशक पहले यह फिल्म चकित कर सकती थी पर आज खुशी देती है। नेपथ्य में जाकर देखें तो ‘क्वीन’ फिल्म यह भी सिखाती है की लड़कियों की दुनिया को सिर्फ घर की दीवारों में कैद करना गुनाह है। उन्हे घर से निकलने का मौका मिले तो वे कुछ बेहतर विकल्प खुद ला सकती है।

रिवाल्वर रानी
‘रिवाल्वर रानी’ कंगना राणावत की एक कमजोर फिल्म ही सही पर स्त्री-स्वर से भरी हुई है। हिंदी फिल्मों मे टपोरी गुंडे की भूमिका आज तक नायक ही करते आए हैं, पर सिनेमा बदल रहा है। अभिनय की परिपाटी बादल रही है। कंगना ने ‘रिवाल्वर रानी’ में जिस भूमिका को जिया है उसका उद्देश्य मात्र व्यवसायिकता का चरम है परंतु कंगना ने हाथ में पिस्तौल और आँखों में अपने सामने बच्चे दिखते नायक से प्यार भरकर प्यार का इजहार करती है तो वह उन लड़कियों की कहानी है जो मजबूरी में हथियार उठाती तो हैं पर प्यार मिलते ही पिघल जाती है। पूर्ण रूप से व्यावसायिक पर स्त्री जीवन के छूट गए पक्ष को देखने लिए ठीक ठाक फिल्म है।

मरदानी
‘मरदानी’ को ‘रिवाल्वर रानी’ के अगली कड़ी के रूप मे याद किया जा सकता है यहाँ भी नायिका के हाथ में पिस्तौल है, पर कानूनी है। इस रिवाल्वर से होने वाले कत्ल गैर-कानूनी नहीं होंगे क्योंकि उसके पास लाइसेंस है। दोनों ही नायिकाओं का मुख्य स्वर गुनाह खत्म करना है पर तरीका अलग है। एक कानूनी ढंग से तो दूसरी कानून को हाथ में लेकर। जो कानून को हाथ में लेकर काम करती है उसका भरोसा कानून से उठ चुका है क्योंकि उसका मानना है कानून सही होता हो वह बंदूक ही क्यूँ उठाती। दूसरी कानून को मानने पर बाध्य है क्योंकि वह उसकी नौकरी करती है और उसका उसमें विश्वास भी है। रानी मुखर्जी प्रतिभावान अभिनेत्री हैं पर फिल्मों में उनकी क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं हो सका। यह हिंदी सिनेमा है जहाँ स्त्रियाँ जल्द ही रिटायर्ड हो जाती है। अपनी असफलता से घबराई रानी कई तरह की भूमिका में एक्सपेरिमेंट करने के बाद थक कर ‘मरदानी’ बनी। ‘मरदानी’ उनके घोषित पति आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित फिल्म है जिसका उद्देश्य रानी की पुनर्स्थापना है। लेकिन फिल्म औसत रही पर रानी को चर्चा मिलनी थी मिली। रानी मुखर्जी को इस भूमिका में देखकर बराबर ‘तेजस्वनी’, ‘फूल बने अंगारे’ जैसी कुछ फिल्मों की याद आना लाजिमी है। स्त्री-अस्मिता के बदलते तेवर की दृष्टि से यह एक जरूरी फिल्म हो सकती है।
इस साल के मध्य में कांची, अनुराधा, सुपर नानी जैसी स्त्री केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। हालाँकि यह फिल्में स्त्री अस्मिता को मजबूत करने में किसी बड़ी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पातीं बावजूद उनका महत्व इस मायने में है कि इन फिल्मों में स्त्री जीवन के कुछ ऐसे पक्षों को भी देखने का अवसर मिलता है जो हमें हिंदी फिल्मों में तो जल्दी नहीं ही दिखता है।
कांची
‘कांची’ के द्वारा सुभाष घई ने एक बार फिर से एक स्त्री की बदले की भावना को आधार बनाकर बड़े लेबल का मैलोड्रामा रचा लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। परंतु थोड़ा स्त्रीवादी होने की छूट लेते हुए कहूँ तो एक स्त्री का अपने साथ हुए अन्याय के लिए लड़ते हुए बदला लेना अच्छा लगा। पुरुषवादी समाज में एक लड़की का संघर्ष देख आकर्षित हुई।
अनुराधा
‘अनुराधा’- जैसा कि नाम से लग जाता है कि यह एक सीधी साधी लड़की कहानी है, जो संस्कार से लबरेज और परिवार की आदर्श लड़की है। अपने ससुराल की जिम्मेदार बहू है, पतिव्रता पत्नी है। उसका संस्कारी और अदर्शवादी होना ही उसके लिए घातक है। उसके सीधेपन को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। पूरी फिल्म की कहानी यही है कि एक स्त्री अगर हर तरह से अपने आप को समाज में फिक्स भी कर ले तो उसके शोषण की कहानी का अंत नहीं हो जाता है। ठीक-ठाक, औसत दर्जे से थोड़ी कम लेकिन स्त्री मनोविज्ञान और उससे साथ बर्ताव करने समाज के मनोविज्ञान को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण फिल्म है।
लक्ष्मी
‘अनुराधा’ के लगभग साथ ही नागेश कुकनूर ने एक बहुत ही उम्दा फिल्म का निर्माण किया – ‘लक्ष्मी’। नागेश कुकनूर समकालीन हिंदी सिनेमा के ऊर्जावान युवा निर्देशक हैं। अर्थपूर्ण स्त्री जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं उन्होने बहुत ही बेहतरीन और अर्थपूर्ण फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत उसकी सादगी है। वह कभी भी बड़ी बात कहने के लिए फिल्म को गंभीर नहीं बनाते। उनकी फिल्में ‘डोर’, ‘मोड़’ और आशाएँ स्त्री-अस्मिता को रेखांकित करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म के रूप में हमेशा याद की जाएँगी। वह उलझी हुई कहानी को बहुत आसानी से सुलझाते हैं।
‘लक्ष्मी’ की कहानी बाल वेश्यावृत्ति पर आधारित है। ये फिल्म तमाम समारोहों और फिल्म प्रदर्शनों में सम्मानित और पुरस्कृत हुई। इस फिल्म की मूल कथा में बाल वेश्यावृत्ति तो है लेकिन उसके बहाने पूरे भारतीय समाज धर्म की आड़ में की जा रही जिस्म-फरोसी को दिखाने की कोशिश की गई है। हालाँकि ये फिल्म उन्ही द्वारा स्त्री-समस्या को लेकर बनाई गई ‘डोर’ की संवेदना को छू भी नहीं पाती। बेहतरीन निर्देशन होते हुए भी विषय-वस्तु की कमजोर प्रस्तुति फिल्म को उस वेदना से नहीं जोड़ पाती जिसके उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है। जहाँ रेड्डी नाम का एक व्यक्ति जो ‘धर्मविलास’ नाम की संस्था के आड़ में मजबूर और कम उम्र की लड़कियों का धंधा करता है। उसी के जाल में अनजाने में लक्ष्मी भी फँस जाती है। पूरी कहानी में लक्ष्मी को रेड्डी जैसे कुत्सित देह व्यापारी से संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। पैसे के बल पर बह कई बार लक्ष्मी को बेईज्जत भी करता-करवाता है परंतु वह हारती नहीं, लड़ती है और अपना हक प्राप्त करती है। इस पूरी कहानी में एक ऐसी लड़की की कहानी को देखा जा सकता है जो छोटी सी उम्र में शासन, प्रशासन और समाज के कुकर्मियों से टकराती है। यह कहानी मात्र लक्ष्मी की नहीं है उसके बहाने उन लाखों लड़कियों की है जो रेड्डी जैसे जिस्म बेचकर ऐश करने वाले सेठों के जाल में हैं और दुर्भाग्य यह है कि जब वह लड़कियाँ साहस करके कोर्ट-कचहरी तक न्याय पाने पहुँचती हैं तो वहाँ उनका मजाक बनाया जाता है। इस फिल्म के बहाने नागेश ने पूरी व्यवस्था में व्याप्त दलाली और घूसखोरी की परत उधेड़ने की मजबूत कोशिश की है। अच्छी विषय-वस्तु पर एक कमजोर प्रस्तुति होते हुए भी ‘लक्ष्मी’ जैसी लड़कियों की समस्या से हम अवगत होते हैं और बहुत नजदीक से महसूसते हैं यही इस फिल्म की संवेदना है। स्त्री-अस्मिता के बिंदुओं से खड़े होकर देखें तो ‘लक्ष्मी’ मजबूत और ऊर्जावान फिल्म है।
सुपर नानी
‘सुपर नानी’ एक स्त्री के त्याग और पारिवारिक समता को बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं की बलि देने वाली स्त्री की कहानी है। ममतामयी स्त्री के कठोर बन जाने के चरित्र को रेखा ने बखूबी अदा किया है। फिल्म की कहानी आम भारतीय नारी की है जिसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपना परिवार है। परिवार मतलब पति, बच्चे और अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी। परिवार की वरिष्ठ सदस्य होकर भी उपेक्षित नारी का जीवन जी रही भारती भाटिया (रेखा) का पूरा जीवन अपने घर-परिवार को सँभालने में गुजर जाता है, यह ठीक है कि एक पारिवारिक नारी कि अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिन्हें वह निभाती भी है पर यहाँ समस्या दूसरी है। यहाँ एक स्त्री के अपने परिवार के लिए मर-खप जाने कि कहानी भर नहीं है, न ये फिल्म का मुद्दा है बल्कि मुद्दा यह है कि इतना शारीरिक, मानसिक और आर्थिक बलि देने के बाद भी स्त्री का सम्मान क्यूँ नहीं हैं? सवाल सम्मान का है? दिन भर घर में सबकी इच्छाओं कि पूर्ति करती नानी को जब उसका नाती अचानक उससे मिलने आता है तो वह उसकी इस उपेक्षा से दुखी होकर उसके अंदर छुपे रूप-गुण को निखरता है और एक दिन उन्हें प्रोत्साहित करता है तो वह जिस साबुन का वह प्रयोग करती हैं उसी की ब्रांड अंबेसडर बन जाती हैं। यह करिश्मा होते ही नानी की वैल्यू बढ़ जाती है। समाज में सम्मान मिलते ही वह परिवार की हीरोइन बन जाती हैं। सामान्य सी इस फिल्म का महत्व इसलिए है कि यह फिल्म ये संदेश देने में सफल हो जाती है कि स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता ही उसे सम्मान दिला सकती है। स्त्री सिर्फ परिवार के लिए किचेन में पूरी अपनी जिंदगी गुजार दे तो वह मात्र सहानुभूति पा सकती है पर उसकी आर्थिक स्थिति ही उसे हर तरह से मजबूत कर सकती है। फिल्म की कहानी में यह भी छुपा है कि किसी भी उम्र में किसी भी क्षेत्र में नई शुरुआत की जा सकती है बस आपकी स्वयं की इच्छा हो। उम्र खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। वैसे तो पूरे साल लगभग 30-35 ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ जिन्होने हिंदी सिनेमा की लीक को तोड़ते हुए हमें नए सिनेमा से परिचित करवाया है, जिस पर एक विस्तृत लेख लिखने का विचार है। स्त्री जीवन की उपलब्धियों और चुनौतियों की दृष्टि से देखें तो इस साल के दूसरी छमाही में ‘हैदर’, ‘मेरीकाम’ और ‘रंगरसिया’ जैसी बेहतरीन फिल्मों को निर्माण हुआ जिन्हे पर्याप्त चर्चा भी मिली।

हैदर
‘हैदर’ को सामाजिक और साहित्यिक चिंतकों ने भी बहुत गंभीरता से लिया। जनसत्ता जैसे लब्धप्रतिष्ठित समाचार पत्र में बहुत दिन बाद किसी फिल्म पर बड़े स्तर पर बड़े विद्वानों द्वारा सार्थक बहसें हुईं। ‘हैदर’ चाहे भले ही शाहिद कपूर के नायकत्व की फिल्म हो पर इसके केंद्र में तब्बू हैं, एक स्त्री। ऐसी स्त्री जिसका पति ईमानदार और इनसानी भावों से युक्त एक डाक्टर है। एक माँ है जिसे अपने शहर के बिगड़ते हालत में अपने बच्चे के बिगड़ जाने की पूरी संभावना है इसलिए वह उसे अलीगढ़ पढ़ने भेजती है। विशाल भारद्वाज की बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित फिल्म की चर्चा इसलिए भी अधिक हुई क्योंकि यह फिल्म अपने समय के कई मुद्दों से भी जुड़ जाती है। कश्मीर भारत का सबसे विवादित और और खूबसूरत हिस्सा है पर यहाँ का जीवन कठिन हैं, हालत गंभीर हैं यहाँ घर से सब्जी लेने जाने से पहले आपके हाथ में पैसा हो कि नहीं आपका पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है वरना आप अपने घर में आतंकवादी घोषित किए जा सकते हैं। पहचान और अस्मिता का यह संकट सबसे अधिक स्त्रियों के साथ है।
हैदर का नायक अगर शाहिद कपूर को मान लें तो नायिका श्रद्धा कपूर को होना था लेकिन सच ये है कि हैदर की नायिका तब्बू ही हैं। यह नायिका पति से जितना प्रेम करती है उसका देवर उससे ज्यादा प्रेम उसे करने का दम भरता है। अपने देवर द्वारा अपने पति की हत्या की बात उसे नहीं पता पर बेटे को पता चल जाती है। समस्या यहाँ है कि पति की हत्या की पूरी आशंका होते हुए भी उसे उम्मीद है कि उसका पति वापस आ जाएगा। क्योंकि हत्या को छुपा लिया गया, ये कहकर कि एक आतंकवादी के इलाज के शक में उन्हें पूछपाछ के लिए ले जाया गया है। उम्मीद तो होती ही है टूटने के लिए, कुछ वक्त के अंतराल पर नायिका को यह आभास हो जाता है कि उसके पति को मारा जा चुका है लिहाजा वह अपने देवर के साथ निकाह कर लेती है। फिल्म की मूल कहानी के साथ बहुत सारी कहानियाँ भी साथ चलती हैं। नायिका की कहानी सुनने में बहुत सरल है पर पर्दे पर देखें तो कचोटती है। फिल्म में बहुत सारे पेंच हैं जो भारतीय मानसिकता से देखने पर समस्या पैदा करते हैं। विदित है कि ‘हैदर’ सेक्सपियर के महान नाटक ‘हेमलेट’ का भारतीय संस्करण है। जाहिर इसका परिवेश भारतीय स्त्री का नहीं है इसलिए तब्बू का पति के मृत्यु की पूरी सूचना नहीं होने पर भी अपने देवर (जो इस फिल्म का खलपात्र है) से निकाह करना दर्शकों को खलता है। तब्बू के प्रति घृणा पैदा करता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तब्बू ने यह फैसला अपने अपने बेटे की सुरक्षा की दृष्टि से लिया हो। वह पूरी फिल्म में अजीब कश्मकश में जीती है, अजीब उलझन उसके चेहरे पर झलकते हैं, मुस्कुरा कर अपने देवर (जो अब उसका पति है) के लिए जाम बनाते समय भी उसके खूबसूरत चेहरे (जिस पर उसका देवर वर्षों से फिदा है) में अंदर तक बेधने वाली बेचैनी है। ‘हैदर’ की नायिका पत्नी और प्रेमिका होने के साथ ही एक जवान होते बेटे की माँ भी है। वह जिस माहौल में है वहाँ सारी सुविधा और सुंदरता होते हुए भी घुटन है। वह नहीं चाहती कि उसका बेटे इस घुटन का हिस्सा बने। बेटे को अंत तक यही शिकायत है कि माँ अपने पति के हत्यारे के साथ खुश है, पर सच यह है कि नायिका को जरा भी भान नहीं है कि, उसके पति का हत्यारा उसका देवर ही है। वह देवर को इसलिए ही चुनती है कि उसे अपने से ज्यादा अपने बेटे की सुरक्षा और एक नाम की जरूरत है, क्योंकि वह जानती है यह ऐसी जगह है जहाँ जीने के लिए साँसों से ज्यादा जरूरत आपकी ‘आइडेंटिडी’ की है।
दरअसल ‘हैदर’ एक स्त्री की कहानी है जो ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहाँ से एक रास्ता उसके पति की तरफ जाता है जिसका होना और न होना बराबर है। एक रास्ता बेटे की तरफ है जिसके लिए उसे एक नाम चाहिए। तीसरा रास्ता ये है कि वह शहर छोड़ दे जो संभव ही नहीं है चौथा रास्ता उसके देवर की ओर जाता है जहाँ उसे वह सारी सुविधाएँ मिल सकती हैं मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक भी। कभी-कभी ऐसा भी होता है जब विकल्पों का ढेर हमें विकल्पहीन बना देता है। हमारे साथ जुड़े लोगों की समस्याएँ इतनी बड़ी होती हैं कि उनके ही लिए मजबूरी में हमें ऐसा रास्ता चुनना पढ़ता है जो कभी भी ठिकाने पर नहीं ला सकता। इस फिल्म में एक सबसे बड़ा दिखने की चाह में खड़ी एक लोभी सत्ता है। हालात से मजबूर इनसानों से जानवरों जैसा व्यवहार करने पर मजबूर कानून है, लाचार और कट्टर सामाजिक व्यवस्था है और इन सबसे टकराती एक स्त्री कि घायल अस्मिता है। जो अपने अस्मिता को बचाए रखने के लिए पुरुषों की तरफ दया से देखने पर बाध्य है। बेटे को अपनी माँ के इस समझौते पर कोफ्त है। वह खुद को अकेलेपन के किनारे तक घसीट ले जाता है। नायिका के साथ एक दिक्कत यह भी है कि उसका पति पेशेवर डाक्टर होने के साथ एक नेक इनसान भी है, वह किसी के इलाज से पहले उसकी पहचान, मजहब या जाति नहीं पूछता बस इलाज करता है। पर उसके साथ एक दिक्कत यह भी है कि उसके पास अपनी पत्नी के लिए वक्त नहीं है। पास रहकर भी अपने पति से एक दूरी को झेलती नायिका खुद में एक खालीपन महसूस करती है। बेहद खूबसूरत होकर भी, पति का उसमें कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं। फिल्म के एक दृश्य में अपने बेटे से गजाला (तब्बू) का यह कहना – ‘तेरे पिता की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है’ कई अर्थों को खोलता है। एक शादीशुदा औरत कि जिंदगी में उसकी कुछ भावनाएँ जुड़ी होती हैं जो पारिवारिक भी होती हैं और शारीरिक भी। गजाला इन दोनों मे कमी महसूस करती है। उसका देवर इस कमी को पूरा करता है लिहाजा वह वहाँ अपने आप को सेफ महसूस करती है। दरअसल गजाला को अपना दुख कहने के लिए कोई साथी भी नहीं, सिवाय बेटे के। अब सवाल यह भी है कि क्या वह अपनी ऐसे खालीपन को अपने बेटे से बता सकती है जो उसके निजी हैं? नहीं, क्योंकि स्त्री जब माँ हो जाती है तो वह सामाजिक और भावनात्मक दोनों रूपों से और बंधन में बँध जाती है।
तब्बू के साथ श्रद्धा कपूर भी फिल्म की मुख्य भूमिका में है। उनके चेहरे की मासूमियत और आँखों में प्रेम का उदात्त भाव एक ऐसी प्रेमिका की छवि बनाता है जिसकी चाहत हर प्रेमी करता है। इससे पहले वह ‘आशिकी-2’ में प्रेम आकंठ डूबी प्रेमिका की बेहतरीन भूमिका से अपना दर्शक वर्ग बना चुकी है। ‘हैदर’ में में वह नायक का कवच बन पूरी फिल्म में मौजूद हैं। हैदर की शारीरिक और मानसिक जरूरतों को वह पूरी करती हैं क्योंकि वह उसकी घोषित मंगेतर है और प्रेमिका भी। वह बदले की भावना में तिल-तिल कर पिघलते अपने प्रेमी के जीवन के हर दुख में बिना किसी शिकायत के शामिल है। एक तरह से देखें तो पूरी फिल्म में यह साफ दिख जाता है कि स्त्रियाँ समाज और व्यवस्था के बनाए गए नियम के बिंदुओं में सबसे नीचे होती हैं। उनकी बारी सबसे बाद में आती है पर जहाँ पारिवारिक जिम्मेदारी की बात आती है उसकी जरूरत सबसे पहले महसूस होती है। पारिवार की बुनियादी चीजों के लिए हैरान परेशान होती स्त्री को अपनी जरूरतों के लिए घुटना पड़ता है। जिस बेटे के लिए वह अपने स्वाभिमान तक को दाँव पर लगा देती है उसी बेटे के लिए अंत में उसकी मृत्यु भी होती है।
‘हैदर’ की कहानी एक स्त्री की ध्वस्त होती इच्छाओं, खोई हुई अस्मिताओं और कभी न मिलने वाले अधिकारों के साथ विवश होकर जीने की कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। ‘हैदर’ उन्ही कहानियों का एक पार्ट है।
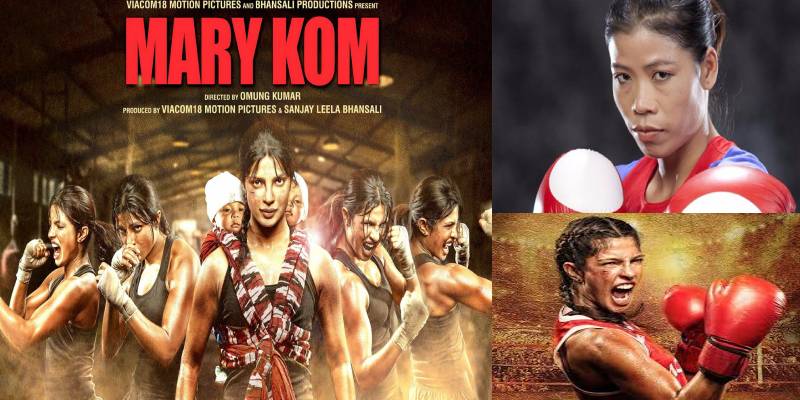
मेरीकाम
‘मेरीकाम’ एक स्त्री की जिजीविषा और प्रगतिशील चेतना की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। इस फिल्म की कहानी सबको पता है इसलिए अधिक कुछ कहने की जरूरत मुझे महसूस नहीं होती पर यह तय है कि ‘मेरीकाम’ उन तमाम लड़कियों, औरतों के लिए एक प्रेरणा की तरह है जिनके जीवन में सिर्फ अभाव है। शून्य से शिखर तक पहुँचने की कहानी को प्रियंका चोपड़ा ने जी लिया है। अपने फिल्मी कैरियर की ग्लैमर से शुरुआत करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने बहुत ही जल्दी ये समझ लिया कि सिर्फ बदन दिखाकर बहुत दिन तक यहाँ टिकना मुश्किल है। वैसे भी हमारे सिनेमा का एक वर्ग अश्लीलता के उस छोर तक पहुँच चुका है जहाँ बस नंगा होना बाकी है। स्वाभिमान और इज्जत कि बात करने वाली नयिकाएँ यहाँ ब्रांड बनाए के इच्छा में यहाँ कभी अपनी यौनिकता को दाँव पर लगती हैं तो कभी बोली लगाकर बेच देती हैं। प्रियंका की फिल्म में बहुत लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि वह मेरीकाम जैसी नहीं दिखती हैं पर यहाँ सवाल ‘मेरीकाम’ जैसे दिखने से अधिक ‘मेरीकाम’ कि जिंदगी के अध्यायों को खोलना था। उनके संघर्षों से परिचित होना था। उनके जीवन में आने वाली अवरोधों को दर्शकों से परिचित कराना था और निःसंदेह प्रियंका चोपड़ा इसमें 100 प्रतिशत सफल ही हैं। ‘मेरीकाम’ से पहले मिल्खा सिंह के जीवन पर ‘भाग मिल्खा भाग’ निर्माण हो चुका था लिहाजा उससे भी तुलना होनी ही थी, हुई भी पुनः कहती हूँ, निःसंदेह ‘मेरीकाम’ कहीं से कमजोर फिल्म नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरी बहस इस बात पर नहीं है कि फिल्म की कहानी, उसका निर्देशन और प्रस्तुतिकरण कैसा है, मेरी सारी चेतना इस बात में है कि उसमें स्त्री अस्मिता और स्त्री चेतना का कौन सा रूप कितनी मजबूती से प्रस्तुत हुआ है। ‘मेरीकाम’ की कहानी एक मामूली और साधारण सी स्त्री के संघर्ष से शुरू होती है, जिसका पहला विरोध घर में ही होता है। एक स्त्री के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होता है कि उसे अपने संघर्ष कि शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ती है। हमारे भारतीय समाज का कोई भी हिस्सा हो, क्षेत्र हो, स्त्री का संघर्ष बराबर है। जहाँ वह जागरूक है वह थोड़ा सकून है पर वहाँ भी दूसरे तरीके का शोषण है। एक बात और कि स्त्री को जगह हर समाज हर समय जो वह करना चाहती है, उसे प्रूफ करना पढ़ता है कि वह कर पाएगी या नहीं। अगर वह प्रूफ कर दे तो और दिक्कत है कि आगे कैसे करोगी? कौन मौका देगा? ‘मेरीकाम’ इन सवालों से बार-बार टकराती हैं पर डिगती नहीं। प्रेम भी करती हैं तो हारती नहीं। माँ बनती है तो रुकती नहीं, अपमानित होने पर डरती नहीं बल्कि और मजबूत होती जाती है। ‘मेरीकाम’ की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को समझने के साथ ही एक संघर्ष करती स्त्री की ये छवि बहुत बहुत प्यारी है। दिल में उतर जाने वाली। पुरुषवादी इस समाज में रात के समय घर जाने के लिए ‘मेरीकाम’ का प्रेमी जब उसके डरने की बात पूछता है ‘मेरीकाम’ का यह कहना कि – ‘तुम मेरे साथ सेफ हो’ हिंदी सिनेमा के संवादों के अध्याय का सबसे वजनदार संवाद प्रतीत होता है। ‘मेरीकाम’ की कहानी सिर्फ जमीन से आसमान तक पहुँचने की कहानी नहीं है बल्कि भावनाओं और संवेदनाओं की पूरी एक गठरी है जो आपको रुलाएगी भी और हँसाएगी भी और अगर आप स्त्री हैं तो आपको हौसला भी देगी कि – ‘डर के आगे जीत है।’

रंगरसिया
‘रंगरसिया’ पर लिखने का मतलब किसी फिल्म की समीक्षा लिखना भर नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता पर बहस करना है। कला और धर्म के अंतर्द्वंद्व को परिभाषित करना है। ‘रंगरसिया’ इस दशक की कुछ बेहतरीन फिल्मों में है जिसके केंद्र में भी एक स्त्री है। जिसे समाज वेश्या कहता है पर कलाकार देवी कहता है क्योंकि उसकी सुंदरता में उसे किसी देवी का चेहरा दिखता है। जाहिर है ये फिल्म महान कलाकार रवि वर्मा के जीवन पर केंद्रित है। जिन्होंने हिंदू देवी-देवताओं की कहानियों को रंगों में परिभाषित किया। धार्मिक जकड़न से देवी-देवताओं को मुक्त कर उस जनता तक पहुँचाया जो समाज के हाशिए पर थे।
‘रंगरसिया’ स्त्री की मुक्ति और अस्मिता दोनों के संकट को बहुत ही गंभीरता से व्यक्त कर ले जाती है। फिल्म की नायिका नंदना सेन बेहद खूबसूरत हैं, इतनी कि रवि वर्मा जैसा कलाकार उनके इस रूप में देवत्व को महसूस करता है। इस फिल्म में एक कलाकार द्वारा एक वेश्या को देवी बनाकर उसके सोए हुए स्वाभिमान को जगा देना और फिर समाज के कुछ संकीर्ण लोगो द्वारा उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करना कला और समाज की व्यवस्था को बहुत बारीकी से चित्रित किया गया है। फिल्म का नायक रवि वर्मा स्त्री सौंदर्य का उपासक भी है और भोगी भी। कला उसकी पहली प्राथमिकता है। नायिका को देवी बन जाने से अधिक खुशी कलाकार की अभिव्यक्ति का साधन बन जाने में है। दुनिया के लिए उपेक्षित नायिका को प्रेम मिलता है तो वह पिघल जाती है। कलाकार उसकी तस्वीर बनाता है तो उसे देवी कि तरह पूजता है और जैसे ही कलाकार की खोल से बाहर निकलता है प्रेमी बन जाता है। कलाकार और प्रेमी की अद्भुत भूमिकाओं में रणदीप हुडा ने आने फिल्मी कैरियर का सर्वोत्कृष्ट अभिनय किया है।
‘रंगरसिया’ एक बार में देखी जाने वाली फिल्म नहीं है। बार-बार देखी जाने वाली फिल्म है। कभी नारी सौंदर्य कि दृष्टि से, कभी प्रेम में डूबे कलाकार और उसकी प्रेरणा में सब कुछ न्योछावर करने को आह्लादित एक एक स्त्री कि दृष्टि से, कभी कलाकार का एक उपेक्षित स्त्री को देवी बना देने की जिद की दृष्टि से। यह फिल्म तमाम कोणों से देखी जानी चाहिए। पर इतना निश्चित है कि आप फिल्म चाहे जिस कोण से देखें उसके केंद्र में नारी है, उसका सौंदर्य हैं, उसका समर्पण है, मूर्तिवत खड़ी एक कलाकार की प्रेरणा, उसके कला को जीवंत बनाने के लिए उसके बाँहों मे झूलती एक प्रेमिका है…
इस तरह देखें तो इस वर्ष स्त्री अस्मिता के तमाम सूत्रों को खोलने वाली फिल्मों की अधिकता रही। सुखद है कि सिनेमा अब स्त्री जीवन को लेकर गंभीर हो रहा है निश्चय ही उसे उसके समर्पण और शक्ति का एहसास हो चुका होगा।