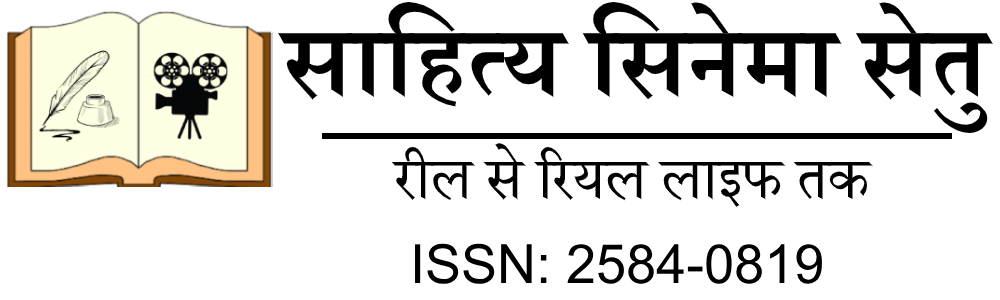बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार पुरुष जैसा आचरण करता है वैसा ही होता है। सदाचारी या पापी की व्यवस्था सदाचार एवं पापाचार के अधीन है। पुण्य-कर्म से पुण्य एवं पाप कर्म से पाप कहा जाता है। जो कर्म करता है वही फल प्राप्त करता है। कर्मासक्त पुरुष कर्म की वासना के साथ वही लिघङ्ग शरीर प्राप्त करता है जिसमें उसका मन अन्तर्निहित रहा करता है। उस कर्म का भोग के द्वारा अन्त प्राप्त कर इस लोक में पुरुष पुनः जो कुछ करता है उसी कर्मलोक को प्राप्त करता है और उस लोक में पुनः कर्म के लिए इस लोक में आता है। भावार्थ यह है कि कर्म के कारण ही प्राणी का आवागमन बना रहता है। मन ही कर्म का मूल कहा गया है। इस सन्दर्भ में छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार पुरुष जब मन द्वारा चाहता है कि कर्म करूँ तभी कर्म करता है। वह मन से ही पुत्रों एवं पशुओं की तथा इहलोक एवं परलोक की इच्छा करता है। अतः कर्म का मूल मन है जिससे तीनों लोकों की प्राप्ति फलरूप में बतलायी गयी है।
स्मृति के अनुसार कर्म के प्रवर्तक तीन अघङ्ग हैं- ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। स्मृति में कहा गया है कि क्रियारूप कर्म गुणभेद से तीन प्रकार का होता है जिसमें आसक्ति, राग तथा द्वेष के बिना फलेच्छा रहित पुरुष द्वारा किया हुआ नियत कर्म (नित्य एवं नैमित्तिक) (क) सात्विक कर्म होता है। स्पष्ट है कि काम्य और निषिद्ध कर्म इस श्रेणी में नहीं आते। फलप्राप्ति की इच्छा वाला अहंकारयुक्त पुरुष अधिक आयासपूर्वक जो (काम्य) कर्म करता है वह (ख) राजस कर्म होता है। परिणाम, धन एवं शक्ति के क्षय से, हिंसा तथा पौरुष की अपेक्षा न करके मोहवश किया जाने वाला (निषिद्ध) कर्म (ग) तामस कर्म कहलाता है। इस विषय पर धर्मग्रन्थ आदि में और भी कई प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं जिनमें प्रवृत्ति-निवृत्ति जनक कर्म, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, काम्य कर्म, सहज कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म आदि की गणना विशेष रूप से होती है।
यद्यपि इन सभी प्रकार की कर्मों की भूमिका विभिन्न सन्दर्भों में महत्त्वपूर्ण है तथापि जिस दार्शनिक पटल पर हम ‘कर्म सिद्धान्त’की चर्चा करने जा रहे है, वहाँ कर्मों का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है जो अत्यन्त प्रासंगिक है।
(i) क्रियमाण कर्म/संचीयमान कर्म- वह कर्म जो इस जीवन में दैनन्दिन किया जा रहा है एवं भविष्य में जिसका फल प्राप्त होगा, उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। ये कर्म ही संचित कर्म बनते हैं।
(ii) संचित कर्म- दैनन्दिन या वर्तमान समय से पहले किया कर्म, चाहे इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का और जिसका कर्मविपाक (फलभोग) आरम्भ नहीं हुआ है, वह संचित कर्म कहलाता है।
(iii) प्रारब्ध कर्म- जिन कर्मों का या कर्माशयों का फलभोग आरम्भ हो चुका है, वे ही प्रारब्ध कर्म है। दूसरे शब्दों में, जिन कर्मों के फलभोग के प्रभाववश प्राणी के द्वारा शरीरविशेष को धारण किया गया है, वे प्रारब्ध कर्म हैं। अतः वर्तमान शरीर अथवा जीवन में प्राणी जिन पूर्व कर्मों का फल भोग रहा है वही ‘प्रारब्ध कर्म’ है।
कर्म सिद्धान्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
यदि एक मत से यह मान लिया जाए कि सृष्टि की समस्त घटनाएँ ईश्वरेच्छा है या किसी ईश्वरीय शक्ति के बिना स्वयं ही घटित हो रही हैं तो ऐसी स्थिति में कर्मसिद्धान्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। किन्तु ये दोनों ही पक्ष मान्य नहीं हैं। ईश्वर के पक्ष में यह प्रश्न उठता है कि यदि वह सब कुछ अपनी इच्छा से ही कर रहा है तो ‘ईश्वर’होकर वह इतना कठोर, अन्यायी या असमानता की दृष्टि वाला कैसे हो सकता है? क्योंकि भारतीय धर्म और दर्शन में ईश्वर की अवधारणा ठीक इसके विपरीत है। लोक में यह देखा जाता है कि सत्कर्मी भी दुःखी रहते हैं और दुष्कर्मी भी सुख पाते हैं। कोई बहुत ही सम्पन्न परिवार में जन्म लेता है और किसी का जन्म ऐसे परिवार में होता है जहाँ दो समय आहार भी नहीं मिल पाता। किसी की आयु लम्बी होती है और कोई अल्पायु होता हैं, कोई वृद्धावस्था में भी स्वस्थ रहता है और कोई युवा होते हुए भी अत्साध्य रोग से पीडि़त। इस प्रकार की कई विविधताएँ हमें प्रत्यक्ष हैं। ऐसे में क्या ईश्वर का यह स्वभाव किसी भी धर्म अथवा दर्शन को स्वीकार्य होगा, नहीं। तो फिर संसार की इस विषमता का कारण किसे माना जाए? यदि हम ईश्वर को न मान कर यह कल्पना करें कि सब कुछ स्वतः ही घटित हो रहा है, तब यह प्रश्न उठता है कि संसार की जो व्यवस्था दिखलायी पड़ रही है- यह कहाँ से और कैसे बनी? ऐसी स्थिति में ‘कर्मसिद्धान्त’ही जगत् में प्राप्त होने वाली विषमता और सम्यक् व्यवस्था का एक युक्तिसंगत समाधान प्रस्तुत करता है। यही ईश्वर के फलाध्यक्ष होने में नियामक बनता है और पुनर्जन्म को भी स्थापित करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते है कि संचित कर्म भूतकालिक, संचीयमान कर्म भविष्यकालिक और प्रारब्ध कर्म वर्तमानकालिक हैं।
‘कर्मवाद’जगत् की दो पूर्वमान्यताओं पर प्रतिष्ठित है- (i) कृतप्रणाशशून्यता और (ii) अकृत-अभ्यागमशून्यता। कर्ता के द्वारा किये गए कर्म के सुख अथवा दुःख रूपी फल उसको अवश्यम्भावी रूप में प्राप्त होता है अर्थात् कृत का प्रणाश असम्भव है। उसी प्रकार संसार में कर्ता के द्वारा न किए हुए कर्म का फल कभी भी उसे प्राप्त नहीं होता है अर्थात् अकृत का अभ्यागम असम्भव है। कर्मवाद के अनुसार कर्ता का कर्मविषयक उत्तरदायित्व तथा उसके द्वारा कर्मफल भोग की दृष्टि से चार प्रकार के सांसारिक वातावरण की कल्पना की जा सकती है –
(क) जहाँ पर कृत का प्रणाश और अकृत का अभ्यागम उभय घटित होते हैं।
(ख) जहाँ पर कृत का प्रणाश होने पर भी अकृत का अभ्यागम कभी नहीं होता है।
(ग) जहाँ पर कृत का प्रणाश कभी न होने पर भी अकृत का अभ्यागम होता है।
(घ) जहाँ पर न तो कृत का प्रणाश और न अकृत का अभ्यागम होता है।
‘कर्मवाद’ के अन्तर्गत प्रथम तीन सम्भावनाओं में मानव के आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि कृतप्रणाश तथा अकृत के अभ्यागम की सम्भावनाएँ विधि-निषेधव्यवस्था की मूलोच्छेदी होती है। विधि-निषेधव्यवस्था के बिना मानव का आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन आधारहीन हो जाता है। अतः मानव के आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन की उपपत्ति के लिए जगत् की कृतप्रणाशशून्यता तथा अकृत-अभ्यागमशून्यता अपरिहार्यरूप से स्वीकार्य है। सम्भवतः उपर्युक्त प्रकार की नैतिक युक्ति के आधार पर ही कर्मवाद को भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक परम्परा में सर्वमान्यता प्राप्त हुई है।
कर्मवाद के स्वरूप निरूपण के लिए विधि-निषेध (करणीय-अकरणीय) व्यवस्थाओं की साधारण पूर्वमान्यताओं पर विचार अपेक्षित है। भारतीय धर्मशास्त्र परम्परा में व्यवहार (आचार) नाम से परिचित व्यवस्था, आधुनिक राष्ट्रों की विधि व्यवस्थाएँ, नैतिक एवं सामाजिक अकर्तव्य व्यवस्थाएँ इत्यादि सभी विधि तथा निषेध व्यवस्था के उदाहरण है। ‘सत्य भाषण करना चाहिए, ‘प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना चाहिए, ‘प्रतिश्रुत वचन का पालन करना चाहिए आदि विधि के उदाहरण हैं।
‘परस्व का अपहरण नहीं करना चाहिए, ‘दूसरों की दुर्दशा का लाभ नहीं उठाना चाहिए’, ‘मिथ्याचार से निवृत रहना चाहिए’, ‘दुर्बल एवं निःसहाय का शोषण नहीं करना चाहिए’आदि निषेध के उदाहरण हैं। विधि एवं निषेध के अनुसार पुरुष (कर्ता) द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा नियमों का अनुपालन है और उनसे विपरीत आचरण उसके द्वारा नियमों का उल्लंघन है। परन्तु विशेष परिस्थिति में विधि एवं निषेध का अपवाद अपरिहार्य होता है। जैसे, यदि अपना अथवा दूसरे प्राणी का प्राण सघड्ढट में हो, तब मौनालम्बन या असत्य भाषण करना कर्तव्य का पालन ही है। किन्तु किन विशेष परिस्थितियों में नियमों का अपवाद अपरिहार्य है- इस ज्ञान की योग्यता भी कर्ता से अपेक्षित है। कर्मवाद में इन नियमों के पालन से कर्ता को इष्ट की प्राप्ति एवं नियमों के उल्लंघन से अनिष्ट की प्राप्ति होना, विधि-निषेध व्यवस्था की अन्य अपरिहार्य पूर्वमान्यताएँ हैं।
वस्तुतः व्यक्ति को एक साथ अनेक विधि-निषेध व्यवस्थाओं में कर्ता की भूमिका निभानी पड़ती है। व्यक्ति परिवार एवं समाज विशेष का सदस्य होता है, एक राष्ट्र का नागरिक होता है, संस्थाविशेष का कर्मचारी एवं समग्र मानव समाज का सदस्य भी होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से धर्म तथा अधर्म, न्याय और अन्याय, उचित तथा अनुचित में भेद करने वाली नैतिक कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था, अन्य विधि-निषेध की व्यवस्थाओं से उत्तरकालीन होने पर भी पुरुषार्थमीमांसा की दृष्टि से आधारभूत है। कारण यह है कि समाज एवं राज्यों की विधि-निषेध व्यवस्थाओं का मूल्याङ्कन उनके प्रयोजन एवं नैतिक व्यवस्था के आधार पर ही किया जा सकता है।
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-
उपनिषद् _ (108 उपनिषद् तीन खण्डों में) सम्पा- श्री राम शर्मा आचार्य ब्रह्मर्चस, शान्तिकुञ्ज हरिद्वार, 2000
श्रीमद्भगवद्गीता _ वेदव्यास (शाङ्करभाष्यसहित), सम्पा- वी- सदानन्द, कम्प्लीट वर्क्स आफ श्री शङ्कराचार्य (भाग 6), समता बुक, मद्रास, 1983
भारतीय दर्शन बृहत्कोश _ बच्चूलाल अवस्थी, शारदा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2012
भारतीय दर्शनों में अन्तर्निहित समरूपता_ वागीश कुमार, परिमल पब्लिकेशन, दिल्ली, 1990
वैशेषिक पदार्थव्यवस्था का पद्धतिमूलक विमर्श _ विश्वम्भर पाहि, दर्शन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 2000