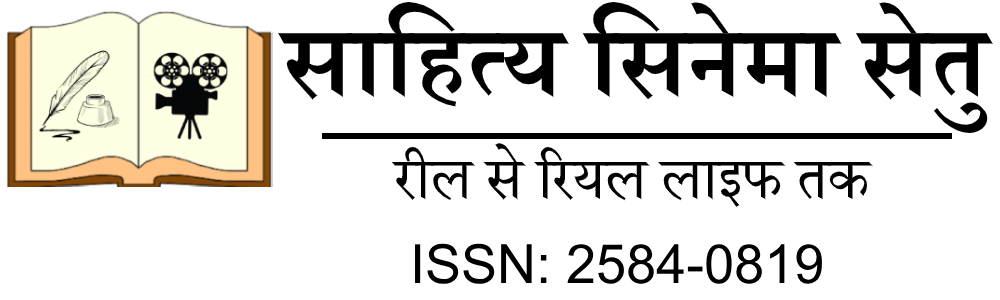“पृथ्वी घूम रही है, कहानी संग्रह में जीवन के संघर्ष”
प्राचीन समय में भी मौखिक रूप से कथा कहानियों की परंपरा रही है। ज्यादातर कहानियों लोक कथाओं का विशेष महत्व रहा है। समकालीन हिंदी कहानी में भी समाज की विडंबनाएं, विद्रूपताएं एवं संवेदनाएं देखने को मिलती हैं। इसी प्रसंग में चर्चित कहानीकार उमाकांत खुबालकर का नया कहानी संग्रह “पृथ्वी घूम रही है” नीरज बुक सेंटर, नई दिल्ली से सन 2024 में प्रकाशित हुआ है। यह समसामयिक विषयों पर आधारित है।
नागपुर में जन्मे उमाकांत खुबालकर जी का यह पांचवा कहानी संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने चार नाटक, एक काव्य संग्रह और दो बाल साहित्य की पुस्तक लिखी हैं। अभी उनकी लेखनी अनवरत जारी है।
‘पृथ्वी घूम रही है’ कहानी संग्रह में कुल ग्यारह कहानियां हैं, जिनमें :- प्रतिघात, परावर्तन, पृथ्वी घूम रही है, नारी अस्मिता, अपराधी का न्याय-तंत्र, अपहृत दिशाएं, हुंकार, कर्मचारी तंत्र, अथ कछुआ पुराण नव कथा, कालचक्र, आहुति। साथ ही ग्यारह लघु कथाएं हैं जिनमें :- तिर्यक रेखा, तांडव, युगबोध, जीते रहो बरखुरदार, समीकरण, फेलामिना आंटी, साक्षात्कार, व्यथा-कथा, इंतजाम, गुरु दक्षिणा, शोकांतिका शामिल हैं।
‘प्रतिघात’ कहानी में सामाजिक संबंधों पर चर्चा, कारोबार के उफान पर मुखिया का अचानक चले जाने से घर परिवार का डगमगाना, संघर्ष, धैर्य, मुसीबत में अंदरूनी ताकत, निर्मल मन की दुआओं को हृदय में उतारना, आत्म अनुशासन से जीवन की दशा और दिशा बदलने, अधेड़ उम्र के प्रेमी की प्रायोजित हत्या, मां के गलत आचरण से बच्चों का आहत होना, दुकानदारी के गुर सीखना, सामाजिक कार्य, प्रेम विवाह में कोर्ट को तरजीह देना इत्यादि है।
मध्यम व्यापारी वर्ग में धन की बहुलता के बीच स्त्री को सांस लेना दूभर हो रहा है। व्यापारी वर्ग में स्त्री की घुटन, बंदिशें, शिकंजे में जकड़ी हुई स्त्री के कदम अपनी स्वतंत्रता की ओर सरक जाते हैं। लेखक स्त्री के शिकंजे को खोलने का प्रयास करते हैं। कहानी की मुख्य पात्र सेठानी की दुकान पर काम करने की झिझक खुलती है और तेजी से व्यापार के समीकरण आत्मसात करके रुके हुए कारोबार को हवा देती है। कहानी स्त्री विमर्श को इंगित करती है।
‘परावर्तन’ कहानी आज के अद्यतन युग के दौर में भौतिक सुख के हवस के पीछे भागते समाज के नैसर्गिक यथार्थ को बेबाकी से बयां करती है। इस भौतिकवादी युग की चकाचौंध में स्त्री हो या पुरुष कोई पीछे नहीं रहना चाहता। इसके लिए वह समाज की सीमाएं भी लांघ जाते हैं। कहानी के मुख्य पात्र नितिन और निकिता का जीवन इसी तरह का है। नितिन जहां अखबार रिपोर्टिंग में अपनी जी जान लगाकर काम करता है, वहीं निकिता अपनी व्यस्त जिंदगी में फिल्म और सीरियल की शूटिंग में अपने पति और परिवार पर ध्यान नहीं देती और साथ काम करने वाले वासु या कपिल कुमार के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने से नहीं चूकती। इस संबंध में कहानी में नितिन अपनी पत्नी के बारे में कहता है कि – “जानेमन, तो लाइफ का कैरेक्टर कब समझ में आएगा? तुमसे ज्यादा तो बाजारू औरत ईमानदार होती है, जो हर हालत में अपने ग्राहक को संतुष्ट कर देती है। अपना देह धर्म बिन हाटहै।”1.
दरअसल निकिता शूटिंग के कैरक्टर में उलझ गई और फिर उसे जीवन के कैरेक्टर भी समझ नहीं आ रहे थे। वह अपने जीवन में कामयाबी का ढोल तो पीटती रही लेकिन गृहस्थ जीवन में असफल हो गई।
इस कहानी में शहरी जीवन की भाग दौड़, बंद मकान में मानवीय छायाओं का कैद होना, महानगरी जीवन संघर्ष और तालमेल, अड़ियल और बेलगाम, फिकरे कसना, महत्वाकांक्षा और व्यस्तता के चलते पेट में पल रहे नवजात शिशु का गर्भपात करवाना, गृहस्थी के बिखरते सूत्र, मानसिक अवसाद, खतरे वाले स्कैंडल की रिपोर्टिंग, जीवन का विचित्र द्वंद, रिश्तों की ताकत, एकाकीपन, आर्थिक तंगी और दिमाग का संतुलन, मजदूरी का हुनर, दांपत्य जीवन की लक्ष्मण रेखा लांघना, वहशी की तरह नोंचना और खसोटना, नारी का रौद्र रूप इत्यादि है।
गरीबी बहुत कठिन दिन दिखा देती है।गरीबों को बेटी की शादी पहाड़ पर चढ़ना जैसा लगता है। वे शादी के काम को जल्दी से निपटाना चाहते हैं, क्योंकि आज के युग में वहशीपन और दरिंदगी का बोलबाला है। हर कोई गरीब स्त्री की अस्मत से खिलवाड़ करने पर आमादा है। इस संबंध में कहानी में भानु कहती है कि- “गांव हो या शहर; जवान तो क्या छोटी अबोध बच्ची पर भी मौका पाकर लोग बाग भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। मां ने भी विधवा रहकर अपने शरीर को गलाया था।”2.
दरअसल, समाज का एक तबका हमेशा गरीब लोगों की अस्मतें लूटने में माहिर रहा है वह उसे अपना अधिकार समझते हैं इसलिए गरीब ज्यादातर अपनी बच्चियों की शादी उम्र से पहले कर देते हैं।
‘पृथ्वी घूम रही है’ कहानी मध्यम वर्ग की समस्याओं में उलझे सूरज और उसकी पत्नी सुगंधा पर केंद्रित है। सूरज को वृद्ध मां की बीमारी पत्नी की चेचक और आर्थिक परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती। बूढी मां को बहु सुगंधा ऐसी कमरे से गाय के कोठे वाले कमरे में शिफ्ट करवा देती है, उसकी सेवा करना नहीं चाहती। लेकिन वह लोगों को अच्छा दिखने की कोशिश करती है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। इस संबंध में लेखक कहानी में लिखते हैं कि – “उन्हें थोड़ा ही पता था कि अपनी लाचारी सासू मां को विकलांग बनाने में उसने कितनी नीचता दिखाई थी।”3.
कहानी में – स्त्री की अंतहीन चिक-चिक, पीड़ाओं की व्यथा, निर्मम व्यवस्था से प्रतिपल पिसने की अंतरकथा, उद्दीप्त कामनाओं की पूर्ति न होना, कोरोना काल का फैलता आतंक, महंगी दवाओं का खर्च, अंग्रेजी माध्यम के महंगे और स्टैंडर्ड स्कूल में दाखिला, बंधुआ मजदूरी, बेगारी, स्वामित्व की भूमि हड़पना, भू-माफिया बन जाना, जर्जर बुढ़ापे की दर्द भरी चीख पुकार, सेवा के नाम पर ढोंग इत्यादि है।
‘नारी अस्मिता’ कहानी में मार्केट में फल बेचने वाली भंवरी और लाजवंती का वाक् युद्ध और सामाजिक द्वंद्व को रेखांकित किया है। फल खरीदने वाले ग्राहकों को अपनी कमनीय देह दिखाकर डंडी मारने वाली भंवरी ने मार्केट को ठग्गू घोषित कर रखा है। कई बार ग्राहकों द्वारा बेइज्जत होने के बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, औरत का मजबूरी में गिरना, इंसानी खरीद फरोख्त, लाश की तरह जीना, खूंखार नजरों से देखना, भावात्मक सहारा इत्यादि है। कहानी में – भंवरी अपने बारे में बताती है कि – ” हां, सिर्फ चौदह बरस की थी रे… एकदम नासमझ, बिन मां बाप की बच्ची। यह मल्लू का बच्चा मेरे शराबी मामा से सिर्फ दो हजार रुपए में खरीद लाया था। क्या बताऊं? मेरी ऐसी दुर्गति की थी कि शराब के नशे में मुझ अनाथ को यह कंस मामा भी नोंच लेता था। तू क्या समझेगी री? मेरे अंदर एक औरत रोज मरती है और लाश के माफिक जीती हूं मैं?”4.
इस प्रकार स्त्री की अस्मिता आज भी खतरे में है। समाज में स्त्री का दमन उसके रिश्तेदार, पड़ोसी और नजदीक के लोग ज्यादा करते हैं। समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
‘अपराधी का न्याय तंत्र’ कहानी में प्रो. रामधन का वृद्धावस्था में अपनों से बार-बार अपमानित होना और छोटे भाई चेतन जिसने अंतरजातीय विवाह किया, उसे घर से निष्कासित करना। चेतन का मानसिक तनाव से नशाखोरी अपराध में लिप्त हो जाना इत्यादि है। बहादुर नेपाली प्रो.रामधन के घर चोरी करके पुलिस में जाने से उसे खुखरी दिखा देता है और चेतन को समाज में अपनाने की धमकी प्रो. रामधन को देता है।अंत में प्रो.रामधन का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अपने आप कहता है कि “रामधन, जितना जो है, देकर छुट्टी पा लो। चलो चेतन, घर चलो। नई बहू का गृह प्रवेश जो कराना है।”5.
इस प्रकार कहानी में जातीय मानसिकता की आग कभी-कभी दबाने से भी शांत होती है। चोरी और सीना जोरी, भय, क्रोध, महानगरी जीवन रक्षक बने भक्षक, चुभती नजरों से देखना, किंकर्तव्यविमूढ़, चीख-चिल्लाहट, वृद्धावस्था का जर्जर शरीर, उदासीनता, खेत बेचकर आलीशान फ्लैट खरीदना, इंद्रियों का निष्पादन, पुश्तैनी जायदाद से बेदखल, अंतर्जातीय विवाह इत्यादि है।
‘अपहृत दिशाएं’ कहानी में शिवकांत और दीपशिखा का निश्छल प्रेम देखने को मिलता है। दीपशिखा को शिवकांत डूबती नैया में तिनके का सहारा साबित होता है। दोनों की मुलाकात नवलेखन शिविर में होती है। मानवीय संबंधों के ताने-बाने में जकड़ी कहानी सामाजिक संबंधों की छटपटाहट और स्वच्छंदता का मार्ग भी ढूंढती है। अद्यतन युग के परिवर्तन और संबंधों की बिखरती कड़ियों को कहानी में देखा जा सकता है। जीवन का सहारा ढूंढ रही दीपशिखा को हर एक जगह आंचल मैला करना पड़ता है।
कहानी में – स्त्री की सुंदरता के मायने, स्त्री को खोलकर पढ़ने की लालसा,लोक लज्जा के भय से दूरी बनाना, हाल-चाल पूछने के बहाने स्त्री का सामिप्य प्राप्त करना, इर्द गिर्द मंडराने वाले पुरुषों के दाव पेंच समझना, संवेदनशीलता, छोटी सोच और मनचले लोगों के ताने, छोटी उम्र में वैधव्य, चरित्रहीन जीवनसाथी से घर में कलह और मानसिक तनाव, जिंदगी की ठोकने खाकर मजबूत होना, स्त्री का रौद्र रूप, ब्रह्मराक्षस से मुक्ति, खून के रिश्ते का कुकर्म, देह व्यापार, संस्कार विहीन समाज की अधोगति, मानसिक उद्वेलन, ठरकी जज द्वारा गुप्तांगों को छूने की कोशिश, मखमली सानिध्य में समय बिताने की अभिलाषा, अनाम विश्वास का रिश्ता, घनघोर संकट और मानसिक अवसाद से घिरना, क्रूर अतीत का हावी होना, अनाथ बच्चों की सेवा से मानवता मुस्कुराने लगना, छल प्रपंच, दिखावे की दुनिया से मुक्ति, खोया हुआ आत्मविश्वास लौटना, वैधव्य जीवन का दंश, ग्लैमर की दुनिया, निर्बाध अवैध संबंध, रिश्तों की डोर धन पर टिकी होना जिंदगी के दुख दर्द न बांटना इत्यादि है।
कहानी में मानवीय संबंधों को सामाजिक धरातल पर तौलने का प्रयास है। इस संबंध में कहानीकार लिखते हैं कि- “इधर, शिवकांत में कुछ दिनों बाद सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति लेकर अपने वृद्ध मां और बहन के साथ छत्तीसगढ़ के गांव में बस गए थे। वे जीवन की आपा-धापी एवं दौड़ से पराजित नहीं थे। जीवन संगिनी को जायदाद का अधिकांश हिस्सा देकर अनाथ एवं निराधार बच्चों की एन.जी.ओ. चलाने लगे थे। अब उनका कुटुंब बड़ा हो गया था। जहां बहु के कुटिल, प्रपंच, शहरी चकाचौंध एवं दिखावे की दुनिया से सदा के लिए मुक्ति मिल गई थी। यह सचमुच अपनों की दुनिया थी, जहां मानवता मुस्कुराने लगी थी।”6.
‘हुंकार’ कहानी में प्रेम विवाह करने वाली कावेरी को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। पति की जॉब में काम में सहायता, दकियानूसी, समय का अभाव, स्कूल टीचर्स द्वारा ताने मारना, आत्मविश्वास जागृत होना, पति शरद कुमार को सब लोगों के साथ जेल की सलाखों के पीछे भेजना, कहानी में – कंजूस पुरुष का अहंकार, कुत्सित मानसिकता, घरेलू हिंसा, बेइज्जती से जागृत होना, अपना पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, लालची, क्रूर पाश्विक मनोवृति, संस्कार हीनता, घुटना और दफन होना, आत्म सम्मान का तहस नहस होना, अन्याय और शोषण पर विराम, संत्रास, मानसिक गुलामी से मुक्ति इत्यादि है।
कावेरी को उनके पति शरद कुमार द्वारा अनेक तरह की शारीरिक-मानसिक यातनाएं देकर प्रताड़ित किया गया। वह परिवार के विरुद्ध चलकर, नाता तोड़कर शरद कुमार के घर में प्रेम विवाह करके आई थी। लेकिन उसने कावेरी की जिंदगी को नर्क बना दिया। बार-बार अपमान की घूंट पीकर रह जाती, स्टाफ में टीचर्स भी चटकारे ले लेकर ताना मारते। अचानक कावेरी का आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत हो गया।इस संबंध में कहानीकार लिखते हैं कि -“असभ्य बर्बर पुरुष की तरह मारता पीटता है। पिछले आठ वर्षों से मेरी चेतना, आत्मसम्मान और जीवन को तहस-नहस कर रहा है। नहीं। अब इस अन्याय एवं शोषण पर विराम लगना चाहिए। होने दो हमारे कुल परिवार की बदनामी। आखिर कब तक घुटती रहूंगी मैं? थैट इज एंड नाउ।”7.
‘कर्मचारी तंत्र’ एक लघुकथा है। इसमें प्रशासन व्यवस्था को गति देने के लिए नए शिक्षा अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को अनुशासन से काम करने की हिदायत देते हैं।काम न करने वालों को कारण बताओं नोटिस देते हैं। और दूर-दराज के इलाकों में स्थानांतरण की धमकी देते हैं। शिक्षा अधिकारी में ने मनकुराम गुप्ता को डांट लगा दी। अब मनकूराम उनके ड्राइवर प्यारेलाल के साथ मिलकर शिक्षा अधिकारी को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। कहानी में – प्रशासन व्यवस्था में ढीलापन, अराजकता, अनुशासनहीनता, मनमानी, निठल्लापन, बेईमान कर्मचारियों की एकता, सरकारी काम में बाधा डालना, अधिकारी से अभद्रता और नारेबाजी, ईमानदार को कुचलने की कोशिश, कर्मचारियों का समय पर दफ्तर न पहुंचना, सरप्राईज इंस्पेक्शन, ड्राइवर की चालाकी, विद्यालयों की खस्ता हालत इत्यादि है।
‘अथ कछुआ पुराण नवकथा’ कहानी में कछुआ खरगोश की दौड़ को कछुआ खरगोश पार्ट 2 करके दिखाया गया है। समाज में धूर्त किस्म के लोग आज भी यही गेम खेल रहे हैं। यह राजनीति परक कहानी है। कहानी में नेता ही जनता में ईर्ष्या और नफरत की भावना भरते हैं। कहानी में – विशेष सभा बुलवाना, प्रतियोगिता से जाति का अपमान-सम्मान होना, विजय-पराजय, कलंक मिटाने के लिए दोबारा से प्रतियोगिता, हिराकात से देखना, मुखिया का इंकार, आमरण अनशन, महाधूर्त नेता द्वारा कुटिलता से प्लान बनाना, कछुए के बहाने आरक्षण पर चोट, तिकड़म से सत्ता हासिल करना, प्रतियोगिता के मापदंड, राजनीति में पत्ते न खोलने का सस्पेंस, चालकी से मैदान जीतना, जीत का रहस्य, गोपनीयता इत्यादि देखने को मिलता है।
‘कालचक्र’ कहानी में मेट्रोमोनियल विज्ञापन से हुई जान पहचान को अपने विचारों एवं भावनाओं के आधार पर गणेश टेकड़ी पर मंदिर के पास बिना घर वालों की सहमति के श्रीकांत और स्वाति अपनी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। कहानी में स्वाति की मां-पिता के अलावा स्वाति और श्रीकांत के संवाद पर ही कहानी खत्म हो जाती है।इसमें आज के नारी सशक्तिकरण के युग में बढ़ते कदम अंतरजातीय विवाह का साहस युवा पीढ़ी में उत्साह का संचार करता है।कहानी में :- अद्यतन युग में युवा पीढ़ी को शादी की आजादी, अंतरजातीय विवाह, रंगभेद, अपरिचित युवाओं का विचार मिलना, नारी सशक्तिकरण, शादी विवाह में अनुभवी लोगों का तजुर्बा,अनपेक्षित वज्रघात, रगड़कर काम लेना, ईमानदारी से सच्चाई बताना, अप्रत्याशित खुशी के हिंडोले में झूलना, देह व्यापार, चेहरे पर ईमानदारी और सच्चाई के भाव तैरना इत्यादि है।
‘आहुति’ कहानी में स्त्री जीवन की मार्मिकता देखने को मिलती है। कहानी में रोहिणी के त्याग, दृढ़ निश्चय, समस्याओं का निराकरण, परिवार के लिए जीना, बेटे से बढ़कर कार्य ,घर का संतुलन और अनुशासन मिलता है। रोहिणी खुद अविवाहित रहकर बेटे का फर्ज पूरा करती है। और छोटी बहनों की शादी करवा देती है।
कहानी में :-जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, लाचार जिंदगी से नफरत, गृहणी का तमाम जिंदगी खटना, मुसीबत में दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना, संकटों से जूझने की आदत, जीवन आहुति के लिए बना होना, घर पहुंचते ही जिंदगी में गतिशीलता आना, सामाजिक बंधन का दबाव हावी होना, कर्तव्य निभाने पर आत्मसंतुष्टि मिलना, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाना, आस्था का डगमगाना, संस्कारी मन का विद्रोह, हवा की गंध से तनाव का पता लगाना, रोहिणी का रौद्र रूप, उग्रता, दूसरों के मामले में नाक घुसेडना, मुखिया का हाथ से पारिवारिक नियंत्रण छूटना, जमाने के थप्पड़ों से अस्तित्व को बचाए रखना, आकांक्षाओं और सपनों का चकनाचूर होना, निकम्मापन, पलायन प्रवृत्ति से अलिखित समझौता करना, अंतर्मुखी होना, परिवार को बांधे रखना, परिस्थितियों से जुड़ने का आत्मविश्वास, खामौसी से निरीक्षण करना, आत्म ग्लानि का परिमार्जन करना इत्यादि है।
‘तिर्यक रेखा’ लघु कथा समाज के बंधन और कामकाजी स्त्री को रेखांकित करती है। वह ऑफिस, घर और सगे संबंधियों सहित जन्म-मरण, उत्सव में अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करें? समय के अभाव में वह एक तिर्यक रेखा खींचती है। यदि खुद किसी के मरण पर नहीं पहुंचेगी तो नई पीढ़ी को संस्कार कैसे मिलेंगे? लघु कथा में – रिश्तेदार की मृत्यु पर शोक प्रकट करना, अतीत का चित्र आंखों के सामने घूमना, दहेज का लालच, औरत का पुरुष के बंधन में रहना, शादी का अर्थ खूंटे से बांधना, गृहस्थी का बोझ और पति का अघोषित कर्ज, ससुराल वालों के खिलाफ विद्रोह, लड़कियों का फ्रस्ट्रेशन, एकाकीपन, स्कूल का तनावपूर्ण माहौल, यातायात के साधनों का अभाव, प्राइवेट वाहनों में जानवरों की तरह सवारियां भरना, कानून की धज्जियां उड़ाना, कंजूसी, मानसिक उहापोह, संस्कार सीखना और सिखाना इत्यादि है।
‘तांडव’ लघु कथा में धार्मिक पाखंड की पोल खोली गई है। महाशिवरात्रि पर जाने वाले श्रद्धालुओं में स्त्रियां एक दूसरे के कपड़ों का निरीक्षण बारीकी से करती हैं। आधुनिक युवतियां भड़कीले वस्त्र पहनकर फैशन शो की तरह वहां पर कैट वॉक कर रही हैं।धर्मांधता के चलते दूध को नालियों में बहाया जा रहा है। एक असहाय स्त्री नाली के दूध को चुराना।
लघुकथा में धार्मिक अनुष्ठान का दृश्य, धार्मिक क्रियाकलापों में भी चुगली, बच्चों की अनुपस्थिति, आपराधिक तत्व, गुंडागर्दी पर बहस, महिलाओं की एक दूसरे के कपड़ों पर बहस, पतियों को डांट फटकार, मंदिर की पंडिताइन द्वारा मंदिर की दान दक्षिणा में चढ़ाए गए नोट सिक्कों को ढूंढना, मां को दूध नहीं आता इसलिए मंदिर की नाली से बहने वाले दूध को लोटे में लेना, धार्मिकता का रस गायब होना, मंदिर का स्तब्ध रह जाना, धर्म का डंका पीटने वालों की चोरी पकड़ी जाना, चीख-पुकार इत्यादि।
‘युगबोध’ लघुकथा में जमाने के अनुसार चलने की नसीहत है। बेमौसम बरसात और सुखा ने किसानों को जमीन बेचने पर मजबूर किया है। आधुनिक जीवन शैली वाले लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। सभी शहरी जीवन जीने के लिए लालायित हैं। उधर आधुनिकता के दौड़ में बढ़ती जमीन की कीमत, खराब मौसम की बिगड़ी फसल से मजबूर किसानों को अपना जीवन सुधारने का मौका था। मातादीन तुरंत निर्णय लेकर जमीन का सौदा कर डालता है। शहरीकरण से काम धंधे की किल्लत हो गई। इस लघुकथा में – पानी के अभाव में जमीन का बंजर होना, किसानों की गरीबी, चंदा इकट्ठा करके देवता को बकरा चढ़ाना, थाल का माड़ पीकर जिंदगी घिसटना, निर्धनता, रोजाना की दिहाड़ी पर चूल्हा जलना, पुश्तैनी खेत बेचकर कर पक्के मकान में रहना, सड़कों का राजमार्ग बनना, धड़ाधड़ खेतों में प्लाट काटना, घर बैठे मुनाफा, अंधी जिद पकड़े जिंदगी काटना, चिंतन प्रबल हो उठना इत्यादि देखने को मिलता है।
आधुनिक समय किसान को खेती करना, समय पर खाना नसीब ना होने जैसा है। लोग जमीन प्लाट बेचकर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं, जो खेत की जिद पकड़ कर बैठे हैं उनका जीवन चलना मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में कहानीकार लिखते हैं कि – “अड़ोसी-पड़ोसी अपना पुश्तैनी खेत बेचकर पक्के मकानों में रहने लगे थे। फिर कुछ हिस्सा किराए पर उठा दिया था। इससे घर गृहस्थी का थोड़ा खर्चा पानी निकल ही जाता है। सड़कें अब राजमार्ग बनती जा रही हैं। धड़ाधड़ प्लॉट कट रहे हैं, घर बैठे मुनाफा हो रहा है। एक वही है जो अंधी पकड़े जिंदगी काट रहा है । उसका चिंतन प्रबल हो उठा।”8.
‘जीते रहो बरखुरदार’ लघु कथा में विशंभर प्रसाद स्वयं को एड्स बताकर दिल्ली वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। वहां से दुबई चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। एड्स होने की झूठी खबर खुद ही फैला देता है। घर में कोहराम मच जाता है। लघुकथा में – एड्स की खबर, व्यवहार में परिवर्तन, ससुर द्वारा स्त्रियों को घूरना, सास-बहू में तीखी नोंक-झोंक, चरित्रहीनता, सामाजिक बहिष्कार, एड्स से संक्रमित न होने की सूचना इत्यादि है।
‘समीकरण’ लघु कथा में सब्जी बाजार की मंहगाई को रेखांकित किया गया है। उमाशंकर सब्जी बाजार से लौटी पत्नी को मौसम के हिसाब से ठंडा गर्म पेय पदार्थ प्रस्तुत कर देते हैं। इस लघु कथा में – सब्जी मार्केट से विजेता की तरह लौटना, चेहरे पर सफल गृहस्थी का आत्मविश्वास, प्रशंसा मिश्रित भाव, सब्जी खरीद पुराण खत्म न होना, सुरसा का बढ़ता मुख और मंहगाई, धड़धड़ाते विज्ञापन, रसोई घर में बर्तन पटकने की आवाज से चौंकना इत्यादि है।
फेलामिना आंटी’ लघुकथा में समय के साथ तालमेल न बिठाकर चलने वाली फेलामिना बात-बात पर अपने पति फिलिप को डांटती है। सड़क दुर्घटना में मौत के बाद वह विधवा और असहाय हो जाती है। बच्चे भी उसे के जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वह बिलख-बिलखकर रोती रहती है। अचानक रात में दरवाजे के पीछे से फिलिप की आवाज आती है। वह मरे हुए पति की आवाज से डर जाती है। लघुकथा में – गुस्सैल पत्नी का चरित्र, बुलंद आवाज और धाराप्रवाह गालियां देना, पति को गुलाम बनाकर रखना, पति के मरने बाद पत्नी की दुर्दशा, शोक विलाप का करुण क्रंदन, घमंडी स्त्री को रोते-बिलखते देखकर लोगों को आश्चर्य होना, दुर्व्यवहार के लिए लज्जित होना, अचानक फिलिप के भूत का लौटना, भय और आतंक से चेहरा पीला पड़ना, इत्यादि। इस संबंध में कहानीकार लिखते हैं कि – “उसका चेहरा भय और आतंक से पीला पड़ गया था। जीवनभर फेलामिना की आवाज से फिलिप की रूह कांपती थी। आज उस मृत पति से इतना दर क्यों लग रहा था।”9.
‘साक्षात्कार’ लघुकथा में पंडित दुर्गाप्रसाद और उनकी पत्नी कृतिका का जीवन प्रसंग दिखाया गया है। उन्होंने जीते जी पत्नी को नजरबंद रखा। आना-जाना, पराए मर्द से बातचीत न करना, उसने अपना और पत्नी का चरित्र हनन नहीं होने दिया। उनकी मृत्यु के बाद घर की इज्जत सरेआम दिन में भी तार-तार हुई। लघुकथा में – सरकारी सेवा और पुरोहितगिरी में तालमेल का अभाव, खर्चीली और सुंदर पत्नी, स्त्री पर शिकंजा, घुटन और दबाव, पति-पत्नी में अविश्वास, घरेलू हिंसा, दर्द का सैलाब उमड़ना, दिल पर पत्थर रखना, जिंदगी का तेजी से करवट मारना, सामाजिक शिकंजे में जकड़ी स्त्री का खुली हवा में सांस लेना, स्त्री के आसपास चिपकू और हितचिंतकों की भीड़ होना इत्यादि। इस संबंध में कहानीकार लिखते हैं कि – ” जिस कमनीय देह को पंडित ने वर्षों पहले बंद कमरे में छुआ होगा, वही देह दिन के उजाले में बिकने लग गई थी। पंडित कभी अच्छा पति नहीं बन सका था, फिर भी फ्लादिवार पर लगी उसकी तस्वीर का सामना अब वह नहींकर सकती थी…।”10.
‘व्यथा कथा’ लघु कथा में कोरोनाकाल की झांकी देखने को मिलती है। देश का वीआईपी कल्चर सभी जगह व्याप्त है। वे लोग कभी लाइन में खड़े नहीं होते ,बल्कि सीधे दफ्तर में एंट्री मारते हैं। चाहे कितनी भीड़ क्यों न हो? ऐसी स्थिति में वृद्धजन और अनुशासनप्रिय लोग गच्चा खा जाते हैं। इस लघुकथा में – कोरोनाकाल का अनुशासन, दूरी बनाकर रखना, बैंक के सामने लंबी कतार, कोरोना के नियमों का उल्लंघन, सुरक्षा कर्मी द्वारा भेदभाव, वरिष्ठ नागरिक किंकर्तव्यविमूढ होकर तमाशा देखना, घर बाहर दोनो मोर्चों पर वृद्धजनों का खामोशी से दंश सहना, महिला द्वारा चालकी से बैंक में एंट्री करना, लॉकडाउन में बैंक कार्यों द्वारा ग्राहकों से टालने वाला व्यवहार करना, ग्राहकों के ऊपर गुस्सा दिखाना, मानवीय परछाइयों का धूप में पकना इत्यादि है।
‘इंतजाम’ लघु कथा में फिल्म निर्देशक के एक इशारे पर काम को पलभर में करने वाले फिलिप की हाजिर जवाबी है। फिल्म निर्देशक के चेहरे पर आते जाते संचारी भाव को देखकर ही वह भांप जाते हैं कि उनको क्या चाहिए? इस लघुकथा में – आनन फानन में सामान उपलब्ध कराने वाला निंजा फिलिप, आदमी की परख रखना, साथ काम करने की होड़, सफलता का दारोमदार होना, चेहरे का हाव-भाव को समझना, पल भर में चीज हाजिर करना ,फूल मालाओं का इंतजाम रात के डेढ़ बजे करना, कार्य शैली पर विश्वास, फिल्म स्टूडियो में शूटिंग के लिए फूल माला शमशान से लाना इत्यादि है।
‘गुरू दक्षिणा’ लघु कथा में एक शिक्षिका द्वारा पढ़ाई गए आदिवासी छात्र डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद इतना नकारा और लालची हो गया कि अपनी ही शिक्षिका से भी निशुल्क सैंपल की दवाओं के पंद्रह सौ रुपए ले लेता है। वो भी दवा के नाम पर, इसमें भी डॉक्टर की फीस माफ करके एहसान जताया जाता है। उसे अपने ही लोग असभ्य लगते हैं। इस लघुकथा में – शिक्षक को अपने द्वारा पढ़ाए गए छात्र डॉक्टर बनने पर गर्व होना, डॉक्टर की पढ़ाई की फीस की परेशानी, घूंस देकर काम करवाना, आदिवासियों को असभ्य बर्बर बोलना, दहेज लेने की हसरत, कंजूसी, पूर्व छात्र द्वारा अपनी शिक्षिका को लूटना, बुझा चेहरा, आंख मूंदकर भरोसा इत्यादि है। इस संबंध में कहानीकार लिखते हैं – “वैसे तो पांच सौ हैं, आप गुरू हैं, बहुत कुछ ज्ञान दिया है, इसलिए आपसे फीस नहीं लूंगा। हां, ये कुछ प्रोटीन-विटामिन दे रहा हूं। इसका पंद्रह सौ रुपए चार्ज है।’ ‘क्या?’…
सुप्रिया ने ध्यान से देखा। वे सभी दवाओं के नि:शुल्क सैंपल थे। अपनी सामग्री बटोरकर बुझे चेहरे से घर की ओर चल पड़ी थी।”11.
‘शोकांतिका’ लघुकथा में कबूतर के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। जाल में फंसे कबूतर को एक-एक करके सभी लोग देखकर जा रहे थे। लेकिन कोई बचाने का प्रयास नहीं कर रहा था। इस लघुकथा में – बालकनी से ताजी प्राण वायु लेने का प्रयास, तार में निरीह कबूतर का फंसना, मुक्त होने के लिए छटपटाहट, जान बचाने का जज्बा, हृदयहीनता, चुभन, संवेदनहीनता, चेहरा अपराध बोध से उतरना, आत्मा की मौत का तमाशा देखना, पंछियों का झुंड इकट्ठा होना और मूक संवेदना व्यक्त करना इत्यादि।
इस प्रकार ‘पृथ्वी घूम रही है’ कहानी संग्रह में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित किया गया। इसमें मानव जीवन के नैतिक मूल्य, साहस, संघर्ष, आत्मानुशासन, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ाना, स्त्री जीवन पर शिकंजा, भौतिकता की चकाचौंध में सामाजिक रिश्ते और प्रेम को भूलना, जीवन में कामयाबी का ढोल पीटना और यथार्थ से दूर रहना, वृद्ध जीवन का संकट, मानसिक अवसाद, एकाकीपन, युवाओं का लक्ष्य से भटकना और अपराधिक प्रवृत्ति में लीन होना, प्रेम विवाह का रोग गले की हड्डी बनना, दकियानूसी प्रवृत्ति, पितृसत्तात्मकता, आत्मविश्वास जागृत होना, शोषण पर विराम लगाना, सरकारी दफ्तर में काम चोरी और अनुशासनहीनता, आरक्षण पर चोट, नारी सशक्तिकरण, स्त्री जीवन की मार्मिकता, जीवन की परिवार के लिए आहुति, कर्तव्य निभाने पर आत्मसंतुष्टि, संस्कारी मन का विद्रोह, पलायन प्रवृत्ति से अलिखित समझौता, दहेज, आस्था का द्वंद्व और इंसान , शाश्वत चिंता को दिशा देना, चिंतन का प्रबल होना, एड्स का नाम सुनकर चौंकना, महंगाई की मार, जिंदे पति को गुलाम बनाना और मरने पर याद करना, विधवा जीवन के तिरस्कार, स्त्री देह का दिन के उजाले में बिकना, देश का वीआईपी कल्चर, मानवीय परछाइयों का धूप में पकना, काम के लिए हाजिर जवाब, छात्र द्वारा अपनी शिक्षिका को लूटना, अपने ही लोगों को गालियां देना, निशुल्क सैंपल की दवा को बेचना, हृदयहीनता, पक्षियों द्वारा मूक संवेदना व्यक्त करना इत्यादि।
कहानी संग्रह अच्छा है कई स्थानों पर वर्तनी की त्रुटियां हैं। लेखक देर से सही लेकिन यदि कहानी संग्रह और लघुकथा संग्रह अलग-अलग प्रकाशित करते तो पाठकों को ज्यादा लाभ होता। पूरे संग्रह में स्त्री चेतना पर अधिक पढ़ने को मिलता है।कई कहानी और लघु कथाओं में स्त्री पात्र प्रेरणादायक है। लेखक को कहानी का शीर्षक स्त्री पर रखना चाहिए था।कहानियां और लघु कथाओं में भाषा और शब्दों की कसावट की आवश्यकता है।कई स्थानों पर कहानी लघु कथा का शीर्षक भी अटपटा सा लगता है। इस तरह के सुझाव है उम्मीद है लेखक उन पर अमल करेंगे।
संदर्भ ग्रंथ:
1. उमाकांत खुबालकर, पृथ्वी घूम रही है (कहानी संग्रह), पृष्ठ 27
2. वही पृष्ठ 25
3.वही पृष्ठ 33
4.वही पृष्ठ 35-36
5.वही पृष्ठ 42
6.वही पृष्ठ 51
7.वही पृष्ठ 60
8.वही पृष्ठ 101
9.वही पृष्ठ 107
10.वही पृष्ठ 110
11.वही पृष्ठ 116