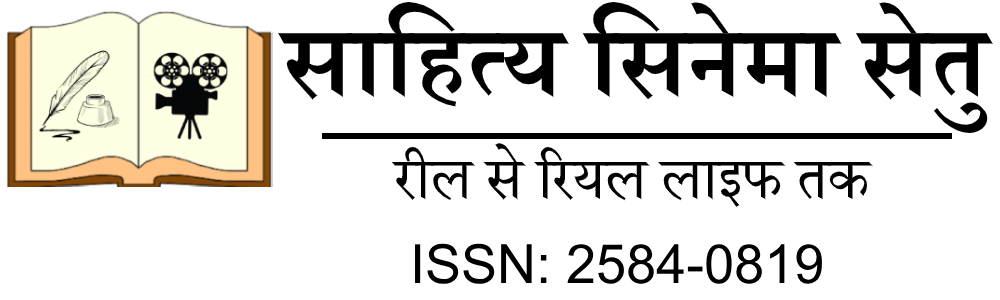शुक्ल ने न केवल इतिहास लेखन की बहुत ही कमजोरपरम्परा को उन्नत किया बल्कि आलोचना के अतीव रुढ़िग्रस्त और क्षीण परम्परा को अपेक्षित गांभीर्य और विस्तार दिया।
डॉ.नगेन्द्र जहाँ रीतिकाल को पुनप्रतिष्ठित करने की भरपूर कोशिश करते दिखते हैं,वहीं शुक्ल वहाँ पर बार-बार प्रहार करते दिखे।
रीतिकाल को पुनप्रतिष्ठित करना नगेन्द्र की पतनोन्मुख दृष्टिकोण का प्रमाण है।आचार्य शुक्ल की आलोचना चिंतन पर हिंदी के आलोचको में मतभेद है।शुक्ल जी का इतिहास एक दृष्टि से प्रथम और अन्तिम है।शुक्ल के बाद से आजतक इतना व्यवस्थित और संगत इतिहास नहीं लिखा गया।शुक्ल इतिहास की गति और नैरन्तर्य पर लिखते हैं–‘जनता की चित्त-वृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चलता है।’ और जनता की चित्त-वृत्ति के परिवर्तन के पीछे वस्तुजगत परिस्थितियाँ होती है।इन वस्तुगत परिस्थितियों की ओर भी शुक्ल का ध्यान जाता है।लेकिन आज की वर्ग-दृष्टि जैसी वैज्ञानिकता की अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती।डॉ.मैनेजर पाण्डेय ने ठीक ही लिखा है कि जनता और शिक्षित जनता के बीच शुक्ल में एक तनाव दिखाई देता है,सम्भवतः इसलिए सिद्धों और संतों को साहित्य से बाहर रखने की बात करते हैं।सिद्धों-संतों के सिद्धांत का निषेध जीवन-प्रियता के स्तर पर उचित है,पर उनकी वस्तुगत स्थितियों का विश्लेषण भी आवश्यक था,और तभी उस आन्दोलन की क्रांतिकारिता को भी सराह सकते थे,यहाँ शुक्ल की सीमा स्पष्ट है।
शुक्ल की इतिहास-दृष्टि शुद्ध साहित्यिक नहीं है,बल्कि वस्तुपरक या सामाजिक है।समाज के अन्तर्सम्बंधों और जातिय स्त्रोतों की ओर भी उनका ध्यान गया है।शुक्ल की तर्क-पद्धति यथार्थोन्मुख कल्पनाशीलता के कारण रचनात्मक है।उनका प्रवृत्तिगत काल-विभाजन प्रायः सर्वमान्य रहा है।रीतिकालीन दरबारी संकीर्णताओं और कलाबाजी पर शुक्ल बार-बार प्रहार करते हैं और इस कारण हिन्दी पाठकों के रुचि-निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय रही है।
आचार्य शुक्ल के मूल्यांकन को लेकर मार्क्सवादी समीक्षकों की दो धाराएँ मिलती है– एक धारा पल्लवग्राही,शौकिया,यान्त्रिक तथा विध्वंसक समीक्षकों के चलते बनी है,जो शुक्ल के साहित्य को प्रतिक्रियावादी साबित करते हुए खारिज करने में जुटे रहें,इस धारा में शिवदान सिंह चौहान,रांगये राघव और डॉ.नामवर सिंह(दूसरी परम्परा की खोज) आते हैं।दूसरी धारा में प्रो.प्रकाशचन्द गुप्त,डॉ.रामविलास शर्मा,डॉ.शिवकुमार मिश्र,डॉ.मैनेजर पाण्डेय आदि कई समीक्षक आते हैं,जो शुक्ल के मूल्यवान विरासत से पहचान रखते हैं और उसे स्थापित करते हैं।
प्रेमचंद के बारे में आचार्य शुक्ल बहुत कम लिखे हैं।पर प्रेमचंद के महत्व पर वे सदा ही दृष्टिपात करते दिखे।—‘नूतन विकास को लेकर आनेवाले प्रेमचंदजी जो कर गये है वह तो हमारे साहित्य की एक निधि ही है।हिंदी साहित्य का इतिहास में शुक्ल लिखते हैं–‘उपन्यास के क्षेत्र में देखिए तो एक ओर प्रेमचंद ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार हिन्दी की कीर्ति को देशभर में प्रसार कर रहे हैं,दूसरी ओर कोई उनकी भरपेट निन्दा करके टॉलस्टॉय का ‘पापी के प्रति घृणा नहीं,दया वाला सिद्धांत लेकर दौड़ता है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेमचंद के निन्दकों से शुक्ल का विरोध है तो टॉलस्टॉय के खोखले मानवतावाद का निषेध भी करते हैं।
आचार्य शुक्ल के चिंतन का प्रगतिशील पक्ष है आध्यात्म को काव्य-क्षेत्र से बाहर रखने की वकालत।वे पण्डिताऊ,रुढ़िग्रस्त आलोचना पद्धति का भी विरोध करते हैं।पश्चिमी कलावाद जो हमारी जातीय- साहित्य- चेतना को समृद्ध करने में बाधक थे,उनका भी डटकर विरोध किया।