कौन जो आवाज़ देता,
बादलों की ओट से ।
भय से मन थर-थर हुआ है,
बिजलियों की चोट से ।
बूंदों की लड़ियां , ये जैसे,
विष में बुझे बाण हैं ।
छिल रहा यह मन तो मेरा,
जो कब से बना पाषाण है।
क्षितिज जैसे, खो स्वरुप को,
आज अदर्श सा हो गया ।
जैसे सूरज , अग्नि अपनी ,
बस बूंदों ही में ,डुबो गया।
नीली आभा आज गगन की,
ले अवकाश के चली गई।
बादलों की गरज-बरस से,
लगता है वह भी छली गई ।
रुप वह भी प्रकृति का ही ,
स्वरुप यह भी उसका है ।
पर बदलना , उसका-इसमें ,
मूल कर्म यह किसका है ?
वो ही ना ,दिखता किसी को,
जो कारक है, सब कर्म का ।
‘अजस्र ‘ आंखें थक गई है ,
न अंश पाया ,उस धरम का ।
कण-कण जो आंखो के आगे,
स्वरुप सब आमूल है। तर्क-वितर्क और ज्ञान चक्षु से,
पर दिखता नहीं, निर्मूल है ।
कण-कण और जन-जन में भी हो ,
सृष्टि-सह-अस्तित्व जैसे ।
कैसे कोई ,फिर हो अछूता,
घोर अंधकार में, घिरे कैसे ?
सगुण-निगुण की भूल-भुलइया,
निराकार का भरम बना।
दिव्य-चक्षु वो कहां से लाऊं,
मूरत में देखूं अक्ष बना ।
पाने उस ही को ,उस स्वरूप में,
तीरथ-तीरथ माथ धरूँ ।
‘अजस्र ‘ पर किरपा बनी रहे उसकी ,
आँखे बंद और दरश करूँ ।
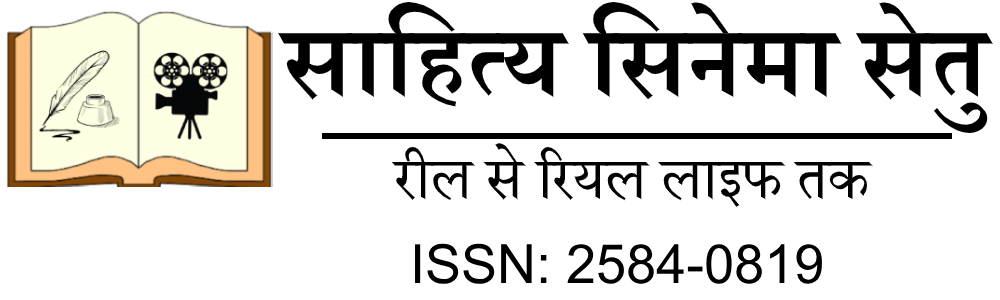

बहुत सार्थक कविता। साधुवाद।