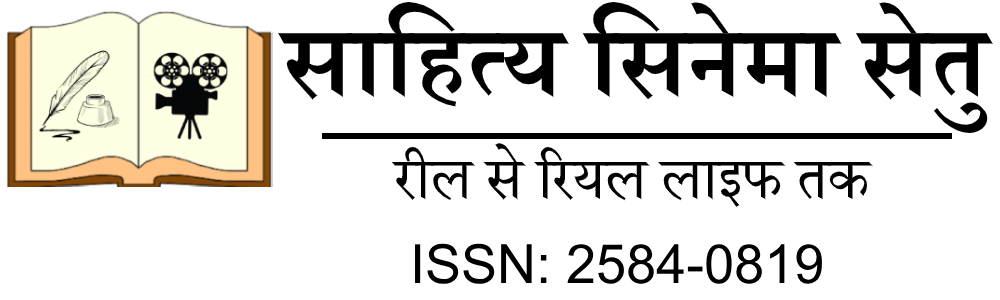असरानी (पूरा नाम : गोवर्धन असरानी) — एक ऐसा नाम जो अपने आप में हँसी की गूंज है पर उस हँसी के पीछे छिपी हुई गहरी मानवीय संवेदना शायद ही किसी ने उतनी स्पष्टता से देखी हो। हिन्दी सिनेमा के इस अद्भुत अभिनेता ने अपने जीवन के पाँच दशक इस बात को प्रमाणित करने में लगा दिए कि कॉमेडी कोई हल्की चीज़ नहीं होती, वह जीवन के सबसे भारी अनुभवों को सहज सामान्य मनोरंजक व व्यंग्यात्मक भाषा में कहने की एक गूढ़ कला है। असरानी को श्रद्धांजलि देते हुए आज यह स्मरण अनायास ही मन में उठता है कि किस तरह एक कलाकार अपने दौर से आगे जाकर भी अपने दर्शकों की सांसों में बसा रह सकता है।
असरानी की हँसी केवल एक दृश्य नहीं थी, वह समय का एक संगीत थी। उनकी मुस्कराहट में भारतीय मध्यमवर्ग की थकी हुई आत्मा को विश्राम मिलता था। वह कभी नौकर बनकर हँसते थे, कभी टीचर बनकर, कभी पुलिस अधिकारी तो कभी जेलर बनकर। “शोले” के उस विख्यात जेलर की भूमिका जब उन्होंने निभाई तब भारत ने एक साथ दो बातें सीखी — कि हँसी कितनी रचनात्मक हो सकती है और कि व्यंग्य केवल मज़ाक नहीं, व्यवस्था के भीतर छिपी हुई सच्चाई का आईना है। “हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं” कहते हुए असरानी जैसे उस पीढ़ी की स्मृति को झकझोरते थे जिसने उपनिवेशिक अवशेषों के साथ जीना सीखा पर उन्हें कभी प्रश्नों के घेरे में नहीं लिया।
उनकी आँखें छोटी थीं पर उनमें एक अथाह गहराई थी। अभिनय करते हुए वे किसी खास प्रयत्न के बिना दर्शक को अपने संसार में खींच लेते थे। वे ‘कॉमेडियन’ नहीं लगते थे, वे एक सामान्य मनुष्य लगते थे जो जीवन की विसंगतियों पर हँसना सीख चुका है। असरानी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने कॉमेडी को नाटक से निकालकर जीवन में ला दिया। वे हमें यह एहसास कराते थे कि हर त्रासदी के भीतर थोड़ी हँसी छिपी है और हर हँसी के भीतर कोई पुरानी पीड़ा।
जयपुर के एक सिंधी परिवार से निकलकर बंबई के फिल्म संसार में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। न शोर था, न प्रपंच। असरानी ने धीरे-धीरे, अपने सहज स्वभाव से दर्शकों का मन जीता। राजकपूर, ऋषिकेश मुखर्जी, हृषिकेश मुखर्जी, गुलजार, बासु चटर्जी — इन सभी संवेदनशील निर्देशकों की फिल्मों में असरानी की उपस्थिति एक गर्माहट की तरह होती थी। “चुपके चुपके”, “अभिमान”, “गोलमाल”, “आलाप”, “बावर्ची” — ये केवल फिल्में नहीं थीं, ये उस दौर की भारतीय आत्मा की कोमल परतें थीं, जिन पर असरानी की हँसी एक पतली रेखा की तरह खिंचती थी और मनुष्य की थकान कुछ पल को उतर जाती थी।
पर असरानी केवल कॉमेडियन नहीं थे। वे एक शिल्पकार थे जिन्होंने अभिनय के शास्त्र को आत्मा के भीतर उतार लिया था। उनकी टाइमिंग, उनका चेहरा, उनकी आवाज़ — सब मिलकर एक ऐसा रिद्म बनाते थे जिसमें नाटकीयता नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक संगीत था। वे जानते थे कि किस क्षण रुकना है, किस क्षण मुस्कराना है और किस क्षण खामोश रह जाना है। यही खामोशी उनके अभिनय की सबसे बड़ी संपदा थी। क्योंकि असली कॉमेडी वहाँ होती है जहाँ हँसी और आँसू एक-दूसरे को पहचान लेते हैं।
उनकी आवाज़ में एक अलग खनक थी। कभी वह आवाज़ बनावटी लगती थी पर वही बनावट भारतीय जीवन की नकली खुशियों की सच्ची परछाई बन जाती थी। असरानी की भूमिकाओं में अक्सर एक ऐसा आदमी दिखता है जो अपने हालात पर हँसने को मजबूर है। “चालबाज़”, “अतरंगी”, “पतंग”, “अभिमान” — हर जगह उनकी आँखों के कोनों में एक सूक्ष्म उदासी छिपी रहती थी। यह उदासी उनका हस्ताक्षर थी।
गोवर्धन असरानी ने न केवल अभिनय किया बल्कि उन्होंने उस अभिनय की एक नई भाषा बनाई। हिन्दी सिनेमा के स्वर्ण युग में जहां कॉमेडी अक्सर साइड रोल मानी जाती थी, उन्होंने उसे एक आत्मीय कला बना दिया। उनके पात्र मुख्य नायक के साथ नहीं चलते थे बल्कि उसकी आत्मा के प्रतिबिंब की तरह खड़े रहते थे। वे दर्शक को नायक से नहीं, इंसान से जोड़ते थे। जब वे हँसते थे तो दर्शक भी खुद पर हँसता था। यह हँसी आत्मचिंतन की हँसी थी, आत्मज्ञान की नहीं, आत्मस्वीकार की। वह पीढ़ी जिसने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, जया भादुड़ी और शबाना आज़मी को देखा, उसने असरानी की हँसी को अपनी रोज़मर्रा की राहत के रूप में जिया। उस दौर में जब सिनेमा में हिंसा, संघर्ष और सामाजिक असंतोष बढ़ रहा था, असरानी की उपस्थिति एक शांत पुल की तरह थी जो दर्शक को कहानी की जटिलता से बाहर निकाल कर उसकी आत्मा में लौटा लाती थी। वे हँसाते-हँसाते जीवन के बहुत गहरे अर्थों को स्पर्श कर जाते थे।
कला का सबसे बड़ा सत्य यही है कि वह अपनी उपस्थिति से अनुपस्थिति को अर्थ देती है। असरानी अब नहीं हैं, पर उनका अभाव भी किसी उपस्थिति की तरह है। जब भी स्क्रीन पर कोई पात्र अपने हास्य से हमें गुदगुदाता है, असरानी की छाया वहाँ झिलमिलाती है। जब कोई अभिनेता बिना ओवरएक्टिंग के सिर्फ एक छोटी-सी हरकत से दर्शक को मुस्कराने पर मजबूर करता है, वहाँ असरानी की आत्मा उपस्थित होती है। उन्होंने सिखाया कि अभिनय का सार ‘अंडरस्टेटमेंट’ में है, अतिशयोक्ति में नहीं। उनका जाना केवल एक अभिनेता का जाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के हास्यबोध के एक युग का अंत है। आज के समय में जहाँ कॉमेडी अधिकतर लाउड हो चुकी है, असरानी का सूक्ष्म, संयत और मानवीय हास्य याद दिलाता है कि असली हँसी वह होती है जो भीतर से उठे — जो दिल के किसी कोने को छू जाए और सोच में डाल दे।
उनके जाने के बाद सिनेमा जगत ने जो शोक प्रकट किया, वह केवल औपचारिक नहीं था। सहकलाकारों ने बार-बार कहा कि असरानी का सेट पर रहना अपने आप में एक आश्वासन होता था — जैसे कोई बड़ा भाई है जो सबको सहज रखेगा, सबके साथ हँसेगा और किसी को भारी नहीं होने देगा। यह स्वभाव किसी प्रशिक्षित अभिनय से नहीं आता, यह मनुष्य की मौलिक भलमनसाहत से आता है। उनकी हँसी अब स्मृति बन चुकी है पर वह स्मृति इतनी जीवंत है कि किसी भी संध्या में जब पुरानी फिल्मों की रोशनी टेलीविज़न पर पड़ती है तो असरानी की आँखें फिर चमक उठती हैं — “हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं” कहती हुई। यह संवाद केवल एक डायलॉग नहीं था, यह एक ऐतिहासिक टिप्पणी थी कि भारत ने किस तरह अपनी हँसी में भी अपने अतीत को जगह दी है। कला, समय से बड़ी होती है। असरानी का काम यही सिद्ध करता है। उन्होंने अभिनय को एक मानवीय स्पर्श दिया और दिखाया कि कलाकार अमर इसलिए नहीं होता कि वह कितनी बड़ी भूमिकाएँ निभाता है बल्कि इसलिए होता है कि वह अपने दर्शकों के भीतर कितनी जगह बना लेता है। असरानी हमारे भीतर हैं, हमारी हँसी में हैं, हमारी थकान में हैं।
जब किसी भीड़ भरी सड़क पर कोई रिक्शावाला मुस्कराता है जब कोई दुकानदार ग्राहकों से मज़ाक करता है, जब कोई बच्चा अपनी गलती पर खुद हँस पड़ता है — वहाँ असरानी की आत्मा जीवित है। उन्होंने हँसी को इतना मानवीय बना दिया कि वह जीवन की भाषा बन गई। गोवर्धन असरानी — यह नाम अब किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक भावना का पर्याय है। उनकी स्मृति हमें यह याद दिलाती है कि हँसने का अर्थ कभी भी जीवन को हल्का लेना नहीं होता; हँसी, जीवन को गहराई से समझने का एक तरीका है। वे गए नहीं हैं, वे सिर्फ सिनेमा के किसी पुराने फ्रेम में स्थिर हो गए हैं — जैसे कोई प्रकाश कण समय की झिल्ली में ठहर गया हो। जब भी पर्दे पर कोई सरल चेहरा दिखता है जब भी कोई पात्र अपनी व्यथा को मुस्कराहट में ढक लेता है तब हम अनायास कहते हैं — “यह असरानी की तरह है।” यही उनका अमरत्व है। उनके लिए यह श्रद्धांजलि कोई शोकगीत नहीं, बल्कि एक स्नेहगीत है — क्योंकि असरानी ने सिखाया कि जीवन को रोने के लिए नहीं, मुस्कराने के लिए जीना चाहिए। वे अपने जीवन से यह कहते चले गए कि हँसी भी एक साधना है और जो इसे साध लेता है, वह मृत्यु से भी परे चला जाता है।
आज जब भारतीय सिनेमा का परिदृश्य बदल चुका है, तकनीक और ग्लैमर ने संवेदना को ढक लिया है तब असरानी की याद एक दीपक की तरह है जो सादगी और संवेदना दोनों को उजागर करती है। उन्होंने हमें दिखाया कि सरलता ही सबसे कठिन कला है और ईमानदारी ही सबसे गहरा अभिनय। गोवर्धन असरानी अब समय के पार हैं — पर उनकी हँसी अब भी हवा में गूंजती है। यह गूंज किसी पुरानी फिल्म के संवाद की नहीं बल्कि एक युग की आत्मा की गूंज है। उन्होंने हमें जीवन की सबसे अनमोल शिक्षा दी — कि हँसी में भी करुणा होती है, और करुणा में भी हँसी। यह श्रद्धांजलि उस हँसी को समर्पित है जिसने हमें मनुष्य बनना सिखाया। असरानी चले गए पर उनका हँसता चेहरा हमारे भीतर अब भी जीवित है — जैसे किसी पुरानी दोपहर में धूप की झिलमिलाहट ठहरी हो, जैसे किसी फिल्म के आख़िरी दृश्य में बजता हुआ संगीत अब भी सुनाई देता हो। हँसी कभी मरती नहीं; वह स्मृति बनकर संसार के हर कोने में फैल जाती है। समय की गति अजीब होती है — वह किसी को मिटाता नहीं, बस उसे बदल देता है। असरानी अब हमारे बीच नहीं हैं पर उनकी मुस्कराहट अब भी हमारे भीतर चलती रहती है। किसी पुरानी फिल्म के दृश्य में, किसी बूढ़े दर्शक की आँखों में, या किसी बच्चे की सहज खिलखिलाहट में उनका अंश झलक जाता है। वे जैसे कह रहे हों — “देखो, ज़िन्दगी उतनी कठिन नहीं जितनी तुमने मान ली है।” यही असरानी का जादू था — वे कठिन समय को आसान बना देते थे।
उनका चेहरा, उनकी आवाज़, उनका चाल-ढाल — सबकुछ इतना स्वाभाविक था कि लगता था वे अभिनय नहीं, जीवन जी रहे हैं। शायद यही अभिनय की सबसे ऊँची मंज़िल है — जब अभिनय और जीवन के बीच की रेखा मिट जाए। वे पात्र में नहीं घुसते थे, पात्र उनमें समा जाता था। इसीलिए उनके किरदार कभी मरते नहीं, वे समय के साथ-साथ चलते रहते हैं। अगर राजेश खन्ना का चेहरा रोमांस का प्रतीक था अगर अमिताभ बच्चन की आवाज़ गुस्से की पहचान थी तो असरानी की मुस्कान भारतीय मध्यवर्ग की राहत थी। उनके भीतर एक ऐसा आदमी था जो थक चुका था पर हँसना नहीं छोड़ा था। वह आदमी हमारी गली-मोहल्लों में भी रहता है और हमारे भीतर भी। असरानी ने उसी आम आदमी को सिनेमा के पर्दे पर प्रतिष्ठा दी। वे कभी ज़ोर से नहीं हँसते थे, पर उनकी हँसी की तरंग देर तक गूंजती थी क्योंकि वह किसी ‘जोकर’ की हँसी नहीं थी, वह मनुष्य की हँसी थी — जो अपने दुखों को स्वीकार कर भी मुस्कराना जानता है। यही हँसी उन्हें चार्ली चैपलिन की परंपरा से जोड़ती है। चैपलिन ने कहा था — “Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.” असरानी ने इस सूत्र को भारतीय धरती पर उतारा। उन्होंने हमारी त्रासदियों को हल्केपन के रंग में रंग दिया ताकि वे बोझ न बनें, अनुभव बनें।
उनकी कॉमेडी कभी सस्ती नहीं होती थी। वह व्यंग्य थी — पर सौंदर्य के साथ। “शोले” में उनका जेलर, “चुपके चुपके” में प्रोफेसर, “गोलमाल” में ऑफिस का सहकर्मी — हर किरदार में एक सामाजिक टिप्पणी छिपी थी। वे समाज के भीतर चल रहे ढोंग को मुस्कराकर दिखा देते थे। उनका तरीका तंज का नहीं, संकेत का था। वह संकेत इतना बारीक होता था कि दर्शक को देर से समझ आता पर जब समझ आता तो वह भीतर तक उतर जाता था।
असरानी की अभिनय-यात्रा भारतीय सिनेमा के विकास की यात्रा है। उन्होंने श्वेत-श्याम से रंगीन तक, मंच से स्क्रीन तक, नाटक से फिल्म तक हर दौर देखा पर वे कभी ‘पुराने’ नहीं लगे क्योंकि उनके भीतर बचपन हमेशा जीवित रहा। उस बचपन में जिज्ञासा थी, खेल था और सबसे ज़रूरी — दूसरों को हँसाने की करुण इच्छा।
जीवन में सबसे कठिन काम है — दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। असरानी ने यह कठिनाई सरलता से निभाई। शायद इसीलिए वे अभिनय के बाद भी, साक्षात्कारों में, समारोहों में, अपने प्रशंसकों के बीच — वही सहज, नम्र, मुस्कराते हुए व्यक्ति बने रहे। वे अपने समय के सबसे लोकप्रिय हास्य कलाकार थे, पर उनमें कोई दंभ नहीं था। वे अपने कला से अधिक अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में जगह बनाते थे। कभी-कभी लगता है, असरानी हमारे सिनेमा का वह अधूरा गीत हैं जो हमेशा गुनगुनाता रहेगा। उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं, एक विराम है — जहाँ हँसी खुद को सँभालती है और करुणा बन जाती है। आज जब हम किसी फ़िल्म में ठहाकों के बीच संवेदना खोजते हैं तो अहसास होता है कि असरानी ने हमें क्या सिखाया — कि हास्य और मानवीय गहराई एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। असली कलाकार वही है जो दर्शक को हँसाते हुए भीतर कुछ बदल दे। असरानी ने हमें भीतर से थोड़ा बेहतर मनुष्य बनाया। उनकी स्मृति में आज भी कोई गीत बजता है — “हँसना मत भूलना, चाहे आँसू ही क्यों न आएँ।” वे इस पंक्ति के सबसे सच्चे दूत थे। उन्होंने सिखाया कि ज़िन्दगी को गंभीरता से नहीं, कोमलता से लेना चाहिए। उनके जाने से सिनेमा से ज़्यादा, जीवन ने एक रोशनी खो दी है।
वे हमें यह कहकर विदा हुए ~“मुस्कराते रहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है।”
सचमुच, जब हम मुस्कराते हैं तो वह असरानी की स्मृति को जीवित रखती है। वह मुस्कान अब भी हमारे भीतर गूंजती है~
कहीं शोले के जेलर की आवाज़ में, कहीं चुपके चुपके के प्रोफेसर की मासूमियत में, कहीं उस आम आदमी की थकी हँसी में जो अब भी ज़िन्दगी से प्यार करता है। गोवर्धन असरानी चले गए पर उनकी हँसी अब भी हमारे बीच है — एक दीपक की लौ की तरह, जो बुझती नहीं, बस दिशा बदलती है।
गोवर्धन असरानी ~आपकी हँसी हमारे समय का सबसे कोमल शोकगीत है।